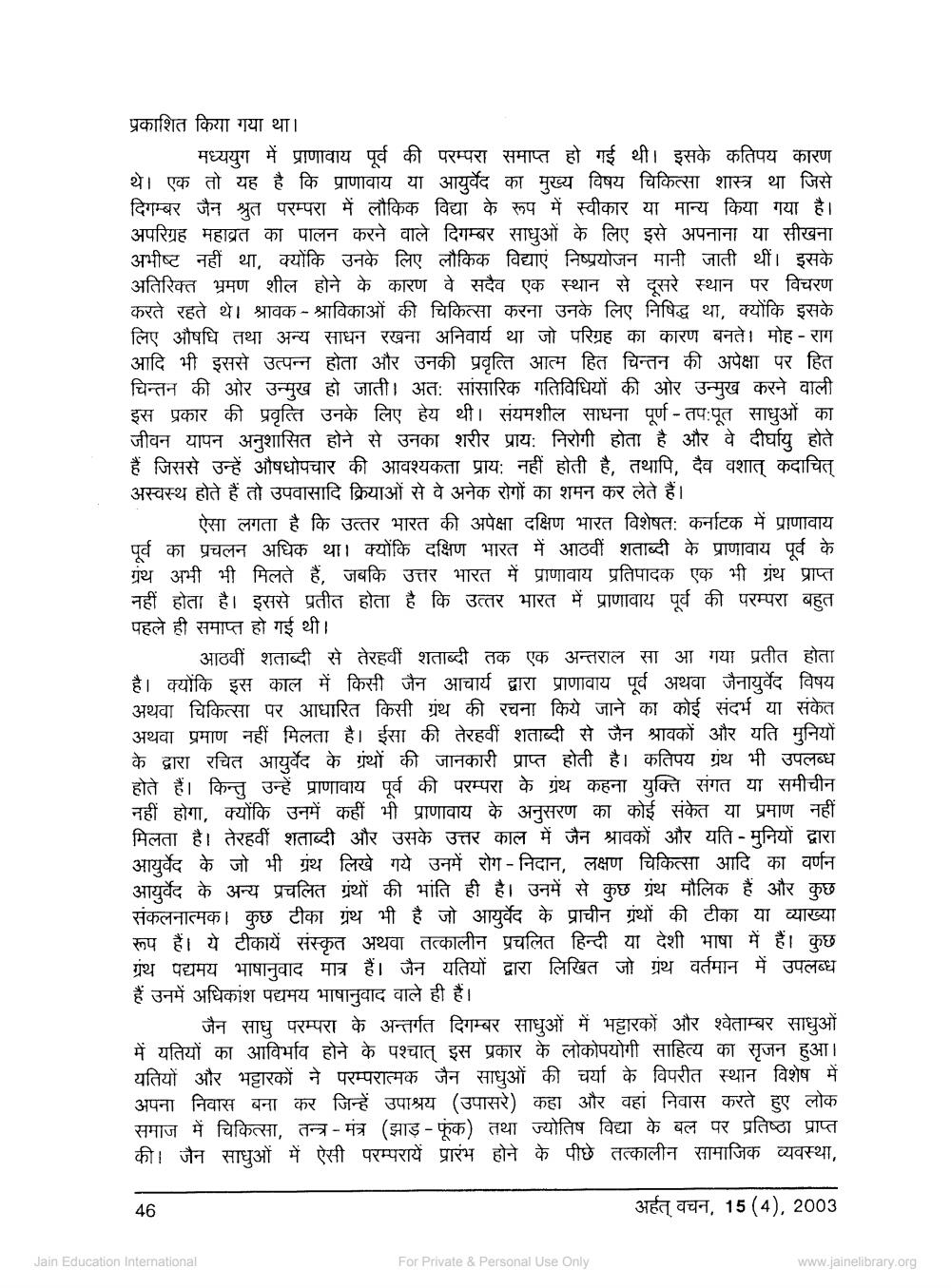________________
प्रकाशित किया गया था।
मध्ययुग में प्राणावाय पूर्व की परम्परा समाप्त हो गई थी। इसके कतिपय कारण थे। एक तो यह है कि प्राणावाय या आयुर्वेद का मुख्य विषय चिकित्सा शास्त्र था जिसे दिगम्बर जैन श्रुत परम्परा में लौकिक विद्या के रूप में स्वीकार या मान्य किया गया है। अपरिग्रह महाव्रत का पालन करने वाले दिगम्बर साधुओं के लिए इसे अपनाना या सीखना अभीष्ट नहीं था, क्योंकि उनके लिए लौकिक विद्याएं निष्प्रयोजन मानी जाती थीं। इसके अतिरिक्त भ्रमण शील होने के कारण वे सदैव एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते रहते थे। श्रावक-श्राविकाओं की चिकित्सा करना उनके लिए निषिद्ध था, क्योंकि इसके लिए औषधि तथा अन्य साधन रखना अनिवार्य था जो परिग्रह का कारण बनते। मोह - राग आदि भी इससे उत्पन्न होता और उनकी प्रवृत्ति आत्म हित चिन्तन की अपेक्षा पर हित चिन्तन की ओर उन्मुख हो जाती। अतः सांसारिक गतिविधियों की ओर उन्मुख करने वाली इस प्रकार की प्रवृत्ति उनके लिए हेय थी। संयमशील साधना पूर्ण तपः पूत साधुओं का जीवन यापन अनुशासित होने से उनका शरीर प्राय: निरोगी होता है और वे दीर्घायु होते हैं जिससे उन्हें औषधोपचार की आवश्यकता प्रायः नहीं होती है, तथापि, दैव वशात् कदाचित् अस्वस्थ होते हैं तो उपवासादि क्रियाओं से वे अनेक रोगों का शमन कर लेते हैं।
ऐसा लगता है कि उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत विशेषत: कर्नाटक में प्राणावाय पूर्व का प्रचलन अधिक था क्योंकि दक्षिण भारत में आठवीं शताब्दी के प्राणावाय पूर्व के ग्रंथ अभी भी मिलते हैं, जबकि उत्तर भारत में प्राणावाय प्रतिपादक एक भी ग्रंथ प्राप्त नहीं होता है। इससे प्रतीत होता है कि उत्तर भारत में प्राणावाय पूर्व की परम्परा बहुत पहले ही समाप्त हो गई थी।
आठवीं शताब्दी से तेरहवीं शताब्दी तक एक अन्तराल सा आ गया प्रतीत होता है। क्योंकि इस काल में किसी जैन आचार्य द्वारा प्राणावाय पूर्व अथवा जैनायुर्वेद विषय अथवा चिकित्सा पर आधारित किसी ग्रंथ की रचना किये जाने का कोई संदर्भ या संकेत अथवा प्रमाण नहीं मिलता है ईसा की तेरहवीं शताब्दी से जैन श्रावकों और यति मुनियों के द्वारा रचित आयुर्वेद के ग्रंथों की जानकारी प्राप्त होती है कतिपय ग्रंथ भी उपलब्ध । होते हैं किन्तु उन्हें प्राणावाय पूर्व की परम्परा के ग्रंथ कहना युक्ति संगत या समीचीन नहीं होगा, क्योंकि उनमें कहीं भी प्राणावाय के अनुसरण का कोई संकेत या प्रमाण नहीं मिलता है। तेरहवीं शताब्दी और उसके उत्तर काल में जैन श्रावकों और यति मुनियों द्वारा आयुर्वेद के जो भी ग्रंथ लिखे गये उनमें रोग निदान, लक्षण चिकित्सा आदि का वर्णन आयुर्वेद के अन्य प्रचलित ग्रंथों की भांति ही है उनमें से कुछ ग्रंथ मौलिक हैं और कुछ संकलनात्मक कुछ टीका ग्रंथ भी है जो आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों की टीका या व्याख्या । रूप हैं। ये टीकायें संस्कृत अथवा तत्कालीन प्रचलित हिन्दी या देशी भाषा में हैं। कुछ ग्रंथ पद्यमय भाषानुवाद मात्र हैं। जैन यतियों द्वारा लिखित जो ग्रंथ वर्तमान में उपलब्ध हैं उनमें अधिकांश पद्यमय भाषानुवाद वाले ही हैं।
-
जैन साधु परम्परा के अन्तर्गत दिगम्बर साधुओं में भट्टारकों और श्वेताम्बर साधुओं में यतियों का आविर्भाव होने के पश्चात् इस प्रकार के लोकोपयोगी साहित्य का सृजन हुआ। यतियों और भट्टारकों ने परम्परात्मक जैन साधुओं की चर्या के विपरीत स्थान विशेष में अपना निवास बना कर जिन्हें उपाश्रय ( उपासरे) कहा और वहां निवास करते हुए लोक समाज में चिकित्सा, तन्त्र मंत्र (झाड़ फूंक ) तथा ज्योतिष विद्या के बल पर प्रतिष्ठा प्राप्त की जैन साधुओं में ऐसी परम्परायें प्रारंभ होने के पीछे तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था,
अर्हत् वचन, 15 (4), 2003
46
Jain Education International
-
-
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org