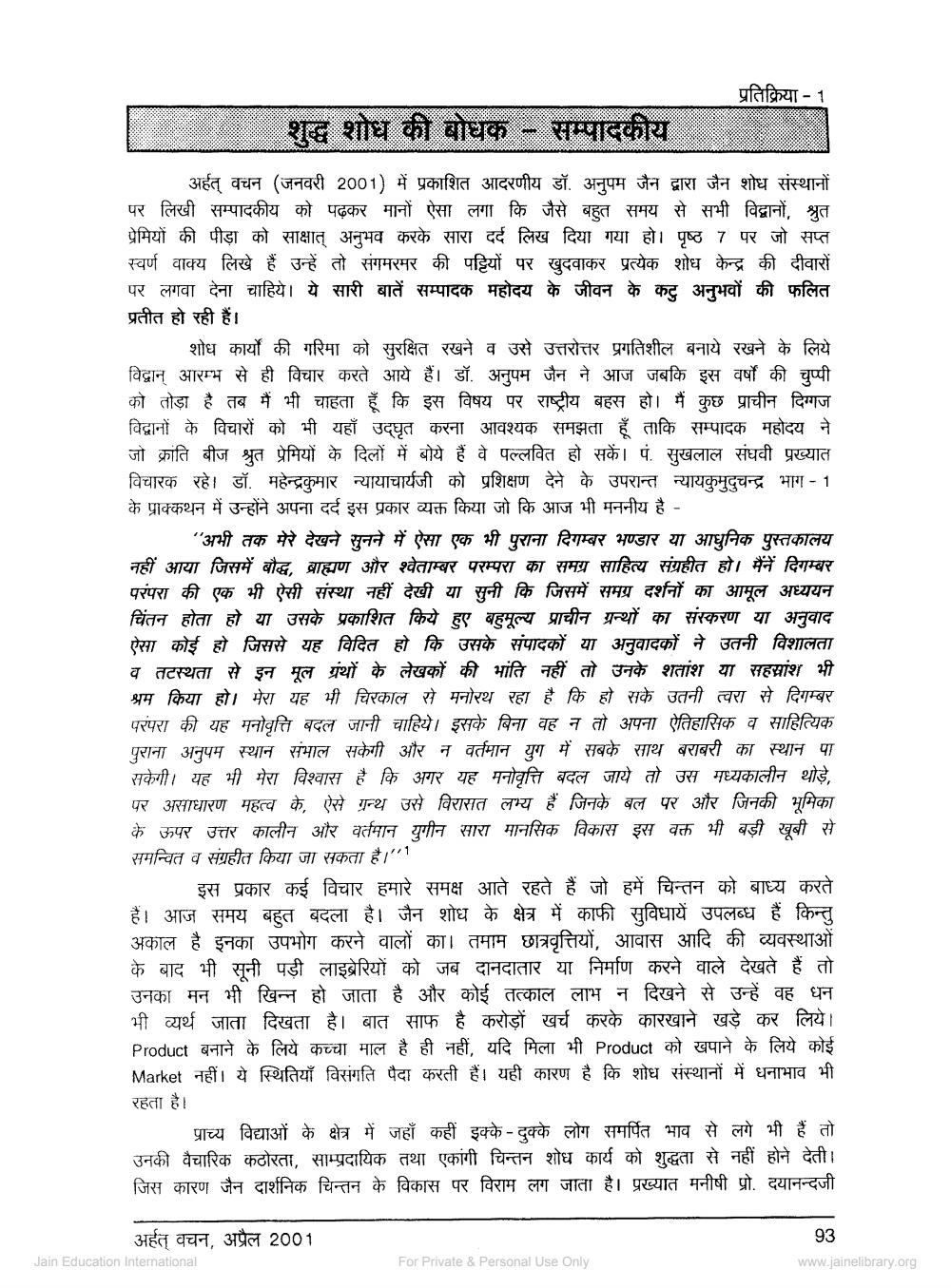________________
प्रतिक्रिया-1
शुद्ध शोध की बाधक - सम्पादकीय
अर्हत् वचन (जनवरी 2001) में प्रकाशित आदरणीय डॉ. अनुपम जैन द्वारा जैन शोध संस्थानों पर लिखी सम्पादकीय को पढ़कर मानों ऐसा लगा कि जैसे बहुत समय से सभी विद्वानों, श्रुत प्रेमियों की पीड़ा को साक्षात् अनुभव करके सारा दर्द लिख दिया गया हो। पृष्ठ 7 पर जो सप्त स्वर्ण वाक्य लिखे हैं उन्हें तो संगमरमर की पट्टियों पर खुदवाकर प्रत्येक शोध केन्द्र की दीवारों पर लगवा देना चाहिये। ये सारी बातें सम्पादक महोदय के जीवन के कटु अनुभवों की फलित प्रतीत हो रही हैं।
शोध कार्यों की गरिमा को सुरक्षित रखने व उसे उत्तरोत्तर प्रगतिशील बनाये रखने के लिये विद्वान आरम्भ से ही विचार करते आये हैं। डॉ. अनुपम जैन ने आज जबकि इस वर्षों की चुप्पी
को तोड़ा है तब मैं भी चाहता हूँ कि इस विषय पर राष्ट्रीय बहस हो। मैं कुछ प्राचीन दिग्गज विद्वानों के विचारों को भी यहाँ उद्धृत करना आवश्यक समझता हूँ ताकि सम्पादक महोदय ने जो क्रांति बीज श्रुत प्रेमियों के दिलों में बोये हैं वे पल्लवित हो सकें। पं. सुखलाल संघवी प्रख्यात विचारक रहे। डॉ. महेन्द्रकुमार न्यायाचार्यजी को प्रशिक्षण देने के उपरान्त न्यायकुमुदुचन्द्र भाग - 1 के प्राक्कथन में उन्होंने अपना दर्द इस प्रकार व्यक्त किया जो कि आज भी मननीय है -
"अभी तक मेरे देखने सुनने में ऐसा एक भी पुराना दिगम्बर भण्डार या आधुनिक पुस्तकालय नहीं आया जिसमें बौद्ध, ब्राह्मण और श्वेताम्बर परम्परा का समग्र साहित्य संग्रहीत हो। मैंनें दिगम्बर परंपरा की एक भी ऐसी संस्था नहीं देखी या सुनी कि जिसमें समग्र दर्शनों का आमूल अध्ययन चिंतन होता हो या उसके प्रकाशित किये हुए बहुमूल्य प्राचीन ग्रन्थों का संस्करण या अनुवाद ऐसा कोई हो जिससे यह विदित हो कि उसके संपादकों या अनुवादकों ने उतनी विशालता व तटस्थता से इन मूल ग्रंथों के लेखकों की भांति नहीं तो उनके शतांश या सहस्रांश भी श्रम किया हो। मेरा यह भी चिरकाल से मनोरथ रहा है कि हो सके उतनी त्वरा से दिगम्बर परंपरा की यह मनोवृत्ति बदल जानी चाहिये। इसके बिना वह न तो अपना ऐतिहासिक व साहित्यिक पुराना अनुपम स्थान संभाल सकेगी और न वर्तमान युग में सबके साथ बराबरी का स्थान पा सकेगी। यह भी मेरा विश्वास है कि अगर यह मनोवृत्ति बदल जाये तो उस मध्यकालीन थोड़े, पर असाधारण महत्व के, ऐसे ग्रन्थ उसे विरासत लभ्य हैं जिनके बल पर और जिनकी भूमिका के ऊपर उत्तर कालीन और वर्तमान युगीन सारा मानसिक विकास इस वक्त भी बड़ी खूबी से समन्वित व संग्रहीत किया जा सकता है।"1
इस प्रकार कई विचार हमारे समक्ष आते रहते हैं जो हमें चिन्तन को बाध्य करते हैं। आज समय बहुत बदला है। जैन शोध के क्षेत्र में काफी सुविधायें उपलब्ध हैं किन्तु अकाल है इनका उपभोग करने वालों का। तमाम छात्रवृत्तियों, आवास आदि की व्यवस्थाओं के बाद भी सूनी पड़ी लाइब्रेरियों को जब दानदातार या निर्माण करने वाले देखते हैं तो उनका मन भी खिन्न हो जाता है और कोई तत्काल लाभ न दिखने से उन्हें वह धन भी व्यर्थ जाता दिखता है। बात साफ है करोड़ों खर्च करके कारखाने खड़े कर लिये। Product बनाने के लिये कच्चा माल है ही नहीं, यदि मिला भी Product को खपाने के लिये कोई Market नहीं। ये स्थितियाँ विसंगति पैदा करती हैं। यही कारण है कि शोध संस्थानों में धनाभाव भी रहता है।
प्राच्य विद्याओं के क्षेत्र में जहाँ कहीं इक्के - दुक्के लोग समर्पित भाव से लगे भी हैं तो उनकी वैचारिक कठोरता, साम्प्रदायिक तथा एकांगी चिन्तन शोध कार्य को शुद्धता से नहीं होने देती। जिस कारण जैन दार्शनिक चिन्तन के विकास पर विराम लग जाता है। प्रख्यात मनीषी प्रो. दयानन्दजी
अर्हत् वचन, अप्रैल 2001 Jain Education International
93
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org