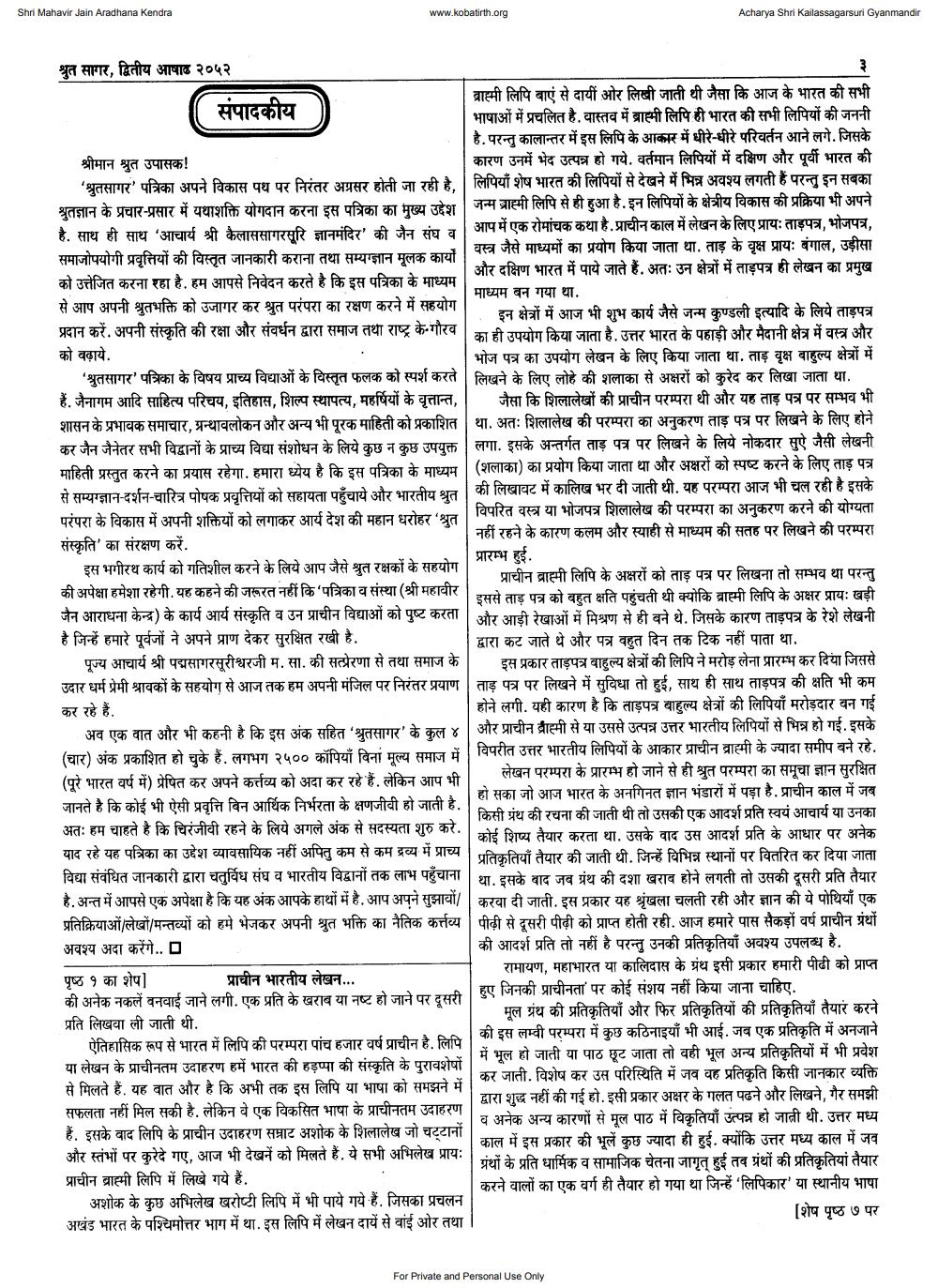________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
श्रुत सागर, द्वितीय आषाढ २०५२
संपादकीय
www.kobatirth.org
श्रीमान श्रुत उपासक!
'श्रुतसागर' पत्रिका अपने विकास पथ पर निरंतर अग्रसर होती जा रही है, श्रुतज्ञान के प्रचार-प्रसार में यथाशक्ति योगदान करना इस पत्रिका का मुख्य उद्देश है. साथ ही साथ 'आचार्य श्री कैलाससागरसूरि ज्ञानमंदिर' की जैन संघ व समाजोपयोगी प्रवृत्तियों की विस्तृत जानकारी कराना तथा सम्यग्ज्ञान मूलक कार्यों को उत्तेजित करना रहा है. हम आपसे निवेदन करते है कि इस पत्रिका के माध्यम से आप अपनी श्रुतभक्ति को उजागर कर श्रुत परंपरा का रक्षण करने में सहयोग प्रदान करें. अपनी संस्कृति की रक्षा और संवर्धन द्वारा समाज तथा राष्ट्र के गौरव को बढ़ाये.
'श्रुतसागर' पत्रिका के विषय प्राच्य विद्याओं के विस्तृत फलक को स्पर्श करते है. जैनागम आदि साहित्य परिचय, इतिहास, शिल्प स्थापत्य, महर्षियों के वृत्तान्त, शासन के प्रभावक समाचार, ग्रन्थावलोकन और अन्य भी पूरक माहिती को प्रकाशित कर जैन जैनेतर सभी विद्वानों के प्राच्य विद्या संशोधन के लिये कुछ न कुछ उपयुक्त माहिती प्रस्तुत करने का प्रयास रहेगा. हमारा ध्येय है कि इस पत्रिका के माध्यम से सम्यग्ज्ञान-दर्शन-चारित्र पोषक प्रवृत्तियों को सहायता पहुँचाये और भारतीय श्रुत परंपरा के विकास में अपनी शक्तियों को लगाकर आर्य देश की महान धरोहर 'श्रुत संस्कृति का संरक्षण करें.
इस भगीरथ कार्य को गतिशील करने के लिये आप जैसे श्रुत रक्षकों के सहयोग की अपेक्षा हमेशा रहेगी. यह कहने की जरूरत नहीं कि 'पत्रिका व संस्था (श्री महावीर जैन आराधना केन्द्र) के कार्य आर्य संस्कृति व उन प्राचीन विद्याओं को पुष्ट करता है जिन्हें हमारे पूर्वजों ने अपने प्राण देकर सुरक्षित रखी है.
पूज्य आचार्य श्री पद्मसागरसूरीश्वरजी म. सा. की सत्प्रेरणा से तथा समाज के उदार धर्म प्रेमी श्रावकों के सहयोग से आज तक हम अपनी मंजिल पर निरंतर प्रयाण कर रहे हैं.
O
अब एक बात और भी कहनी है कि इस अंक सहित 'श्रुतसागर' के कुल ४ (चार) अंक प्रकाशित हो चुके हैं. लगभग २५०० कॉपियाँ विनां मूल्य समाज में ( पूरे भारत वर्ष में) प्रेषित कर अपने कर्त्तव्य को अदा कर रहे हैं. लेकिन आप भी जानते है कि कोई भी ऐसी प्रवृत्ति विन आर्थिक निर्भरता के क्षणजीवी हो जाती है. अतः हम चाहते है कि चिरंजीवी रहने के लिये अगले अंक से सदस्यता शुरु करे. याद रहे यह पत्रिका का उद्देश व्यावसायिक नहीं अपितु कम से कम द्रव्य में प्राच्य विद्या संबंधित जानकारी द्वारा चतुर्विध संघ व भारतीय विद्वानों तक लाभ पहुँचाना है. अन्त में आपसे एक अपेक्षा है कि यह अंक आपके हाथों में है. आप अपने सुझावों/ प्रतिक्रियाओं/लेख/मन्तच्चों को हमे भेजकर अपनी श्रुत भक्ति का नैतिक कर्तव्य अवश्य अदा करेंगे...
पृष्ठ १ का शेष ]
प्राचीन भारतीय लेखन...
की अनेक नकलें बनवाई जाने लगी. एक प्रति के खराब या नष्ट हो जाने पर दूसरी
प्रति लिखवा ली जाती थी.
ऐतिहासिक रूप से भारत में लिपि की परम्परा पांच हजार वर्ष प्राचीन है. लिपि या लेखन के प्राचीनतम उदाहरण हमें भारत की हड़प्पा की संस्कृति के पुरावशेषों से मिलते हैं. यह वात और है कि अभी तक इस लिपि या भाषा को समझने में सफलता नहीं मिल सकी है. लेकिन वे एक विकसित भाषा के प्राचीनतम उदाहरण हैं. इसके बाद लिपि के प्राचीन उदाहरण सम्राट अशोक के शिलालेख जो चट्टानों और स्तंभों पर कुरेदे गए, आज भी देखनें को मिलते हैं. ये सभी अभिलेख प्रायः प्राचीन ब्राह्मी लिपि में लिखे गये हैं.
अशोक के कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में भी पाये गये हैं. जिसका प्रचलन अखंड भारत के पश्चिमोत्तर भाग में था. इस लिपि में लेखन दायें से बांई ओर तथा
Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir
३
ब्राह्मी लिपि बाएं से दायीं ओर लिखी जाती थी जैसा कि आज के भारत की सभी भाषाओं में प्रचलित है. वास्तव में ब्राह्मी लिपि ही भारत की सभी लिपियों की जननी है. परन्तु कालान्तर में इस लिपि के आकार में धीरे-धीरे परिवर्तन आने लगे. जिसके कारण उनमें भेद उत्पन्न हो गये. वर्तमान लिपियों में दक्षिण और पूर्वी भारत की लिपियाँ शेष भारत की लिपियों से देखने में भिन्न अवश्य लगती हैं परन्तु इन सबका जन्म ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है. इन लिपियों के क्षेत्रीय विकास की प्रक्रिया भी अपने आप में एक रोमांचक कथा है. प्राचीन काल में लेखन के लिए प्रायः ताड़पत्र, भोजपत्र, वस्त्र जैसे माध्यमों का प्रयोग किया जाता था. ताड़ के वृक्ष प्रायः बंगाल, उड़ीसा और दक्षिण भारत में पाये जाते हैं. अतः उन क्षेत्रों में ताड़पत्र ही लेखन का प्रमुख माध्यम बन गया था.
इन क्षेत्रों में आज भी शुभ कार्य जैसे जन्म कुण्डली इत्यादि के लिये ताड़पत्र का ही उपयोग किया जाता है. उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र में वस्त्र और भोज पत्र का उपयोग लेखन के लिए किया जाता था. ताड़ वृक्ष बाहुल्य क्षेत्रों में लिखने के लिए लोहे की शलाका से अक्षरों को कुरेद कर लिखा जाता था.
जैसा कि शिलालेखों की प्राचीन परम्परा थी और यह ताड़ पत्र पर सम्भव भी था. अतः शिलालेख की परम्परा का अनुकरण ताड़ पत्र पर लिखने के लिए होने लगा. इसके अन्तर्गत ताड़ पत्र पर लिखने के लिये नोकदार सुऐ जैसी लेखनी ( शलाका) का प्रयोग किया जाता था और अक्षरों को स्पष्ट करने के लिए ताड़ पत्र की लिखावट में कालिख भर दी जाती थी. यह परम्परा आज भी चल रही है इसके नहीं रहने के कारण कलम और स्याही से माध्यम की सतह पर लिखने की परम्परा विपरित वस्त्र या भोजपत्र शिलालेख की परम्परा का अनुकरण करने की योग्यता प्रारम्भ हुई.
प्राचीन ब्राह्मी लिपि के अक्षरों को ताड़ पत्र पर लिखना तो सम्भव था परन्तु इससे ताड़ पत्र को बहुत क्षति पहुंचती थी क्योंकि ब्राह्मी लिपि के अक्षर प्रायः खड़ी और आड़ी रेखाओं में मिश्रण से ही बने थे. जिसके कारण ताड़पत्र के रेशे लेखनी द्वारा कट जाते थे और पत्र बहुत दिन तक टिक नहीं पाता था.
इस प्रकार ताड़पत्र बाहुल्य क्षेत्रों की लिपि ने मरोड़ लेना प्रारम्भ कर दिया जिससे ताड़ पत्र पर लिखने में सुविधा तो हुई, साथ ही साथ ताड़पत्र की क्षति भी कम होने लगी. यही कारण है कि ताड़पत्र बाहुल्य क्षेत्रों की लिपियाँ मरोड़दार बन गई और प्राचीन ब्राह्मी से या उससे उत्पन्न उत्तर भारतीय लिपियों से भिन्न हो गई. इसके विपरीत उत्तर भारतीय लिपियों के आकार प्राचीन ब्राह्मी के ज्यादा समीप बने रहे.
हो
लेखन परम्परा के प्रारम्भ हो जाने से ही श्रुत परम्परा का समूचा ज्ञान सुरक्षित सका जो आज भारत के अनगिनत ज्ञान भंडारों में पड़ा है. प्राचीन काल में जब किसी ग्रंथ की रचना की जाती थी तो उसकी एक आदर्श प्रति स्वयं आचार्य या कोई शिष्य तैयार करता था. उसके बाद उस आदर्श प्रति के आधार पर अनेक प्रतिकृतियाँ तैयार की जाती थी. जिन्हें विभिन्न स्थानों पर वितरित कर दिया जाता था. इसके बाद जब ग्रंथ की दशा खराब होने लगती तो उसकी दूसरी प्रति तैयार करवा दी जाती. इस प्रकार यह श्रृंखला चलती रही और ज्ञान की ये पोथियाँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होती रही. आज हमारे पास सैकड़ों वर्ष प्राचीन ग्रंथों की आदर्श प्रति तो नहीं है परन्तु उनकी प्रतिकृतियाँ अवश्य उपलब्ध है.
रामायण, महाभारत या कालिदास के ग्रंथ इसी प्रकार हमारी पीढी को प्राप्त हुए जिनकी प्राचीनता पर कोई संशय नहीं किया जाना चाहिए.
मूल ग्रंथ की प्रतिकृतियाँ और फिर प्रतिकृतियों की प्रतिकृतियाँ तैयार करने की इस लम्बी परम्परा में कुछ कठिनाइयाँ भी आई. जब एक प्रतिकृति में अनजाने में भूल हो जाती या पाठ छूट जाता तो वही भूल अन्य प्रतिकृतियों में भी प्रवेश कर जाती. विशेष कर उस परिस्थिति में जब वह प्रतिकृति किसी जानकार व्यक्ति द्वारा शुद्ध नहीं की गई हो. इसी प्रकार अक्षर के गलत पढने और लिखने, गैर समझी व अनेक अन्य कारणों से मूल पाठ में विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती थी. उत्तर मध्य काल में इस प्रकार की भूलें कुछ ज्यादा ही हुई. क्योंकि उत्तर मध्य काल में जव ग्रंथों के प्रति धार्मिक व सामाजिक चेतना जागृत हुई तब ग्रंथों की प्रतिकृतियां तैयार करने वालों का एक वर्ग ही तैयार हो गया था जिन्हें 'लिपिकार' या स्थानीय भाषा [शेष पृष्ठ ७ पर
For Private and Personal Use Only