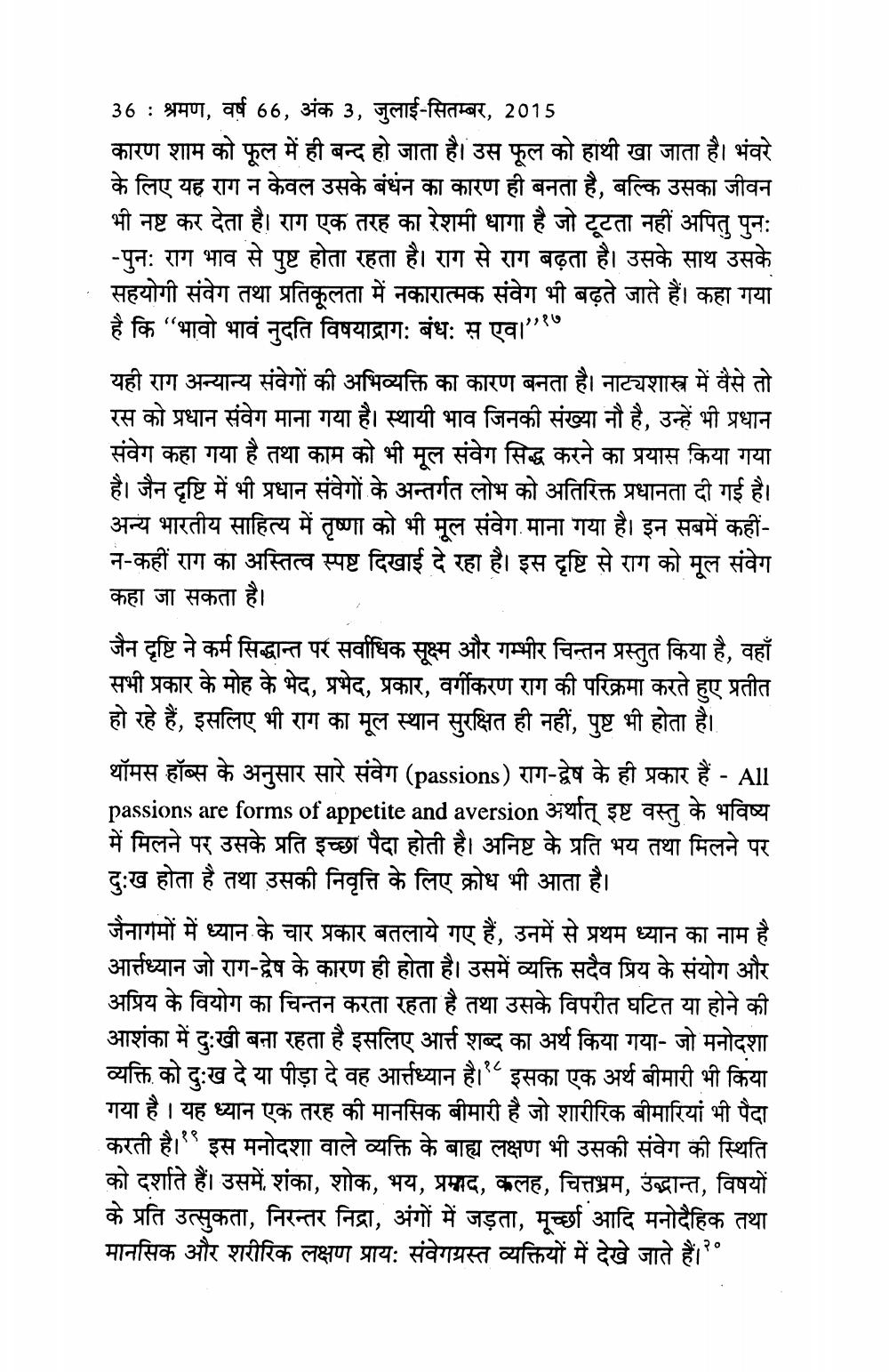________________
36 : श्रमण, वर्ष 66, अंक 3, जुलाई-सितम्बर, 2015 कारण शाम को फूल में ही बन्द हो जाता है। उस फूल को हाथी खा जाता है। भंवरे के लिए यह राग न केवल उसके बंधन का कारण ही बनता है, बल्कि उसका जीवन भी नष्ट कर देता है। राग एक तरह का रेशमी धागा है जो टूटता नहीं अपितु पुनः -पुन: राग भाव से पुष्ट होता रहता है। राग से राग बढ़ता है। उसके साथ उसके सहयोगी संवेग तथा प्रतिकूलता में नकारात्मक संवेग भी बढ़ते जाते हैं। कहा गया है कि "भावो भावं नुदति विषयाद्राग: बंधः स एव।" यही राग अन्यान्य संवेगों की अभिव्यक्ति का कारण बनता है। नाट्यशास्त्र में वैसे तो रस को प्रधान संवेग माना गया है। स्थायी भाव जिनकी संख्या नौ है, उन्हें भी प्रधान संवेग कहा गया है तथा काम को भी मूल संवेग सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। जैन दृष्टि में भी प्रधान संवेगों के अन्तर्गत लोभ को अतिरिक्त प्रधानता दी गई है। अन्य भारतीय साहित्य में तृष्णा को भी मूल संवेग माना गया है। इन सबमें कहींन-कहीं राग का अस्तित्व स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस दृष्टि से राग को मूल संवेग कहा जा सकता है। जैन दृष्टि ने कर्म सिद्धान्त पर सर्वाधिक सूक्ष्म और गम्भीर चिन्तन प्रस्तुत किया है, वहाँ सभी प्रकार के मोह के भेद, प्रभेद, प्रकार, वर्गीकरण राग की परिक्रमा करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए भी राग का मूल स्थान सुरक्षित ही नहीं, पुष्ट भी होता है। थॉमस हॉब्स के अनुसार सारे संवेग (passions) राग-द्वेष के ही प्रकार हैं - All passions are forms of appetite and aversion अर्थात् इष्ट वस्तु के भविष्य में मिलने पर उसके प्रति इच्छा पैदा होती है। अनिष्ट के प्रति भय तथा मिलने पर दुःख होता है तथा उसकी निवृत्ति के लिए क्रोध भी आता है। जैनागमों में ध्यान के चार प्रकार बतलाये गए हैं, उनमें से प्रथम ध्यान का नाम है आर्तध्यान जो राग-द्वेष के कारण ही होता है। उसमें व्यक्ति सदैव प्रिय के संयोग और अप्रिय के वियोग का चिन्तन करता रहता है तथा उसके विपरीत घटित या होने की आशंका में दुःखी बना रहता है इसलिए आर्त शब्द का अर्थ किया गया- जो मनोदशा व्यक्ति को दुःख दे या पीड़ा दे वह आर्तध्यान है।" इसका एक अर्थ बीमारी भी किया गया है । यह ध्यान एक तरह की मानसिक बीमारी है जो शारीरिक बीमारियां भी पैदा करती है। इस मनोदशा वाले व्यक्ति के बाह्य लक्षण भी उसकी संवेग की स्थिति को दर्शाते हैं। उसमें शंका, शोक, भय, प्रमाद, कलह, चित्तभ्रम, उद्धान्त, विषयों के प्रति उत्सुकता, निरन्तर निद्रा, अंगों में जड़ता, मूर्छा आदि मनोदैहिक तथा मानसिक और शरीरिक लक्षण प्राय: संवेगग्रस्त व्यक्तियों में देखे जाते हैं।२०