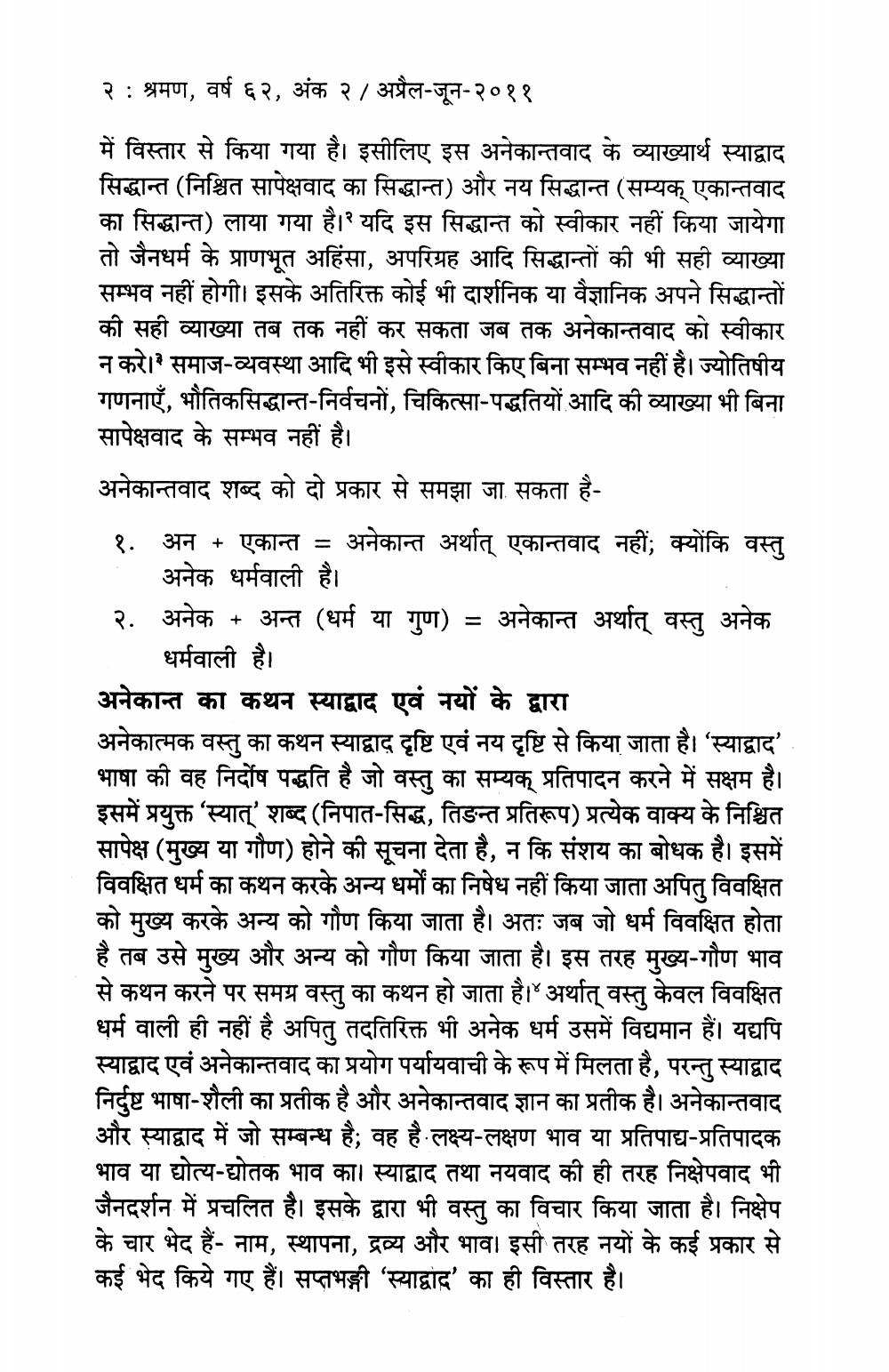________________
२ : श्रमण, वर्ष ६२, अंक २ / अप्रैल-जून २०११
में विस्तार से किया गया है। इसीलिए इस अनेकान्तवाद के व्याख्यार्थ स्याद्वाद सिद्धान्त (निश्चित सापेक्षवाद का सिद्धान्त) और नय सिद्धान्त (सम्यक् एकान्तवाद का सिद्धान्त) लाया गया है। यदि इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया जायेगा तो जैनधर्म के प्राणभूत अहिंसा, अपरिग्रह आदि सिद्धान्तों की भी सही व्याख्या सम्भव नहीं होगी। इसके अतिरिक्त कोई भी दार्शनिक या वैज्ञानिक अपने सिद्धान्तों की सही व्याख्या तब तक नहीं कर सकता जब तक अनेकान्तवाद को स्वीकार न करे।' समाज-व्यवस्था आदि भी इसे स्वीकार किए बिना सम्भव नहीं है। ज्योतिषीय गणनाएँ, भौतिक सिद्धान्त - निर्वचनों, चिकित्सा पद्धतियों आदि की व्याख्या भी बिना सापेक्षवाद के सम्भव नहीं है।
अनेकान्तवाद शब्द को दो प्रकार से समझा जा सकता है -
१.
अन + एकान्त = अनेक धर्मवाली है।
२. अनेक + अन्त (धर्म या गुण) = अनेकान्त अर्थात् वस्तु अनेक
अनेकान्त अर्थात् एकान्तवाद नहीं; क्योंकि वस्तु
धर्मवाली है।
अनेकान्त का कथन स्याद्वाद एवं नयों के द्वारा
अनेकात्मक वस्तु का कथन स्याद्वाद दृष्टि एवं नय दृष्टि से किया जाता है। 'स्याद्वाद' भाषा की वह निर्दोष पद्धति है जो वस्तु का सम्यक् प्रतिपादन करने में सक्षम है। इसमें प्रयुक्त ‘स्यात्' शब्द (निपात- सिद्ध, तिङन्त प्रतिरूप) प्रत्येक वाक्य के निश्चित सापेक्ष (मुख्य या गौण) होने की सूचना देता है, न कि संशय का बोधक है। इसमें विवक्षित धर्म का कथन करके अन्य धर्मों का निषेध नहीं किया जाता अपितु विवक्षित को मुख्य करके अन्य को गौण किया जाता है । अतः जब जो धर्म विवक्षित होता है तब उसे मुख्य और अन्य को गौण किया जाता है। इस तरह मुख्य- य-गौण भाव से कथन करने पर समग्र वस्तु का कथन हो जाता है।' अर्थात् वस्तु केवल विवक्षित धर्म वाली ही नहीं है अपितु तदतिरिक्त भी अनेक धर्म उसमें विद्यमान हैं। यद्यपि स्याद्वाद एवं अनेकान्तवाद का प्रयोग पर्यायवाची के रूप में मिलता है, परन्तु स्याद्वाद निर्दुष्ट भाषा-शैली का प्रतीक है और अनेकान्तवाद ज्ञान का प्रतीक है । अनेकान्तवाद और स्याद्वाद में जो सम्बन्ध है; वह है लक्ष्य लक्षण भाव या प्रतिपाद्यप्रतिपादक भाव या द्योत्य- द्योतक भाव का। स्याद्वाद तथा नयवाद की ही तरह निक्षेपवाद भी जैनदर्शन में प्रचलित है। इसके द्वारा भी वस्तु का विचार किया जाता है। निक्षेप के चार भेद हैं- नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। इसी तरह नयों के कई प्रकार से कई भेद किये गए हैं। सप्तभङ्गी 'स्याद्वाद' का ही विस्तार है।