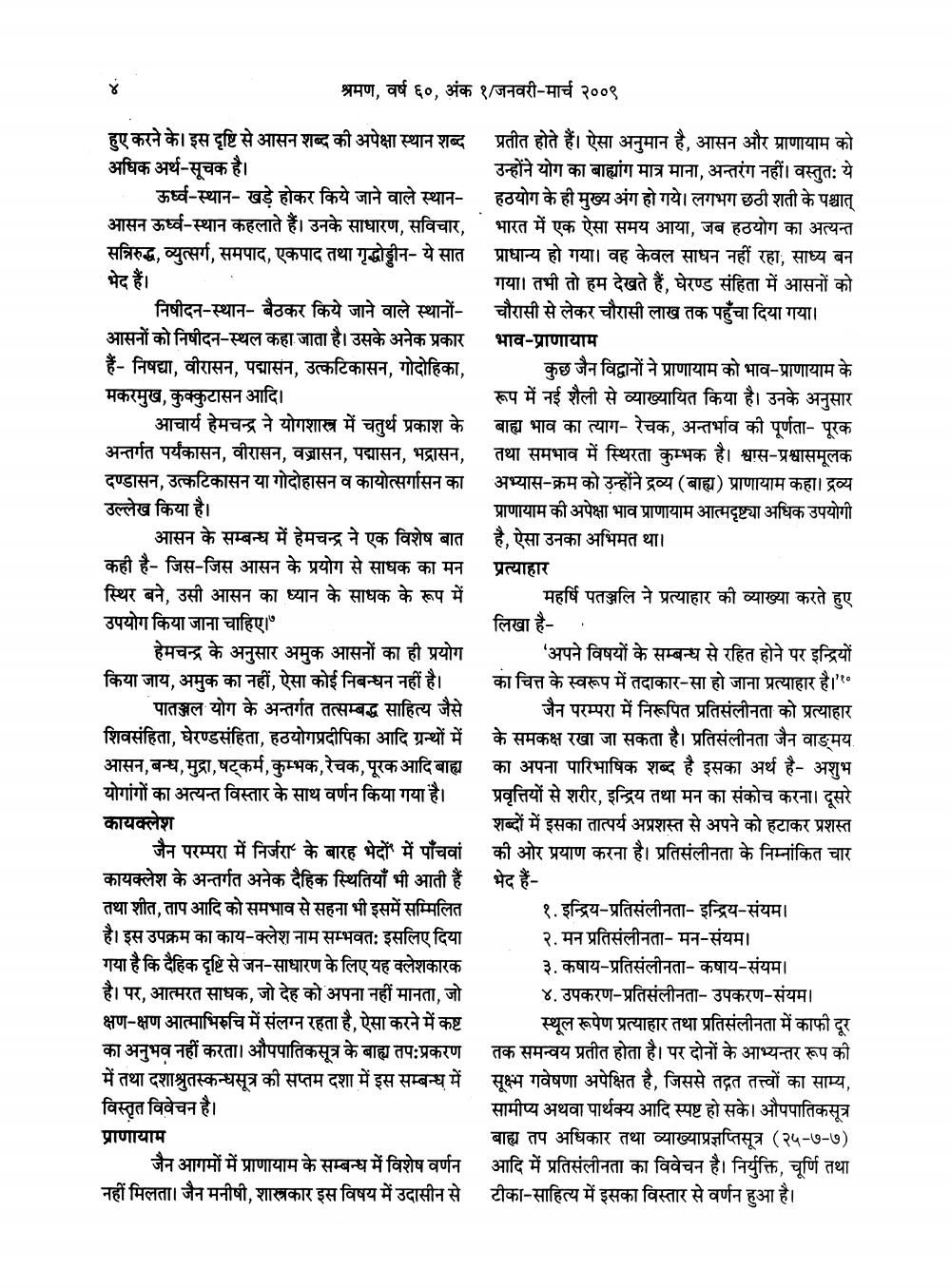________________
श्रमण, वर्ष ६०, अंक १/जनवरी-मार्च २००९
हुए करने के। इस दृष्टि से आसन शब्द की अपेक्षा स्थान शब्द प्रतीत होते हैं। ऐसा अनुमान है, आसन और प्राणायाम को अधिक अर्थ-सूचक है।
उन्होंने योग का बाह्यांग मात्र माना, अन्तरंग नहीं। वस्तुत: ये ऊर्ध्व-स्थान- खड़े होकर किये जाने वाले स्थान- हठयोग के ही मुख्य अंग हो गये। लगभग छठी शती के पश्चात् आसन ऊर्ध्व-स्थान कहलाते हैं। उनके साधारण, सविचार, भारत में एक ऐसा समय आया, जब हठयोग का अत्यन्त सन्निरुद्ध, व्युत्सर्ग, समपाद, एकपाद तथा गृद्घोड्डीन- ये सात प्राधान्य हो गया। वह केवल साधन नहीं रहा, साध्य बन भेद हैं।
गया। तभी तो हम देखते हैं, घेरण्ड संहिता में आसनों को ___निषीदन-स्थान- बैठकर किये जाने वाले स्थानों- चौरासी से लेकर चौरासी लाख तक पहुँचा दिया गया। आसनों को निषीदन-स्थल कहा जाता है। उसके अनेक प्रकार भाव-प्राणायाम हैं-निषद्या, वीरासन, पद्मासन, उत्कटिकासन, गोदोहिका, कुछ जैन विद्वानों ने प्राणायाम को भाव-प्राणायाम के मकरमुख, कुक्कुटासन आदि।
रूप में नई शैली से व्याख्यायित किया है। उनके अनुसार आचार्य हेमचन्द्र ने योगशास्त्र में चतुर्थ प्रकाश के बाह्य भाव का त्याग- रेचक, अन्तर्भाव की पूर्णता- पूरक अन्तर्गत पर्यकासन, वीरासन, वज्रासन, पद्मासन, भद्रासन, तथा समभाव में स्थिरता कुम्भक है। श्वास-प्रश्वासमूलक दण्डासन, उत्कटिकासन या गोदोहासन व कायोत्सर्गासन का अभ्यास-क्रम को उन्होंने द्रव्य (बाह्य) प्राणायाम कहा। द्रव्य उल्लेख किया है।
प्राणायाम की अपेक्षा भाव प्राणायाम आत्मदृष्ट्या अधिक उपयोगी ___ आसन के सम्बन्ध में हेमचन्द्र ने एक विशेष बात है, ऐसा उनका अभिमत था। कही है- जिस-जिस आसन के प्रयोग से साधक का मन प्रत्याहार स्थिर बने, उसी आसन का ध्यान के साधक के रूप में महर्षि पतञ्जलि ने प्रत्याहार की व्याख्या करते हुए उपयोग किया जाना चाहिए।"
लिखा है- . हेमचन्द्र के अनुसार अमुक आसनों का ही प्रयोग 'अपने विषयों के सम्बन्ध से रहित होने पर इन्द्रियों किया जाय, अमुक का नहीं, ऐसा कोई निबन्धन नहीं है। का चित्त के स्वरूप में तदाकार-सा हो जाना प्रत्याहार है।१०
पातञ्जल योग के अन्तर्गत तत्सम्बद्ध साहित्य जैसे जैन परम्परा में निरूपित प्रतिसंलीनता को प्रत्याहार शिवसंहिता.घेरण्डसंहिता. हठयोगप्रदीपिका आदि ग्रन्थों में के समकक्ष रखा जा सकता है। प्रतिसंलीनता आसन,बन्ध, मुद्रा, षट्कर्म,कुम्भक,रेचक, पूरक आदि बाह्य का अपना पारिभाषिक शब्द है इसका अर्थ है- अशुभ योगांगों का अत्यन्त विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। प्रवृत्तियों से शरीर, इन्द्रिय तथा मन का संकोच करना। दूसरे कायक्लेश
शब्दों में इसका तात्पर्य अप्रशस्त से अपने को हटाकर प्रशस्त जैन परम्परा में निर्जरा के बारह भेदों में पाँचवां की ओर प्रयाण करना है। प्रतिसंलीनता के निम्नांकित चार कायक्लेश के अन्तर्गत अनेक दैहिक स्थितियाँ भी आती हैं भेद हैंतथा शीत, ताप आदि को समभाव से सहना भी इसमें सम्मिलित १. इन्द्रिय-प्रतिसंलीनता- इन्द्रिय-संयम। है। इस उपक्रम का काय-क्लेश नाम सम्भवतः इसलिए दिया २.मन प्रतिसंलीनता- मन-संयम। गया है कि दैहिक दृष्टि से जन-साधारण के लिए यह क्लेशकारक ३. कषाय-प्रतिसंलीनता- कषाय-संयम। है। पर, आत्मरत साधक, जो देह को अपना नहीं मानता, जो ४. उपकरण-प्रतिसंलीनता-उपकरण-संयम। क्षण-क्षण आत्माभिरुचि में संलग्न रहता है, ऐसा करने में कष्ट स्थूल रूपेण प्रत्याहार तथा प्रतिसंलीनता में काफी दूर का अनुभव नहीं करता। औपपातिकसूत्र के बाह्य तपःप्रकरण तक समन्वय प्रतीत होता है। पर दोनों के आभ्यन्तर रूप की में तथा दशाश्रुतस्कन्धसूत्र की सप्तम दशा में इस सम्बन्ध में सूक्ष्म गवेषणा अपेक्षित है, जिससे तद्गत तत्त्वों का साम्य, विस्तृत विवेचन है।
सामीप्य अथवा पार्थक्य आदि स्पष्ट हो सके। औपपातिकसूत्र प्राणायाम
बाह्य तप अधिकार तथा व्याख्याप्रज्ञप्तिसूत्र (२५-७-७) जैन आगमों में प्राणायाम के सम्बन्ध में विशेष वर्णन आदि में प्रतिसंलीनता का विवेचन है। नियुक्ति, चूर्णि तथा नहीं मिलता। जैन मनीषी, शास्त्रकार इस विषय में उदासीन से टीका-साहित्य में इसका विस्तार से वर्णन हआ है।