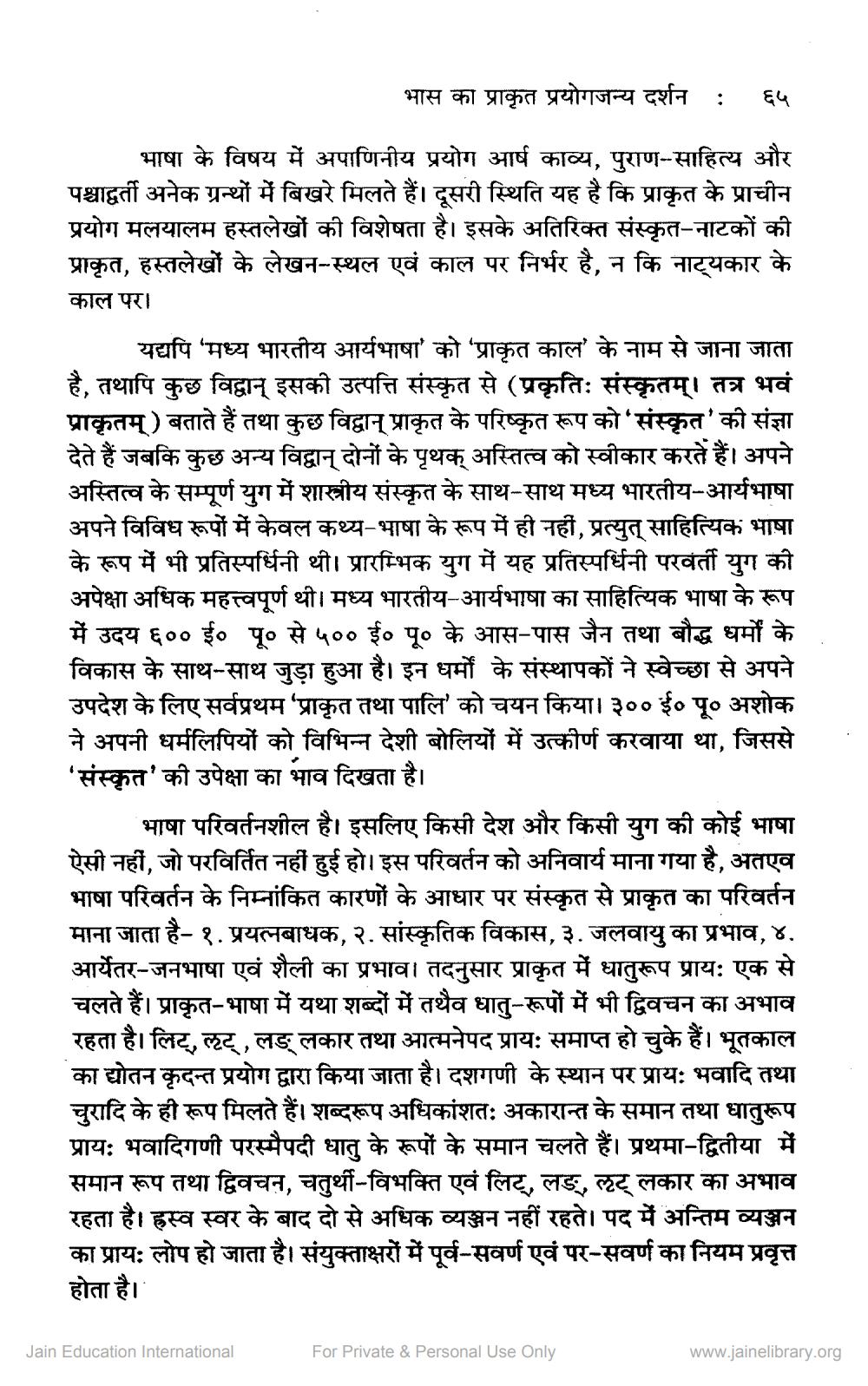________________
भास का प्राकृत प्रयोगजन्य दर्शन : ६५
भाषा के विषय में अपाणिनीय प्रयोग आर्ष काव्य, पुराण- साहित्य और पश्चाद्वर्ती अनेक ग्रन्थों में बिखरे मिलते हैं। दूसरी स्थिति यह है कि प्राकृत के प्राचीन प्रयोग मलयालम हस्तलेखों की विशेषता है। इसके अतिरिक्त संस्कृत - नाटकों की प्राकृत, हस्तलेखों के लेखन-स्थल एवं काल पर निर्भर है, न कि नाट्यकार के
काल पर।
यद्यपि 'मध्य भारतीय आर्यभाषा' को 'प्राकृत काल' के नाम से जाना जाता है, तथापि कुछ विद्वान् इसकी उत्पत्ति संस्कृत से ( प्रकृतिः संस्कृतम् । तत्र भवं प्राकृतम्) बताते हैं तथा कुछ विद्वान् प्राकृत के परिष्कृत रूप को 'संस्कृत' की संज्ञा देते हैं जबकि कुछ अन्य विद्वान् दोनों के पृथक् अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। अपने अस्तित्व के सम्पूर्ण युग में शास्त्रीय संस्कृत के साथ-साथ मध्य भारतीय- आर्यभाषा अपने विविध रूपों में केवल कथ्य-भाषा के रूप में ही नहीं, प्रत्युत् साहित्यिक भाषा के रूप में भी प्रतिस्पर्धिनी थी । प्रारम्भिक युग में यह प्रतिस्पर्धिनी परवर्ती युग की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण थी। मध्य भारतीय - आर्यभाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में उदय ६०० ई० पू० से ५०० ई० पू० के आस-पास जैन तथा बौद्ध धर्मों के विकास के साथ-साथ जुड़ा हुआ है। इन धर्मों के संस्थापकों ने स्वेच्छा से अपने उपदेश के लिए सर्वप्रथम 'प्राकृत तथा पालि' को चयन किया । ३०० ई० पू० अशोक ने अपनी धर्मलिपियों को विभिन्न देशी बोलियों में उत्कीर्ण करवाया था, जिससे 'संस्कृत' की उपेक्षा का भाव दिखता है।
भाषा परिवर्तनशील है। इसलिए किसी देश और किसी युग की कोई भाषा ऐसी नहीं, जो परविर्तित नहीं हुई हो। इस परिवर्तन को अनिवार्य माना गया है, अतएव भाषा परिवर्तन के निम्नांकित कारणों के आधार पर संस्कृत से प्राकृत का परिवर्तन माना जाता है - १. प्रयत्नबाधक, २. सांस्कृतिक विकास, ३. जलवायु का प्रभाव, ४ . आर्येतर - जनभाषा एवं शैली का प्रभाव । तदनुसार प्राकृत में धातुरूप प्राय: एक से चलते हैं। प्राकृत-भाषा में यथा शब्दों में तथैव धातु-रूपों में भी द्विवचन का अभाव रहता है। लिट्, ऌट्, लङ् लकार तथा आत्मनेपद प्रायः समाप्त हो चुके हैं। भूतकाल का द्योतन कृदन्त प्रयोग द्वारा किया जाता है। दशगणी के स्थान पर प्रायः भवादि तथा चुरादि के ही रूप मिलते हैं। शब्दरूप अधिकांशतः अकारान्त के समान तथा धातुरूप प्रायः भवादिगणी परस्मैपदी धातु के रूपों के समान चलते हैं। प्रथमा द्वितीया में समान रूप तथा द्विवचन, चतुर्थी विभक्ति एवं लिट्, लङ, ऌट् लकार का अभाव रहता है। ह्रस्व स्वर के बाद दो से अधिक व्यञ्जन नहीं रहते। पद में अन्तिम व्यञ्जन का प्रायः लोप हो जाता है। संयुक्ताक्षरों में पूर्व-सवर्ण एवं पर-सवर्ण का नियम प्रवृत्त होता है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org