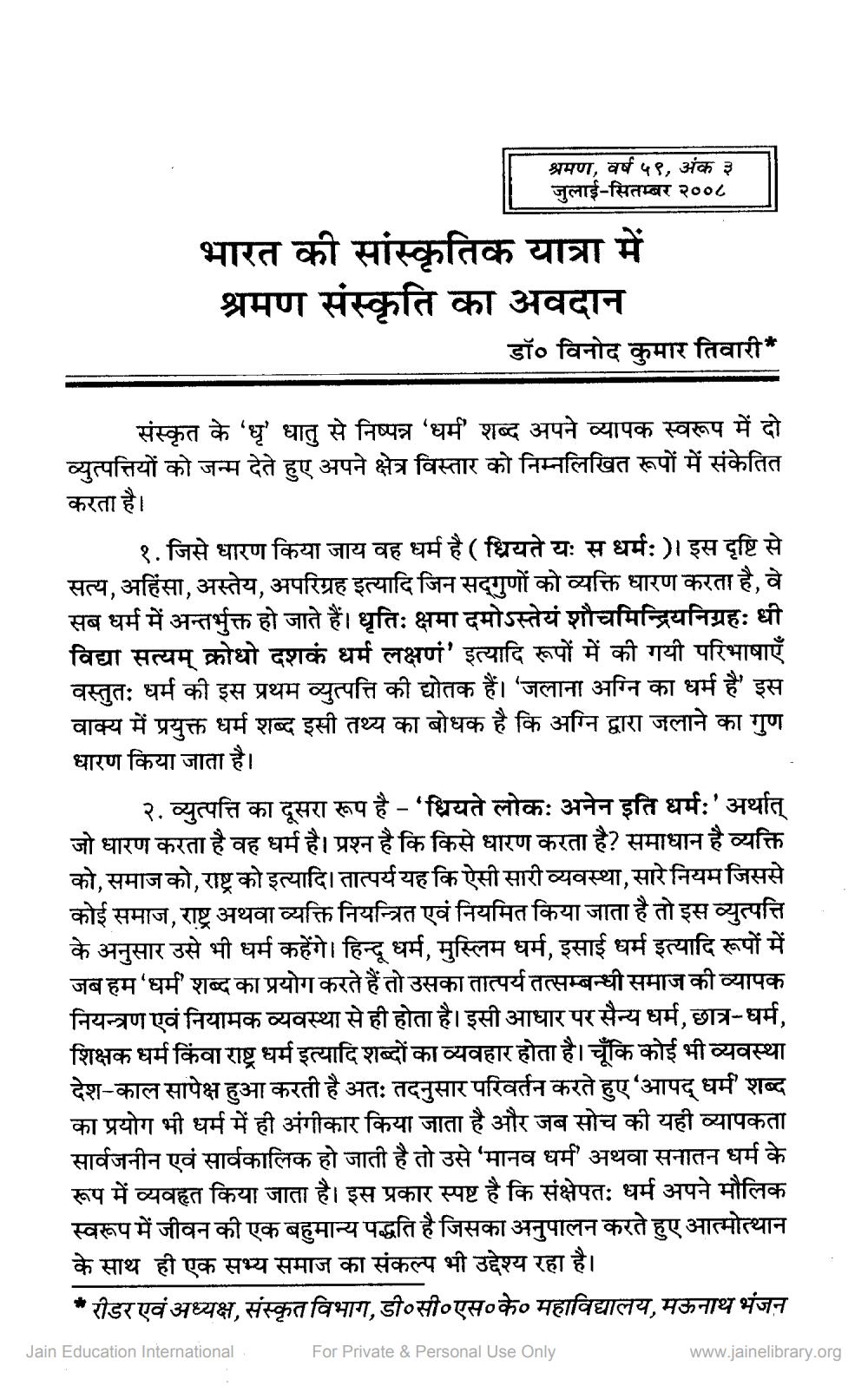________________
श्रमण, वर्ष ५९, अंक ३ जुलाई-सितम्बर २००८
भारत की सांस्कृतिक यात्रा में श्रमण संस्कृति का अवदान
डॉ० विनोद कमार तिवारी*
।
संस्कृत के 'धृ' धातु से निष्पन्न 'धर्म' शब्द अपने व्यापक स्वरूप में दो व्युत्पत्तियों को जन्म देते हुए अपने क्षेत्र विस्तार को निम्नलिखित रूपों में संकेतित करता है।
१.जिसे धारण किया जाय वह धर्म है (ध्रियते यः स धर्मः)। इस दृष्टि से सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह इत्यादि जिन सद्गुणों को व्यक्ति धारण करता है, वे सब धर्म में अन्तर्भुक्त हो जाते हैं। धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः धी विद्या सत्यम् क्रोधो दशकं धर्म लक्षणं' इत्यादि रूपों में की गयी परिभाषाएँ वस्तुतः धर्म की इस प्रथम व्युत्पत्ति की द्योतक हैं। ‘जलाना अग्नि का धर्म है इस वाक्य में प्रयुक्त धर्म शब्द इसी तथ्य का बोधक है कि अग्नि द्वारा जलाने का गुण धारण किया जाता है।
२. व्युत्पत्ति का दूसरा रूप है - 'धियते लोकः अनेन इति धर्मः' अर्थात् जो धारण करता है वह धर्म है। प्रश्न है कि किसे धारण करता है? समाधान है व्यक्ति को,समाजको, राष्ट्र को इत्यादि। तात्पर्य यह कि ऐसी सारी व्यवस्था,सारे नियमजिससे कोई समाज, राष्ट्र अथवा व्यक्ति नियन्त्रित एवं नियमित किया जाता है तो इस व्युत्पत्ति के अनुसार उसे भी धर्म कहेंगे। हिन्दू धर्म, मुस्लिम धर्म, इसाई धर्म इत्यादि रूपों में जब हम 'धर्म' शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका तात्पर्य तत्सम्बन्धी समाज की व्यापक नियन्त्रण एवं नियामक व्यवस्था से ही होता है। इसी आधार पर सैन्य धर्म,छात्र-धर्म, शिक्षक धर्म किंवा राष्ट्र धर्म इत्यादि शब्दों का व्यवहार होता है। चूँकि कोई भी व्यवस्था देश-काल सापेक्ष हुआ करती है अतः तदनुसार परिवर्तन करते हुए आपद् धर्म शब्द का प्रयोग भी धर्म में ही अंगीकार किया जाता है और जब सोच की यही व्यापकता सार्वजनीन एवं सार्वकालिक हो जाती है तो उसे 'मानव धर्म अथवा सनातन धर्म के रूप में व्यवहृत किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संक्षेपत: धर्म अपने मौलिक स्वरूप में जीवन की एक बहुमान्य पद्धति है जिसका अनुपालन करते हुए आत्मोत्थान के साथ ही एक सभ्य समाज का संकल्प भी उद्देश्य रहा है।
* रीडर एवं अध्यक्ष, संस्कृत विभाग,डी०सी०एस०के० महाविद्यालय, मऊनाथ भंजन Jain Education International For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org