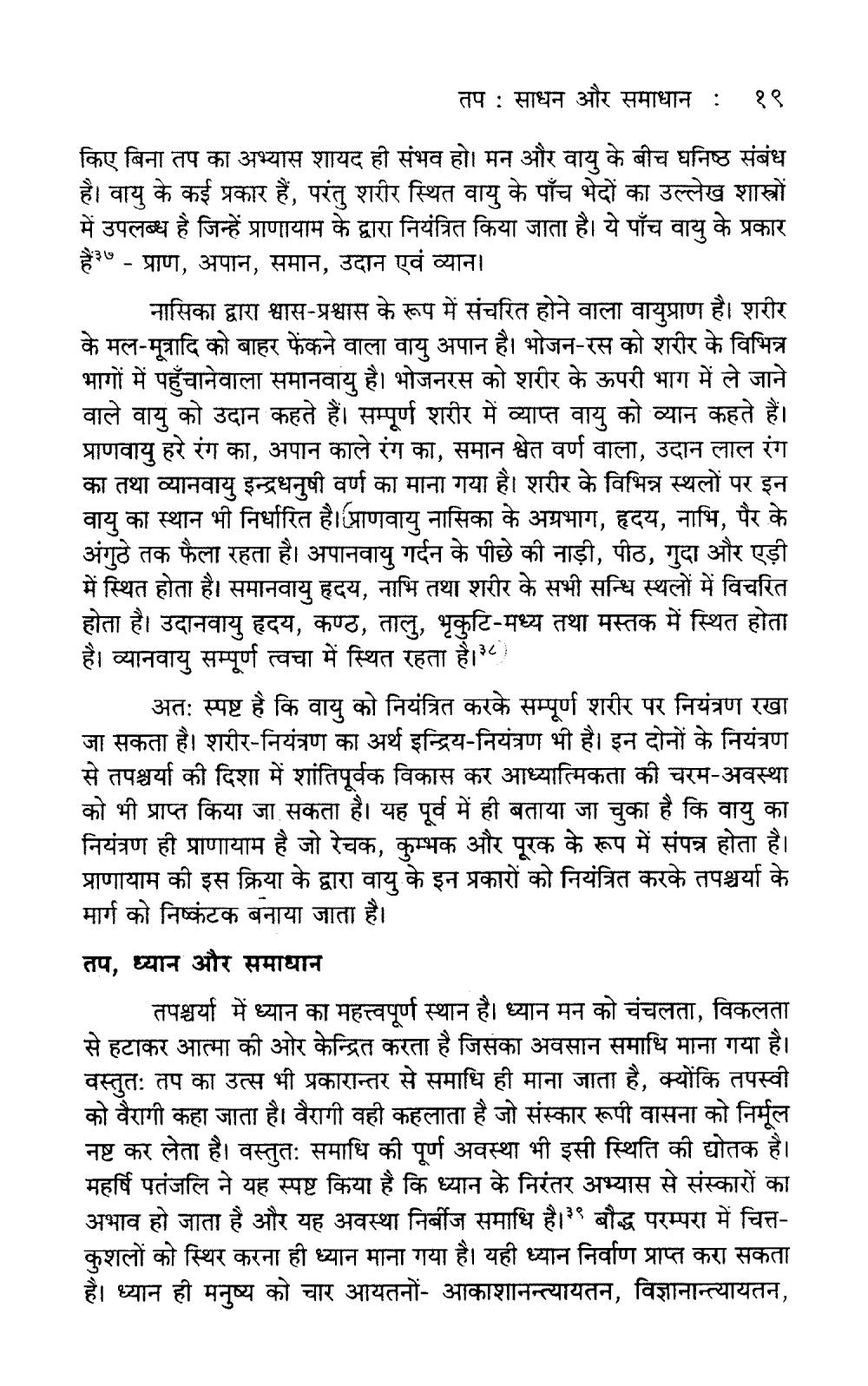________________
तप : साधन और समाधान : १९
किए बिना तप का अभ्यास शायद ही संभव हो। मन और वायु के बीच घनिष्ठ संबंध है। वायु के कई प्रकार हैं, परंतु शरीर स्थित वायु के पाँच भेदों का उल्लेख शास्त्रों में उपलब्ध है जिन्हें प्राणायाम के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये पाँच वायु के प्रकार हैं ३७ - प्राण, अपान, समान, उदान एवं व्यान ।
नासिका द्वारा श्वास-प्रश्वास के रूप में संचरित होने वाला वायुप्राण है। शरीर मल-मूत्रादि को बाहर फेंकने वाला वायु अपान है। भोजन - रस को शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचानेवाला समानवायु है । भोजनरस को शरीर के ऊपरी भाग में ले जाने वाले वायु को उदान कहते हैं। सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त वायु को व्यान कहते हैं। प्राणवायु हरे रंग का, अपान काले रंग का, समान श्वेत वर्ण वाला, उदान लाल रंग का तथा व्यानवायु इन्द्रधनुषी वर्ण का माना गया है। शरीर के विभिन्न स्थलों पर इन वायु का स्थान भी निर्धारित है। प्राणवायु नासिका के अग्रभाग, हृदय, नाभि, पैर के अंगुठे तक फैला रहता है । अपानवायु गर्दन के पीछे की नाड़ी, पीठ, गुदा और एड़ी में स्थित होता है। समानवायु हृदय, नाभि तथा शरीर के सभी सन्धि स्थलों में विचरित होता है । उदानवायु हृदय, कण्ठ, तालु, भृकुटि मध्य तथा मस्तक में स्थित होता है। व्यानवायु सम्पूर्ण त्वचा में स्थित रहता है । ३८)
अतः स्पष्ट है कि वायु को नियंत्रित करके सम्पूर्ण शरीर पर नियंत्रण रखा जा सकता है। शरीर नियंत्रण का अर्थ इन्द्रिय-नियंत्रण भी है। इन दोनों के नियंत्रण से तपश्चर्या की दिशा में शांतिपूर्वक विकास कर आध्यात्मिकता की चरम अवस्था को भी प्राप्त किया जा सकता है। यह पूर्व में ही बताया जा चुका है कि वायु का नियंत्रण ही प्राणायाम है जो रेचक, कुम्भक और पूरक के रूप में संपन्न होता है। प्राणायाम की इस क्रिया के द्वारा वायु के इन प्रकारों को नियंत्रित करके तपश्चर्या के मार्ग को निष्कंटक बनाया जाता है।
तप, ध्यान और समाधान
तपश्चर्या में ध्यान का महत्त्वपूर्ण स्थान है। ध्यान मन को चंचलता, विकलता से हटाकर आत्मा की ओर केन्द्रित करता है जिसका अवसान समाधि माना गया है। वस्तुतः तप का उत्स भी प्रकारान्तर से समाधि ही माना जाता है, क्योंकि तपस्वी को वैरागी कहा जाता है। वैरागी वही कहलाता है जो संस्कार रूपी वासना को निर्मूल नष्ट कर लेता है। वस्तुतः समाधि की पूर्ण अवस्था भी इसी स्थिति की द्योतक है। महर्षि पतंजलि ने यह स्पष्ट किया हैं कि ध्यान के निरंतर अभ्यास से संस्कारों का अभाव हो जाता हैं और यह अवस्था निर्बीज समाधि है । ३९ बौद्ध परम्परा में चित्तकुशलों को स्थिर करना ही ध्यान माना गया है। यही ध्यान निर्वाण प्राप्त करा सकता है। ध्यान ही मनुष्य को चार आयतनों- आकाशानन्त्यायतन, विज्ञानान्त्यायतन,