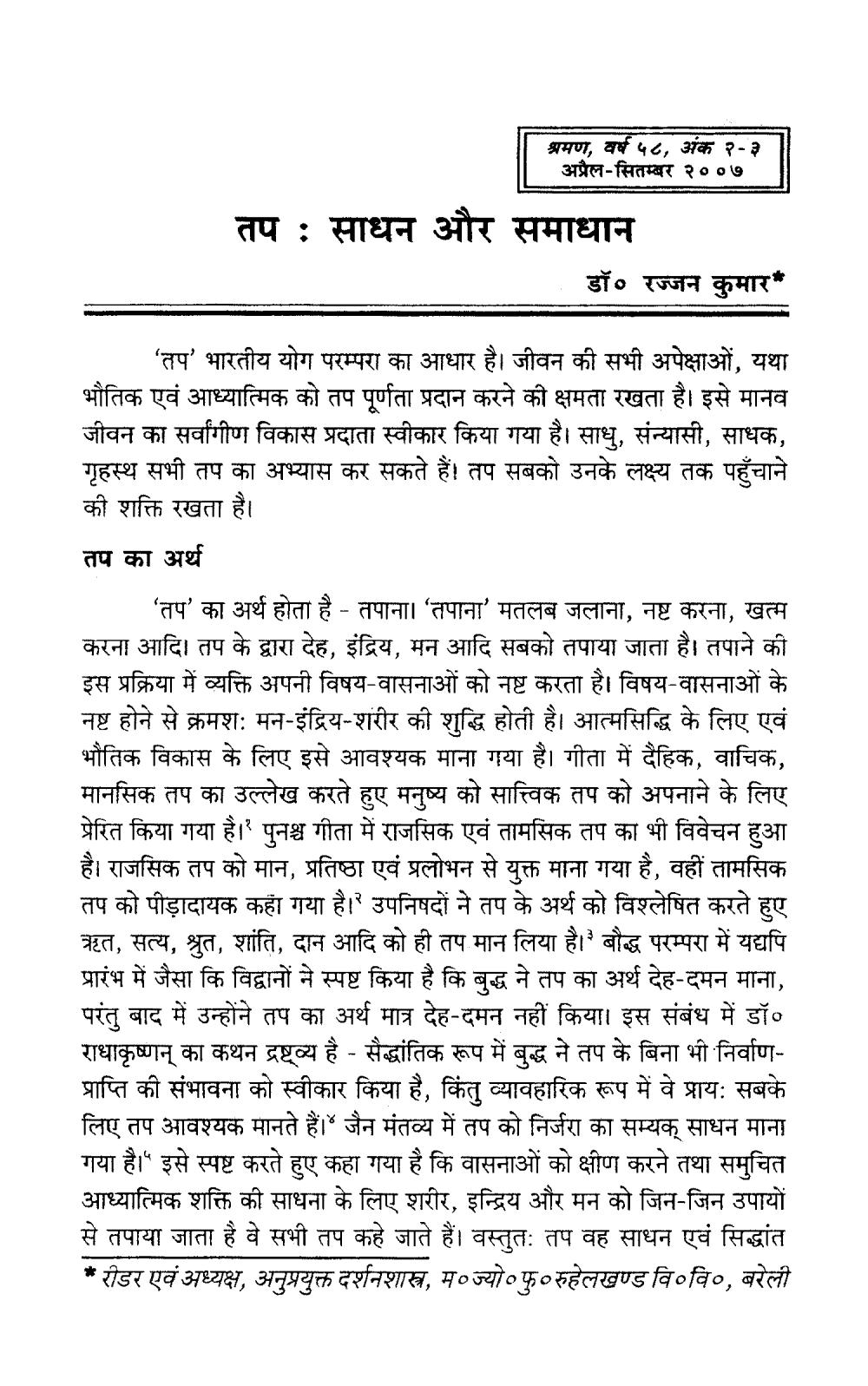________________
-
श्रमण, वर्ष ५८, अंक २-३ अप्रैल-सितम्बर २००७
तप : साधन और समाधान
डॉ० रज्जन कुमार*
'तप' भारतीय योग परम्परा का आधार है। जीवन की सभी अपेक्षाओं, यथा भौतिक एवं आध्यात्मिक को तप पूर्णता प्रदान करने की क्षमता रखता है। इसे मानव जीवन का सर्वांगीण विकास प्रदाता स्वीकार किया गया है। साधु, संन्यासी, साधक, गृहस्थ सभी तप का अभ्यास कर सकते हैं। तप सबको उनके लक्ष्य तक पहुँचाने की शक्ति रखता है। तप का अर्थ
__ 'तप' का अर्थ होता है - तपाना। 'तपाना' मतलब जलाना, नष्ट करना, खत्म करना आदि। तप के द्वारा देह, इंद्रिय, मन आदि सबको तपाया जाता है। तपाने की इस प्रक्रिया में व्यक्ति अपनी विषय-वासनाओं को नष्ट करता है। विषय-वासनाओं के नष्ट होने से क्रमश: मन-इंद्रिय-शरीर की शुद्धि होती है। आत्मसिद्धि के लिए एवं भौतिक विकास के लिए इसे आवश्यक माना गया है। गीता में दैहिक, वाचिक, मानसिक तप का उल्लेख करते हुए मनुष्य को सात्त्विक तप को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है।' पुनश्च गीता में राजसिक एवं तामसिक तप का भी विवेचन हुआ है। राजसिक तप को मान, प्रतिष्ठा एवं प्रलोभन से युक्त माना गया है, वहीं तामसिक तप को पीड़ादायक कहा गया है। उपनिषदों ने तप के अर्थ को विश्लेषित करते हए ऋत, सत्य, श्रत, शांति, दान आदि को ही तप मान लिया है। बौद्ध परम्परा में यद्यपि प्रारंभ में जैसा कि विद्वानों ने स्पष्ट किया है कि बुद्ध ने तप का अर्थ देह-दमन माना, परंतु बाद में उन्होंने तप का अर्थ मात्र देह-दमन नहीं किया। इस संबंध में डॉ० राधाकृष्णन् का कथन द्रष्टव्य है - सैद्धांतिक रूप में बुद्ध ने तप के बिना भी निर्वाणप्राप्ति की संभावना को स्वीकार किया है, किंतु व्यावहारिक रूप में वे प्रायः सबके लिए तप आवश्यक मानते हैं। जैन मंतव्य में तप को निर्जरा का सम्यक् साधन माना गया है। इसे स्पष्ट करते हए कहा गया है कि वासनाओं को क्षीण करने तथा समुचित आध्यात्मिक शक्ति की साधना के लिए शरीर, इन्द्रिय और मन को जिन-जिन उपायों से तपाया जाता है वे सभी तप कहे जाते हैं। वस्तुत: तप वह साधन एवं सिद्धांत * रीडर एवं अध्यक्ष, अनुप्रयुक्त दर्शनशास्त्र, म०ज्यो० फु०रुहेलखण्ड वि०वि०, बरेली