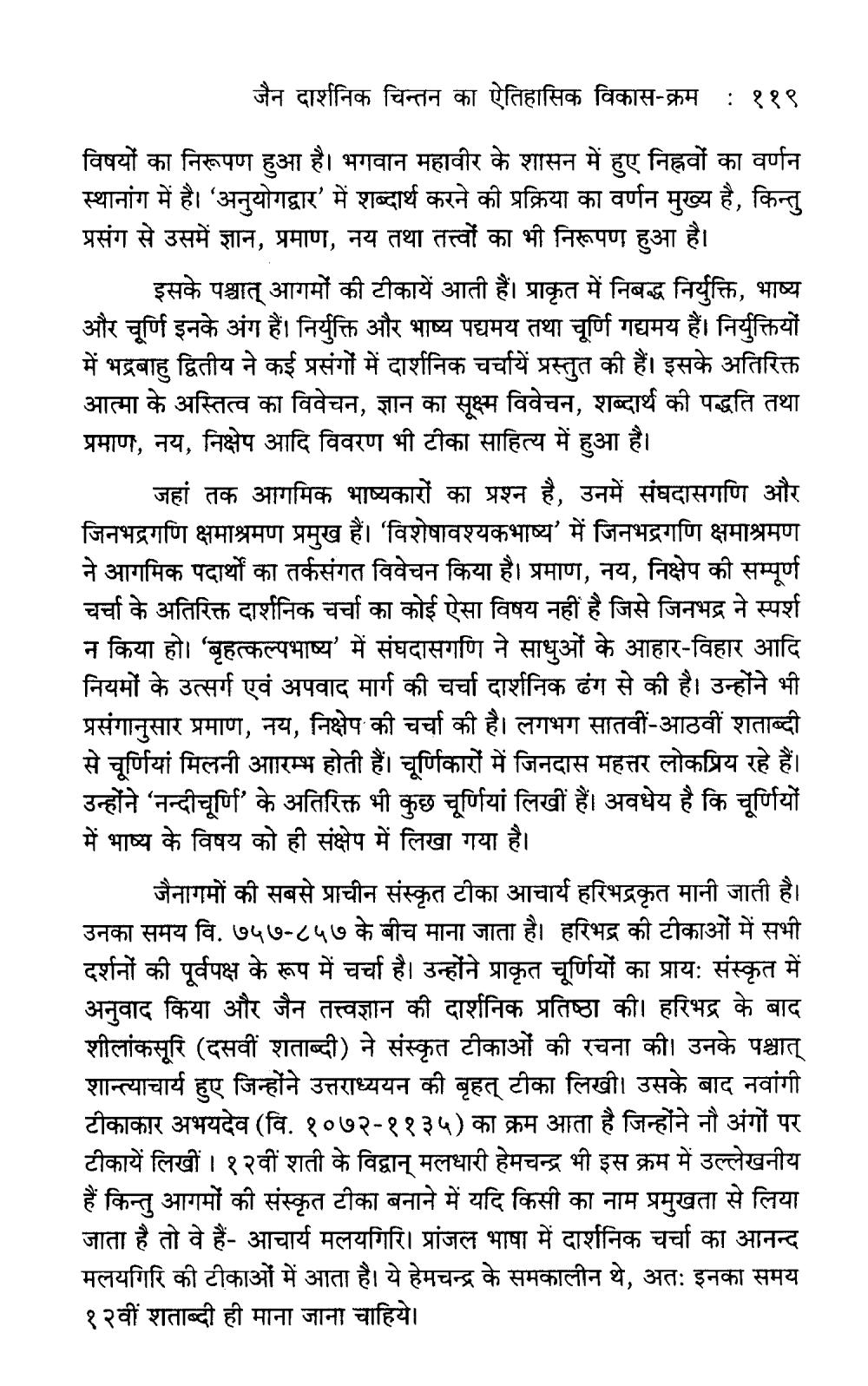________________
जैन दार्शनिक चिन्तन का ऐतिहासिक विकास-क्रम : ११९
विषयों का निरूपण हुआ है। भगवान महावीर के शासन में हुए निह्नवों का वर्णन स्थानांग में है। ‘अनुयोगद्वार' में शब्दार्थ करने की प्रक्रिया का वर्णन मुख्य है, किन्तु प्रसंग से उसमें ज्ञान, प्रमाण, नय तथा तत्त्वों का भी निरूपण हुआ है।
इसके पश्चात् आगमों की टीकायें आती हैं। प्राकृत में निबद्ध नियुक्ति, भाष्य और चूर्णि इनके अंग हैं। नियुक्ति और भाष्य पद्यमय तथा चूर्णि गद्यमय हैं। नियुक्तियों में भद्रबाहु द्वितीय ने कई प्रसंगों में दार्शनिक चर्चायें प्रस्तुत की हैं। इसके अतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व का विवेचन, ज्ञान का सूक्ष्म विवेचन, शब्दार्थ की पद्धति तथा प्रमाण, नय, निक्षेप आदि विवरण भी टीका साहित्य में हुआ है।
जहां तक आगमिक भाष्यकारों का प्रश्न है, उनमें संघदासगणि और जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण प्रमुख हैं। 'विशेषावश्यकभाष्य' में जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण ने आगमिक पदार्थों का तर्कसंगत विवेचन किया है। प्रमाण, नय, निक्षेप की सम्पूर्ण चर्चा के अतिरिक्त दार्शनिक चर्चा का कोई ऐसा विषय नहीं है जिसे जिनभद्र ने स्पर्श न किया हो। 'बृहत्कल्पभाष्य' में संघदासगणि ने साधुओं के आहार-विहार आदि नियमों के उत्सर्ग एवं अपवाद मार्ग की चर्चा दार्शनिक ढंग से की है। उन्होंने भी प्रसंगानुसार प्रमाण, नय, निक्षेप की चर्चा की है। लगभग सातवीं-आठवीं शताब्दी से चूर्णियां मिलनी आरम्भ होती हैं। चूर्णिकारों में जिनदास महत्तर लोकप्रिय रहे हैं। उन्होंने 'नन्दीचूर्णि' के अतिरिक्त भी कुछ चूर्णियां लिखीं हैं। अवधेय है कि चूर्णियों में भाष्य के विषय को ही संक्षेप में लिखा गया है।
जैनागमों की सबसे प्राचीन संस्कृत टीका आचार्य हरिभद्रकृत मानी जाती है। उनका समय वि. ७५७-८५७ के बीच माना जाता है। हरिभद्र की टीकाओं में सभी दर्शनों की पूर्वपक्ष के रूप में चर्चा है। उन्होंने प्राकृत चूर्णियों का प्राय: संस्कृत में अनुवाद किया और जैन तत्त्वज्ञान की दार्शनिक प्रतिष्ठा की। हरिभद्र के बाद शीलांकसूरि (दसवीं शताब्दी) ने संस्कृत टीकाओं की रचना की। उनके पश्चात् शान्त्याचार्य हुए जिन्होंने उत्तराध्ययन की बृहत् टीका लिखी। उसके बाद नवांगी टीकाकार अभयदेव (वि. १०७२-११३५) का क्रम आता है जिन्होंने नौ अंगों पर टीकायें लिखीं। १२वीं शती के विद्वान् मलधारी हेमचन्द्र भी इस क्रम में उल्लेखनीय हैं किन्तु आगमों की संस्कृत टीका बनाने में यदि किसी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है तो वे हैं- आचार्य मलयगिरि। प्रांजल भाषा में दार्शनिक चर्चा का आनन्द मलयगिरि की टीकाओं में आता है। ये हेमचन्द्र के समकालीन थे, अत: इनका समय १२वीं शताब्दी ही माना जाना चाहिये।