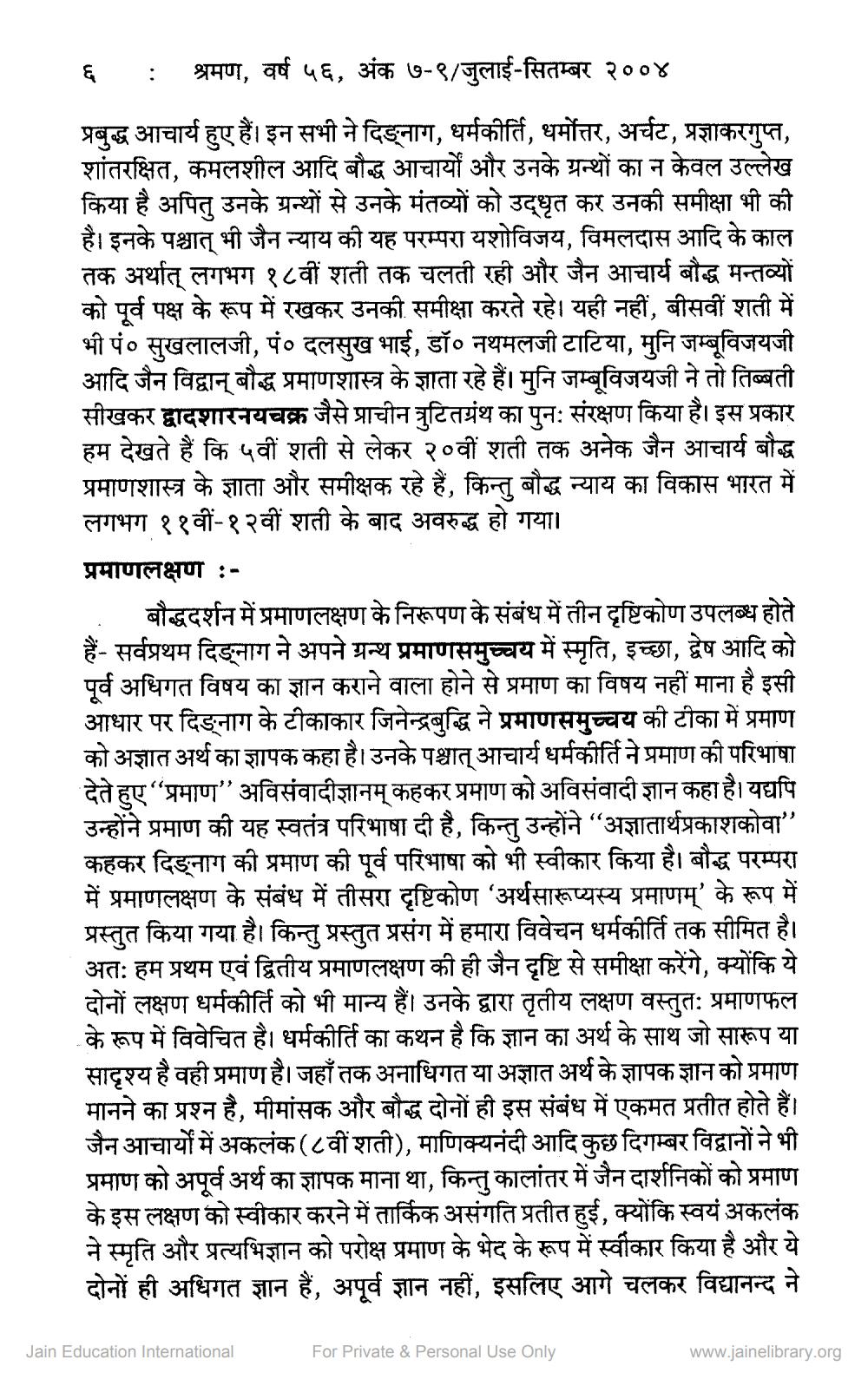________________
श्रमण, वर्ष ५६, अंक ७-९ / जुलाई-सितम्बर २००४
प्रबुद्ध आचार्य हुए हैं। इन सभी ने दिङ्नाग, धर्मकीर्ति, धर्मोत्तर, अर्चट, प्रज्ञाकरगुप्त, शांतरक्षित, कमलशील आदि बौद्ध आचार्यों और उनके ग्रन्थों का न केवल उल्लेख किया है अपितु उनके ग्रन्थों से उनके मंतव्यों को उद्धृत कर उनकी समीक्षा भी की है। इनके पश्चात् भी जैन न्याय की यह परम्परा यशोविजय, विमलदास आदि के काल तक अर्थात् लगभग १८वीं शती तक चलती रही और जैन आचार्य बौद्ध मन्तव्यों को पूर्व पक्ष के रूप में रखकर उनकी समीक्षा करते रहे। यही नहीं, बीसवीं शती में भी पं० सुखलालजी, पं० दलसुख भाई, डॉ० नथमलजी टाटिया, मुनि जम्बूविजयजी आदि जैन विद्वान् बौद्ध प्रमाणशास्त्र के ज्ञाता रहे हैं। मुनि जम्बूविजयजी ने तो तिब्बती सीखकर द्वादशारनयचक्र जैसे प्राचीन त्रुटितग्रंथ का पुनः संरक्षण किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ५वीं शती से लेकर २०वीं शती तक अनेक जैन आचार्य बौद्ध प्रमाणशास्त्र के ज्ञाता और समीक्षक रहे हैं, किन्तु बौद्ध न्याय का विकास भारत में लगभग ११वीं - १२वीं शती के बाद अवरुद्ध हो गया।
प्रमाणलक्षण :
बौद्धदर्शन में प्रमाणलक्षण के निरूपण के संबंध में तीन दृष्टिकोण उपलब्ध होते हैं- सर्वप्रथम दिङ्नाग ने अपने ग्रन्थ प्रमाणसमुच्चय में स्मृति, इच्छा, द्वेष आदि को पूर्व अधिगत विषय का ज्ञान कराने वाला होने से प्रमाण का विषय नहीं माना है इसी आधार पर दिङ्नाग के टीकाकार जिनेन्द्रबुद्धि ने प्रमाणसमुच्चय की टीका में प्रमाण को अज्ञात अर्थ का ज्ञापक कहा है। उनके पश्चात् आचार्य धर्मकीर्ति ने प्रमाण की परिभाषा देते हुए "प्रमाण" अविसंवादीज्ञानम् कहकर प्रमाण को अविसंवादी ज्ञान कहा है। यद्यपि उन्होंने प्रमाण की यह स्वतंत्र परिभाषा दी है, किन्तु उन्होंने “अज्ञातार्थप्रकाशकोवा” कहकर दिङ्नाग की प्रमाण की पूर्व परिभाषा को भी स्वीकार किया है। बौद्ध परम्परा में प्रमाणलक्षण के संबंध में तीसरा दृष्टिकोण 'अर्थसारूप्यस्य प्रमाणम्' के रूप में प्रस्तुत किया गया है । किन्तु प्रस्तुत प्रसंग में हमारा विवेचन धर्मकीर्ति तक सीमित है। अतः हम प्रथम एवं द्वितीय प्रमाणलक्षण की ही जैन दृष्टि से समीक्षा करेंगे, क्योंकि ये दोनों लक्षण धर्मकीर्ति को भी मान्य हैं। उनके द्वारा तृतीय लक्षण वस्तुतः प्रमाणफल के रूप में विवेचित है। धर्मकीर्ति का कथन है कि ज्ञान का अर्थ के साथ जो सारूप या सादृश्य है वही प्रमाण है। जहाँ तक अनाधिगत या अज्ञात अर्थ के ज्ञापक ज्ञान को प्रमाण मानने का प्रश्न है, मीमांसक और बौद्ध दोनों ही इस संबंध में एकमत प्रतीत होते हैं। जैन आचार्यों में अकलंक (८ वीं शती), माणिक्यनंदी आदि कुछ दिगम्बर विद्वानों ने भी प्रमाण को अपूर्व अर्थ का ज्ञापक माना था, किन्तु कालांतर में जैन दार्शनिकों को प्रमाण के इस लक्षण को स्वीकार करने में तार्किक असंगति प्रतीत हुई, क्योंकि स्वयं अकलंक स्मृति और प्रत्यभिज्ञान को परोक्ष प्रमाण के भेद के रूप में स्वीकार किया है और ये दोनों ही अधिगत ज्ञान हैं, अपूर्व ज्ञान नहीं, इसलिए आगे चलकर विद्यानन्द ने
:
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org