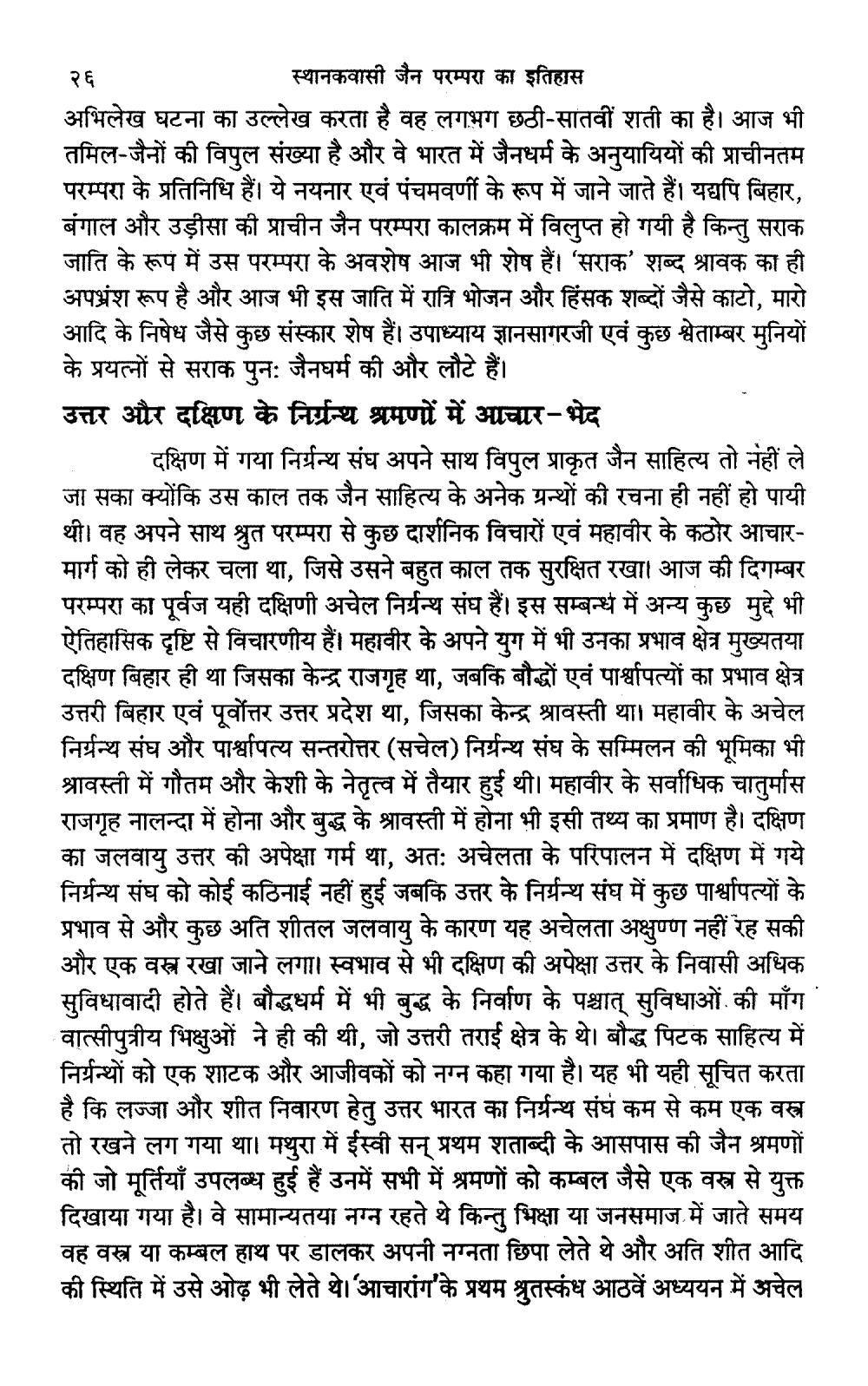________________
२६
स्थानकवासी जैन परम्परा का इतिहास अभिलेख घटना का उल्लेख करता है वह लगभग छठी-सातवीं शती का है। आज भी तमिल-जैनों की विपुल संख्या है और वे भारत में जैनधर्म के अनुयायियों की प्राचीनतम परम्परा के प्रतिनिधि हैं। ये नयनार एवं पंचमवर्णी के रूप में जाने जाते हैं। यद्यपि बिहार, बंगाल और उड़ीसा की प्राचीन जैन परम्परा कालक्रम में विलुप्त हो गयी है किन्तु सराक जाति के रूप में उस परम्परा के अवशेष आज भी शेष हैं। 'सराक' शब्द श्रावक का ही अपभ्रंश रूप है और आज भी इस जाति में रात्रि भोजन और हिंसक शब्दों जैसे काटो, मारो आदि के निषेध जैसे कुछ संस्कार शेष हैं। उपाध्याय ज्ञानसागरजी एवं कुछ श्वेताम्बर मुनियों के प्रयत्नों से सराक पुन: जैनधर्म की और लौटे हैं। उत्तर और दक्षिण के निर्ग्रन्थ श्रमणों में आचार-भेद
दक्षिण में गया निर्ग्रन्थ संघ अपने साथ विप्ल प्राकृत जैन साहित्य तो नहीं ले जा सका क्योंकि उस काल तक जैन साहित्य के अनेक ग्रन्थों की रचना ही नहीं हो पायी थी। वह अपने साथ श्रुत परम्परा से कुछ दार्शनिक विचारों एवं महावीर के कठोर आचारमार्ग को ही लेकर चला था, जिसे उसने बहुत काल तक सुरक्षित रखा। आज की दिगम्बर परम्परा का पूर्वज यही दक्षिणी अचेल निर्ग्रन्थ संघ हैं। इस सम्बन्ध में अन्य कुछ मुद्दे भी ऐतिहासिक दृष्टि से विचारणीय हैं। महावीर के अपने युग में भी उनका प्रभाव क्षेत्र मुख्यतया दक्षिण बिहार ही था जिसका केन्द्र राजगृह था, जबकि बौद्धों एवं पार्थापत्यों का प्रभाव क्षेत्र उत्तरी बिहार एवं पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश था, जिसका केन्द्र श्रावस्ती था। महावीर के अचेल निर्ग्रन्थ संघ और पापित्य सन्तरोत्तर (सचेल) निर्ग्रन्थ संघ के सम्मिलन की भूमिका भी श्रावस्ती में गौतम और केशी के नेतृत्व में तैयार हुई थी। महावीर के सर्वाधिक चातुर्मास राजगृह नालन्दा में होना और बुद्ध के श्रावस्ती में होना भी इसी तथ्य का प्रमाण है। दक्षिण का जलवायु उत्तर की अपेक्षा गर्म था, अत: अचेलता के परिपालन में दक्षिण में गये निर्ग्रन्थ संघ को कोई कठिनाई नहीं हुई जबकि उत्तर के निर्ग्रन्थ संघ में कुछ पार्थापत्यों के प्रभाव से और कुछ अति शीतल जलवायु के कारण यह अचेलता अक्षुण्ण नहीं रह सकी
और एक वस्त्र रखा जाने लगा। स्वभाव से भी दक्षिण की अपेक्षा उत्तर के निवासी अधिक सविधावादी होते हैं। बौद्धधर्म में भी बुद्ध के निर्वाण के पश्चात् सुविधाओं की माँग वात्सीपुत्रीय भिक्षुओं ने ही की थी, जो उत्तरी तराई क्षेत्र के थे। बौद्ध पिटक साहित्य में निर्ग्रन्थों को एक शाटक और आजीवकों को नग्न कहा गया है। यह भी यही सूचित करता है कि लज्जा और शीत निवारण हेतु उत्तर भारत का निर्ग्रन्थ संघ कम से कम एक वस्त्र तो रखने लग गया था। मथुरा में ईस्वी सन् प्रथम शताब्दी के आसपास की जैन श्रमणों की जो मर्तियाँ उपलब्ध हई हैं उनमें सभी में श्रमणों को कम्बल जैसे एक वस्त्र से युक्त दिखाया गया है। वे सामान्यतया नग्न रहते थे किन्तु भिक्षा या जनसमाज में जाते समय वह वस्त्र या कम्बल हाथ पर डालकर अपनी नग्नता छिपा लेते थे और अति शीत आदि की स्थिति में उसे ओढ़ भी लेते थे। आचारांग' के प्रथम श्रुतस्कंध आठवें अध्ययन में अचेल