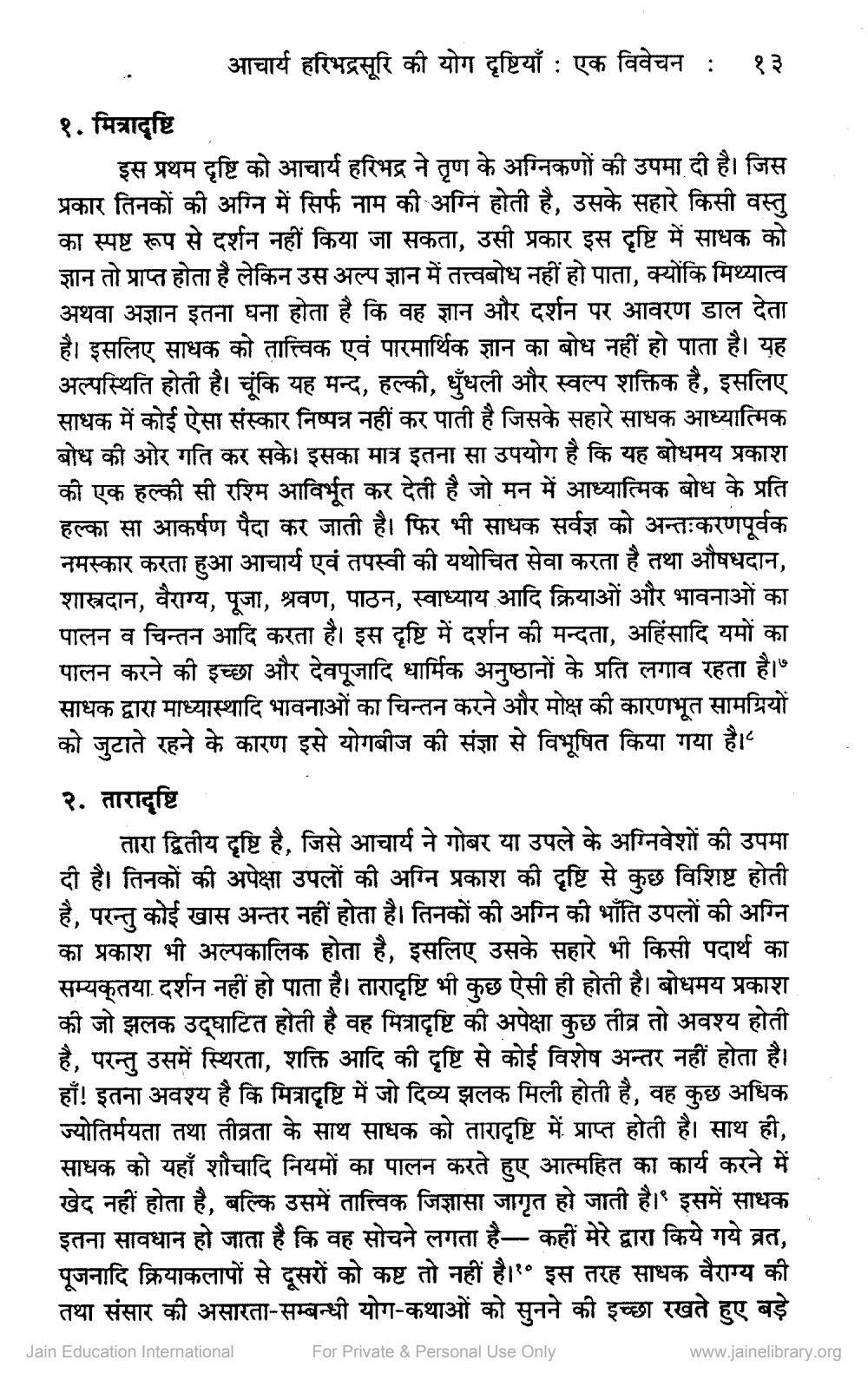________________
आचार्य हरिभद्रसूरि की योग दृष्टियाँ : एक विवेचन : १३
१. मित्रादृष्टि
इस प्रथम दृष्टि को आचार्य हरिभद्र ने तृण के अग्निकणों की उपमा दी है। जिस प्रकार तिनकों की अग्नि में सिर्फ नाम की अग्नि होती है, उसके सहारे किसी वस्तु का स्पष्ट रूप से दर्शन नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार इस दृष्टि में साधक को ज्ञान तो प्राप्त होता है लेकिन उस अल्प ज्ञान में तत्त्वबोध नहीं हो पाता, क्योंकि मिथ्यात्व अथवा अज्ञान इतना घना होता है कि वह ज्ञान और दर्शन पर आवरण डाल देता है। इसलिए साधक को तात्त्विक एवं पारमार्थिक ज्ञान का बोध नहीं हो पाता है। यह अल्पस्थिति होती है। चूंकि यह मन्द, हल्की, धुंधली और स्वल्प शक्तिक है, इसलिए साधक में कोई ऐसा संस्कार निष्पत्र नहीं कर पाती है जिसके सहारे साधक आध्यात्मिक बोध की ओर गति कर सके। इसका मात्र इतना सा उपयोग है कि यह बोधमय प्रकाश की एक हल्की सी रश्मि आविर्भूत कर देती है जो मन में आध्यात्मिक बोध के प्रति हल्का सा आकर्षण पैदा कर जाती है। फिर भी साधक सर्वज्ञ को अन्तःकरणपूर्वक नमस्कार करता हुआ आचार्य एवं तपस्वी की यथोचित सेवा करता है तथा औषधदान, शास्त्रदान, वैराग्य, पूजा, श्रवण, पाठन, स्वाध्याय आदि क्रियाओं और भावनाओं का पालन व चिन्तन आदि करता है। इस दृष्टि में दर्शन की मन्दता, अहिंसादि यमों का पालन करने की इच्छा और देवपूजादि धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति लगाव रहता है।" साधक द्वारा माध्यास्थादि भावनाओं का चिन्तन करने और मोक्ष की कारणभूत सामग्रियों को जुटाते रहने के कारण इसे योगबीज की संज्ञा से विभूषित किया गया है। २. तारादृष्टि
तारा द्वितीय दृष्टि है, जिसे आचार्य ने गोबर या उपले के अग्निवेशों की उपमा दी है। तिनकों की अपेक्षा उपलों की अग्नि प्रकाश की दृष्टि से कुछ विशिष्ट होती है, परन्तु कोई खास अन्तर नहीं होता है। तिनकों की अग्नि की भाँति उपलों की अग्नि का प्रकाश भी अल्पकालिक होता है, इसलिए उसके सहारे भी किसी पदार्थ का सम्यक्तया दर्शन नहीं हो पाता है। तारादृष्टि भी कुछ ऐसी ही होती है। बोधमय प्रकाश की जो झलक उद्घाटित होती है वह मित्रादृष्टि की अपेक्षा कुछ तीव्र तो अवश्य होती है, परन्तु उसमें स्थिरता, शक्ति आदि की दृष्टि से कोई विशेष अन्तर नहीं होता है। हाँ! इतना अवश्य है कि मित्रादृष्टि में जो दिव्य झलक मिली होती है, वह कुछ अधिक ज्योतिर्मयता तथा तीव्रता के साथ साधक को तारादृष्टि में प्राप्त होती है। साथ ही, साधक को यहाँ शौचादि नियमों का पालन करते हुए आत्महित का कार्य करने में खेद नहीं होता है, बल्कि उसमें तात्त्विक जिज्ञासा जागृत हो जाती है। इसमें साधक इतना सावधान हो जाता है कि वह सोचने लगता है- कहीं मेरे द्वारा किये गये व्रत, पूजनादि क्रियाकलापों से दूसरों को कष्ट तो नहीं है। इस तरह साधक वैराग्य की तथा संसार की असारता-सम्बन्धी योग-कथाओं को सुनने की इच्छा रखते हुए बड़े For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org
Jain Education International