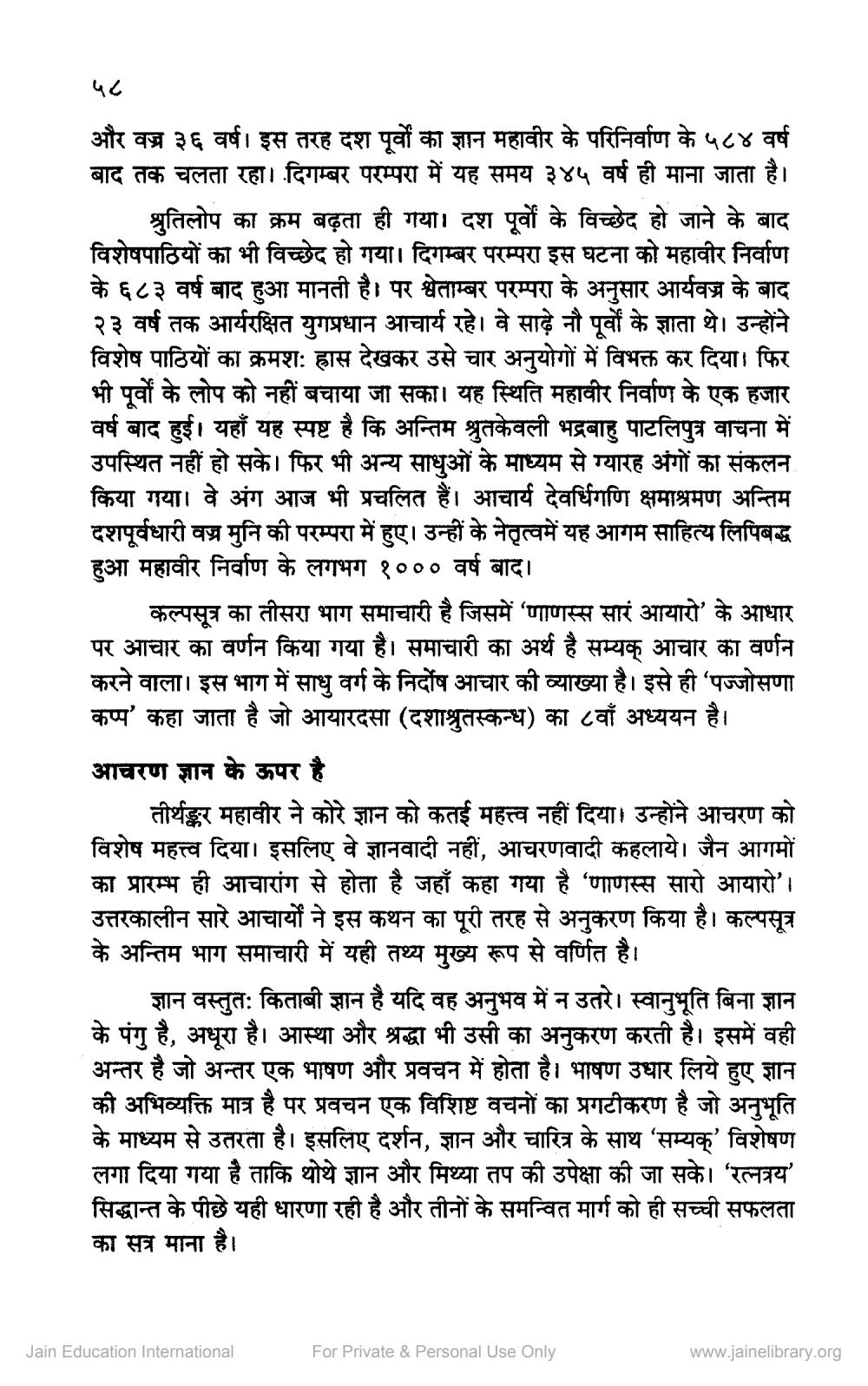________________
५८
और वज्र ३६ वर्ष । इस तरह दश पूर्वो का ज्ञान महावीर के परिनिर्वाण के ५८४ वर्ष बाद तक चलता रहा। दिगम्बर परम्परा में यह समय ३४५ वर्ष ही माना जाता है।
श्रुतिलोप का क्रम बढ़ता ही गया । दश पूर्वों के विच्छेद हो जाने के बाद विशेषपाठियों का भी विच्छेद हो गया। दिगम्बर परम्परा इस घटना को महावीर निर्वाण के ६८३ वर्ष बाद हुआ मानती है। पर श्वेताम्बर परम्परा के अनुसार आर्यवज्र के बाद २३ वर्ष तक आर्यरक्षित युगप्रधान आचार्य रहे। वे साढ़े नौ पूर्वों के ज्ञाता थे। उन्होंने विशेष पाठियों का क्रमशः ह्रास देखकर उसे चार अनुयोगों में विभक्त कर दिया। फिर भी पूर्वों के लोप को नहीं बचाया जा सका। यह स्थिति महावीर निर्वाण के एक हजार वर्ष बाद हुई। यहाँ यह स्पष्ट है कि अन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहु पाटलिपुत्र वाचना में उपस्थित नहीं हो सके। फिर भी अन्य साधुओं के माध्यम से ग्यारह अंगों का संकलन किया गया। वे अंग आज भी प्रचलित हैं। आचार्य देवर्धिगणि क्षमाश्रमण अन्तिम दशपूर्वधारी वज्र मुनि की परम्परा में हुए। उन्हीं के नेतृत्वमें यह आगम साहित्य लिपिबद्ध हुआ महावीर निर्वाण के लगभग १००० वर्ष बाद।
कल्पसूत्र का तीसरा भाग समाचारी है जिसमें 'णाणस्स सारं आयारो' के आधार पर आचार का वर्णन किया गया है। समाचारी का अर्थ है सम्यक् आचार का वर्णन करने वाला । इस भाग में साधु वर्ग के निर्दोष आचार की व्याख्या है। इसे ही 'पज्जोसणा कप्प' कहा जाता है जो आयारदसा ( दशाश्रुतस्कन्ध) का ८वाँ अध्ययन है।
1
आचरण ज्ञान के ऊपर है
तीर्थङ्कर महावीर ने कोरे ज्ञान को कतई महत्त्व नहीं दिया। उन्होंने आचरण को विशेष महत्त्व दिया। इसलिए वे ज्ञानवादी नहीं, आचरणवादी कहलाये । जैन आगमों का प्रारम्भ ही आचारांग से होता है जहाँ कहा गया है 'णाणस्स सारो आयारो' । उत्तरकालीन सारे आचार्यों ने इस कथन का पूरी तरह से अनुकरण किया है। कल्पसूत्र के अन्तिम भाग समाचारी में यही तथ्य मुख्य रूप से वर्णित है ।
ज्ञान वस्तुत: किताबी ज्ञान है यदि वह अनुभव में न उतरे। स्वानुभूति बिना ज्ञान के पंगु है, अधूरा है। आस्था और श्रद्धा भी उसी का अनुकरण करती है। इसमें वही अन्तर है जो अन्तर एक भाषण और प्रवचन में होता है। भाषण उधार लिये हुए ज्ञान की अभिव्यक्ति मात्र है पर प्रवचन एक विशिष्ट वचनों का प्रगटीकरण है जो अनुभूति के माध्यम से उतरता है । इसलिए दर्शन, ज्ञान और चारित्र के साथ 'सम्यक्' विशेषण लगा दिया गया है ताकि थोथे ज्ञान और मिथ्या तप की उपेक्षा की जा सके। 'रत्नत्रय' सिद्धान्त के पीछे यही धारणा रही है और तीनों के समन्वित मार्ग को ही सच्ची सफलता का सत्र माना है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org