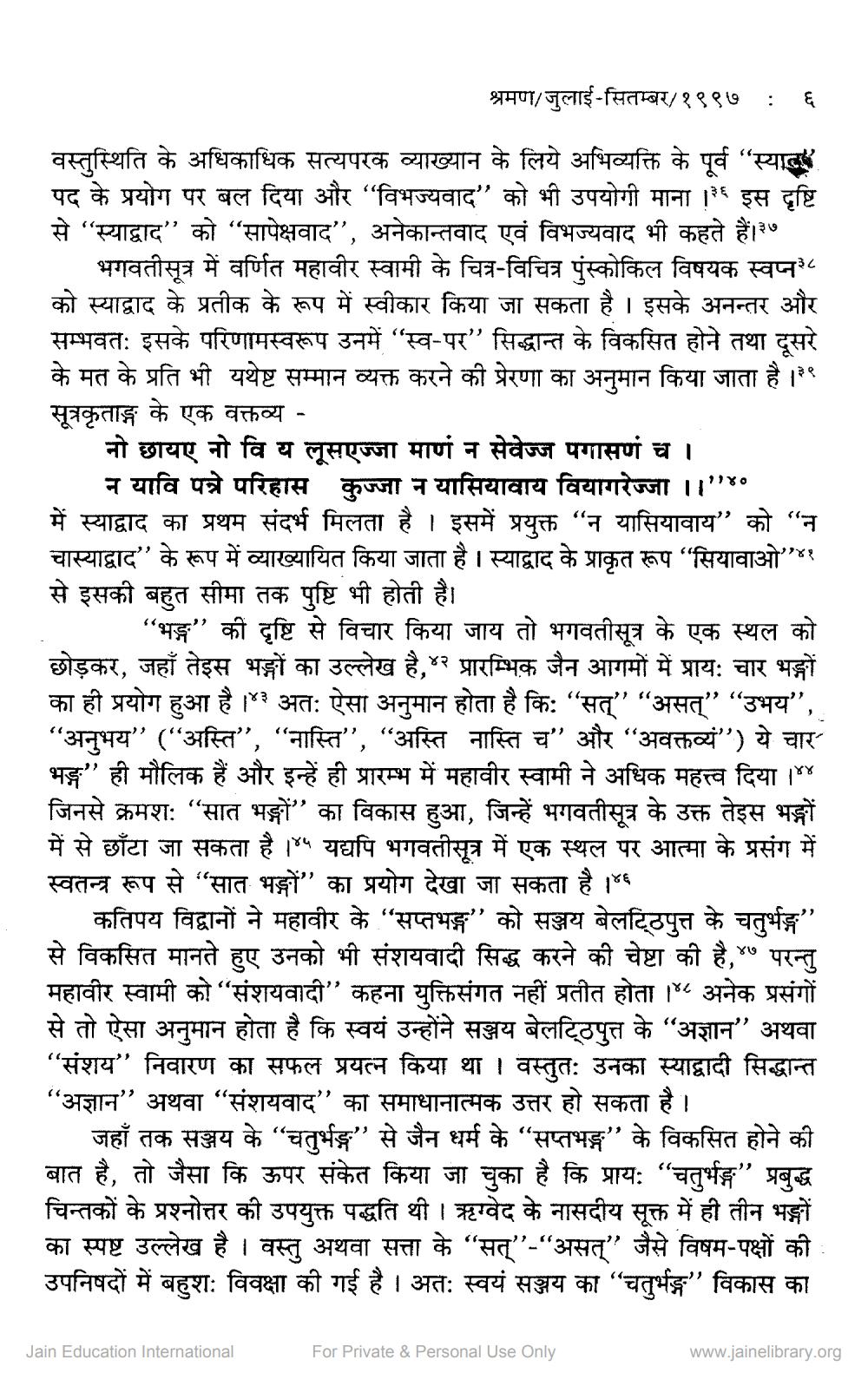________________
श्रमण/जुलाई-सितम्बर/१९९७ : ६
वस्तुस्थिति के अधिकाधिक सत्यपरक व्याख्यान के लिये अभिव्यक्ति के पूर्व "स्यादर पद के प्रयोग पर बल दिया और “विभज्यवाद' को भी उपयोगी माना ।३६ इस दृष्टि से "स्याद्वाद" को "सापेक्षवाद", अनेकान्तवाद एवं विभज्यवाद भी कहते हैं।३७
भगवतीसूत्र में वर्णित महावीर स्वामी के चित्र-विचित्र पुंस्कोकिल विषयक स्वप्न३८ को स्याद्वाद के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया जा सकता है । इसके अनन्तर और सम्भवत: इसके परिणामस्वरूप उनमें "स्व-पर' सिद्धान्त के विकसित होने तथा दूसरे के मत के प्रति भी यथेष्ट सम्मान व्यक्त करने की प्रेरणा का अनुमान किया जाता है ।३९ सूत्रकृताङ्ग के एक वक्तव्य -
नो छायए नो वि य लूसएज्जा माणं न सेवेज्ज पगासणं च ।
न यावि पन्ने परिहास कुज्जा न यासियावाय वियागरेज्जा ।।"४० में स्याद्वाद का प्रथम संदर्भ मिलता है । इसमें प्रयुक्त "न यासियावाय" को "न चास्याद्वाद" के रूप में व्याख्यायित किया जाता है । स्याद्वाद के प्राकृत रूप “सियावाओ"४१ से इसकी बहुत सीमा तक पुष्टि भी होती है।
"भङ्ग' की दृष्टि से विचार किया जाय तो भगवतीसूत्र के एक स्थल को छोड़कर, जहाँ तेइस भङ्गों का उल्लेख है,४२ प्रारम्भिक जैन आगमों में प्राय: चार भङ्गों का ही प्रयोग हुआ है ।४३ अत: ऐसा अनुमान होता है कि: “सत्' "असत्” “उभय", "अनुभय' (“अस्ति", "नास्ति', “अस्ति नास्ति च" और "अवक्तव्यं') ये चार भङ्ग" ही मौलिक हैं और इन्हें ही प्रारम्भ में महावीर स्वामी ने अधिक महत्त्व दिया ।४४ जिनसे क्रमश: “सात भङ्गों' का विकास हुआ, जिन्हें भगवतीसूत्र के उक्त तेइस भङ्गों में से छाँटा जा सकता है।४५ यद्यपि भगवतीसूत्र में एक स्थल पर आत्मा के प्रसंग में स्वतन्त्र रूप से “सात भङ्गों" का प्रयोग देखा जा सकता है ।।६।। । कतिपय विद्वानों ने महावीर के "सप्तभङ्ग'' को सञ्जय बेलट्ठिपुत्त के चतुर्भङ्ग' से विकसित मानते हुए उनको भी संशयवादी सिद्ध करने की चेष्टा की है,४७ परन्तु महावीर स्वामी को "संशयवादी" कहना युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता ।४८ अनेक प्रसंगों से तो ऐसा अनुमान होता है कि स्वयं उन्होंने सञ्जय बेलट्ठिपुत्त के “अज्ञान" अथवा "संशय' निवारण का सफल प्रयत्न किया था । वस्तुत: उनका स्याद्वादी सिद्धान्त "अज्ञान” अथवा “संशयवाद" का समाधानात्मक उत्तर हो सकता है।
जहाँ तक सञ्जय के “चतुर्भङ्ग' से जैन धर्म के “सप्तभङ्ग" के विकसित होने की बात है, तो जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है कि प्राय: "चतुर्भङ्ग" प्रबुद्ध चिन्तकों के प्रश्नोत्तर की उपयुक्त पद्धति थी । ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में ही तीन भङ्गों का स्पष्ट उल्लेख है । वस्तु अथवा सत्ता के “सत्'-"असत्" जैसे विषम-पक्षों की उपनिषदों में बहुशः विवक्षा की गई है । अत: स्वयं सञ्जय का “चतुर्भङ्ग' विकास का
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org