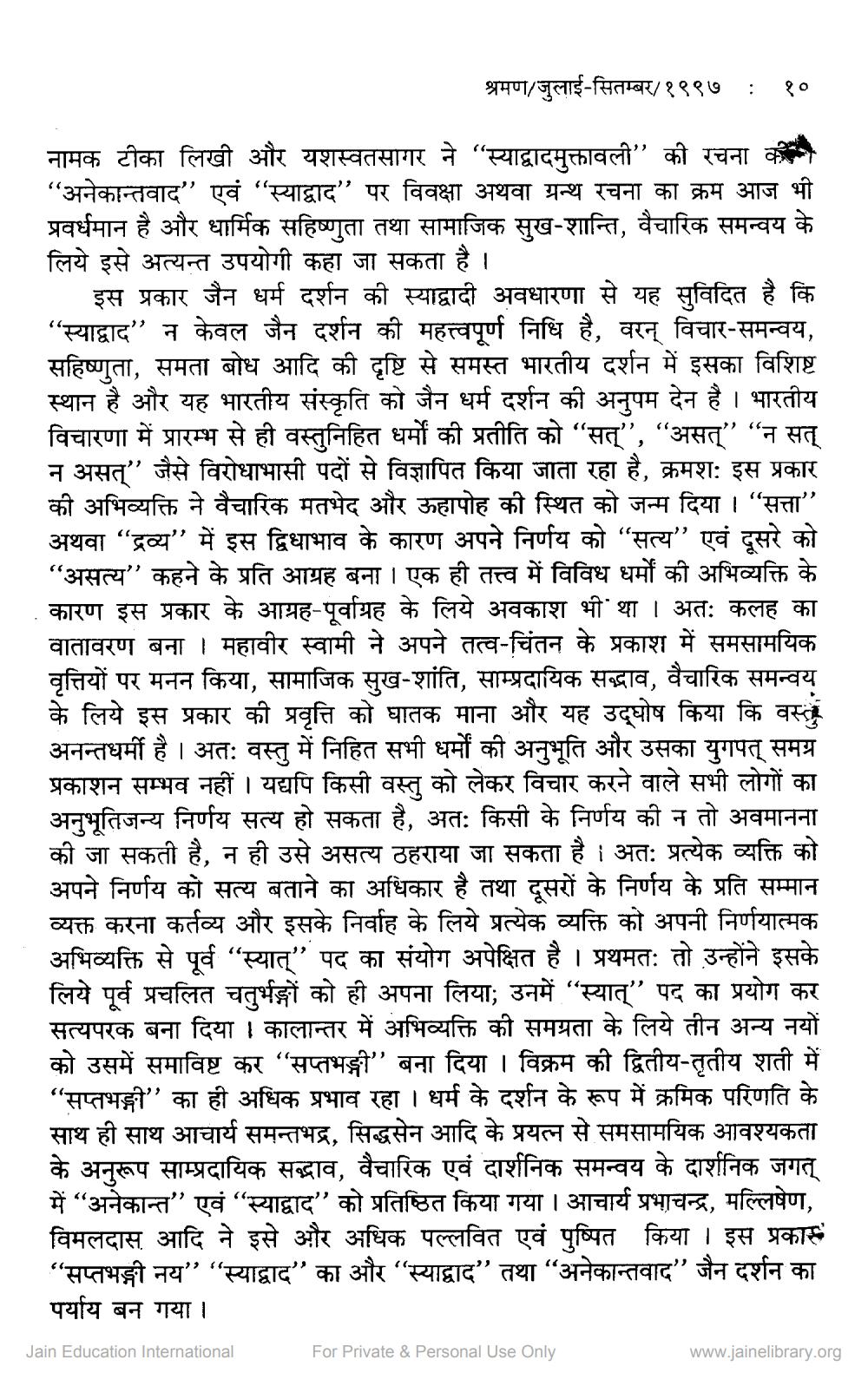________________
श्रमण/जुलाई-सितम्बर/१९९७ : १०
नामक टीका लिखी और यशस्वतसागर ने “स्याद्वादमुक्तावली' की रचना की “अनेकान्तवाद" एवं “स्याद्वाद' पर विवक्षा अथवा ग्रन्थ रचना का क्रम आज भी प्रवर्धमान है और धार्मिक सहिष्णुता तथा सामाजिक सुख-शान्ति, वैचारिक समन्वय के लिये इसे अत्यन्त उपयोगी कहा जा सकता है। __इस प्रकार जैन धर्म दर्शन की स्याद्वादी अवधारणा से यह सुविदित है कि "स्याद्वाद” न केवल जैन दर्शन की महत्त्वपूर्ण निधि है, वरन् विचार-समन्वय, सहिष्णुता, समता बोध आदि की दृष्टि से समस्त भारतीय दर्शन में इसका विशिष्ट स्थान है और यह भारतीय संस्कृति को जैन धर्म दर्शन की अनुपम देन है । भारतीय विचारणा में प्रारम्भ से ही वस्तुनिहित धर्मों की प्रतीति को "सत्", "असत्” “न सत् न असत्" जैसे विरोधाभासी पदों से विज्ञापित किया जाता रहा है, क्रमश: इस प्रकार की अभिव्यक्ति ने वैचारिक मतभेद और ऊहापोह की स्थित को जन्म दिया । “सत्ता" अथवा “द्रव्य" में इस द्विधाभाव के कारण अपने निर्णय को "सत्य" एवं दूसरे को "असत्य' कहने के प्रति आग्रह बना । एक ही तत्त्व में विविध धर्मों की अभिव्यक्ति के कारण इस प्रकार के आग्रह-पूर्वाग्रह के लिये अवकाश भी था । अतः कलह का वातावरण बना । महावीर स्वामी ने अपने तत्व-चिंतन के प्रकाश में समसामयिक वृत्तियों पर मनन किया, सामाजिक सुख-शांति, साम्प्रदायिक सद्भाव, वैचारिक समन्वय के लिये इस प्रकार की प्रवृत्ति को घातक माना और यह उद्घोष किया कि वस्त अनन्तधर्मी है । अत: वस्तु में निहित सभी धर्मों की अनुभूति और उसका युगपत् समग्र प्रकाशन सम्भव नहीं । यद्यपि किसी वस्तु को लेकर विचार करने वाले सभी लोगों का अनुभूतिजन्य निर्णय सत्य हो सकता है, अत: किसी के निर्णय की न तो अवमानना की जा सकती है, न ही उसे असत्य ठहराया जा सकता है । अत: प्रत्येक व्यक्ति को अपने निर्णय को सत्य बताने का अधिकार है तथा दूसरों के निर्णय के प्रति सम्मान व्यक्त करना कर्तव्य और इसके निर्वाह के लिये प्रत्येक व्यक्ति को अपनी निर्णयात्मक
अभिव्यक्ति से पूर्व “स्यात्" पद का संयोग अपेक्षित है । प्रथमत: तो उन्होंने इसके लिये पूर्व प्रचलित चतुर्भङ्गों को ही अपना लिया; उनमें "स्यात्" पद का प्रयोग कर सत्यपरक बना दिया । कालान्तर में अभिव्यक्ति की समग्रता के लिये तीन अन्य नयों को उसमें समाविष्ट कर “सप्तभङ्गी' बना दिया । विक्रम की द्वितीय-तृतीय शती में "सप्तभङ्गी' का ही अधिक प्रभाव रहा । धर्म के दर्शन के रूप में क्रमिक परिणति के साथ ही साथ आचार्य समन्तभद्र, सिद्धसेन आदि के प्रयत्न से समसामयिक आवश्यकता के अनुरूप साम्प्रदायिक सद्भाव, वैचारिक एवं दार्शनिक समन्वय के दार्शनिक जगत् में “अनेकान्त' एवं "स्याद्वाद' को प्रतिष्ठित किया गया । आचार्य प्रभाचन्द्र, मल्लिषेण, विमलदास आदि ने इसे और अधिक पल्लवित एवं पुष्पित किया । इस प्रकार “सप्तभङ्गी नय” “स्याद्वाद" का और “स्याद्वाद” तथा “अनेकान्तवाद” जैन दर्शन का पर्याय बन गया।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org