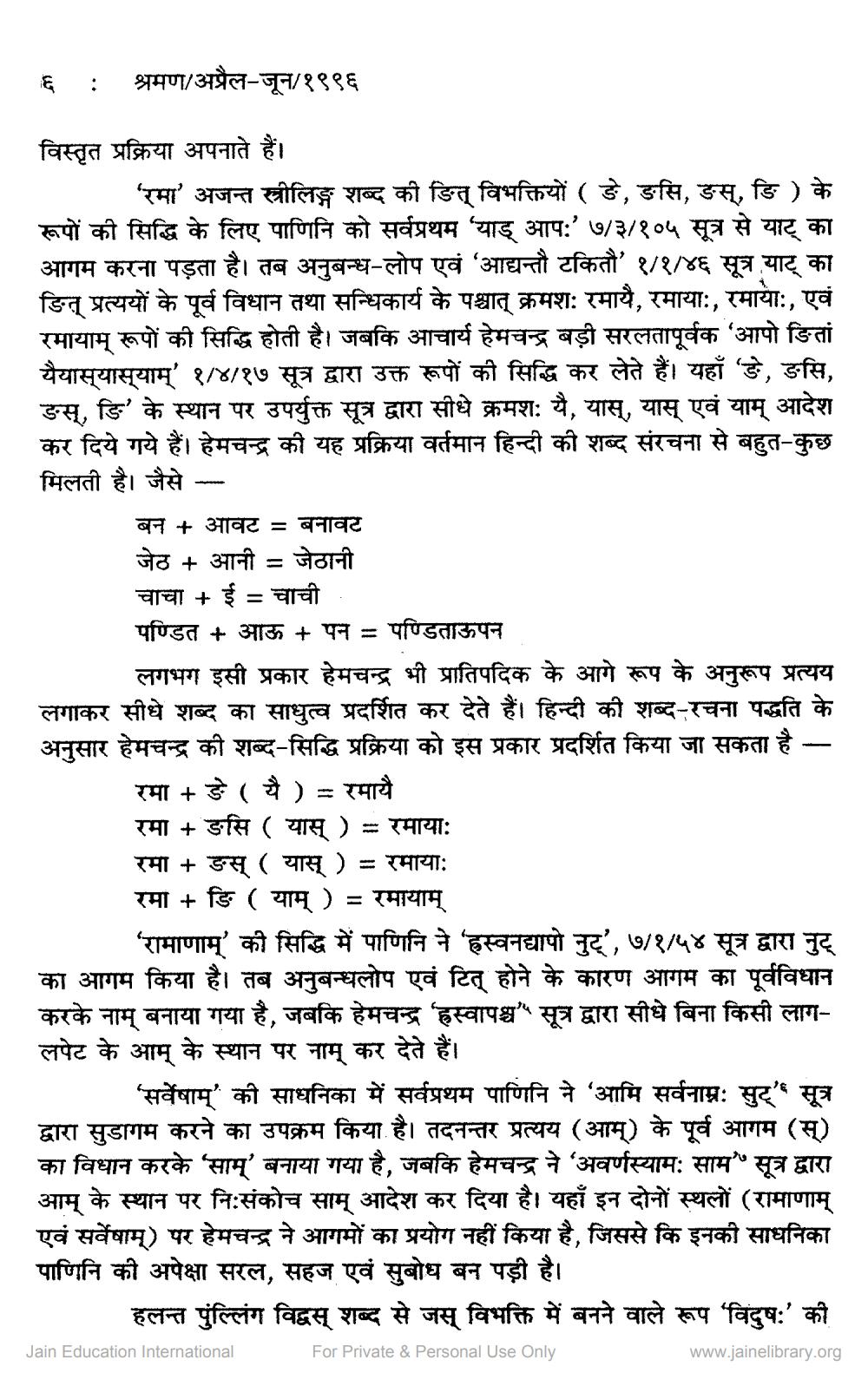________________
६
:
श्रमण/अप्रैल-जून/१९९६
विस्तृत प्रक्रिया अपनाते हैं।
_ 'रमा' अजन्त स्त्रीलिङ्ग शब्द की ङित् विभक्तियों ( 3, ङसि, ङस्, ङि ) के रूपों की सिद्धि के लिए पाणिनि को सर्वप्रथम 'याड् आपः' ७/३/१०५ सूत्र से याट का आगम करना पड़ता है। तब अनुबन्ध-लोप एवं 'आद्यन्तौ टकितौ' १/१/४६ सूत्र याट् का ङित् प्रत्ययों के पूर्व विधान तथा सन्धिकार्य के पश्चात् क्रमशः रमायै, रमायाः, रमायाः, एवं रमायाम् रूपों की सिद्धि होती है। जबकि आचार्य हेमचन्द्र बड़ी सरलतापूर्वक 'आपो ङितां यैयास्यास्याम्' १/४/१७ सूत्र द्वारा उक्त रूपों की सिद्धि कर लेते हैं। यहाँ 'डे, ङसि, ङस, ङि' के स्थान पर उपर्युक्त सूत्र द्वारा सीधे क्रमश: यै, यास्, यास् एवं याम् आदेश कर दिये गये हैं। हेमचन्द्र की यह प्रक्रिया वर्तमान हिन्दी की शब्द संरचना से बहुत-कुछ मिलती है। जैसे -
बन + आवट = बनावट जेठ + आनी = जेठानी चाचा + ई = चाची पण्डित + आऊ + पन = पण्डिताऊपन
लगभग इसी प्रकार हेमचन्द्र भी प्रातिपदिक के आगे रूप के अनुरूप प्रत्यय लगाकर सीधे शब्द का साधुत्व प्रदर्शित कर देते हैं। हिन्दी की शब्द-रचना पद्धति के अनुसार हेमचन्द्र की शब्द-सिद्धि प्रक्रिया को इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है -
रमा + 3 ( 2 ) = रमायै रमा + ङसि ( यास् ) = रमाया: रमा + ङस् ( यास् ) = रमायाः रमा + ङि ( याम् ) = रमायाम्
'रामाणाम' की सिद्धि में पाणिनि ने 'हस्वनद्यापो नुट्', ७/१/५४ सूत्र द्वारा नुट् का आगम किया है। तब अनुबन्धलोप एवं टित् होने के कारण आगम का पूर्वविधान करके नाम् बनाया गया है, जबकि हेमचन्द्र ह्रस्वापश्च५ सूत्र द्वारा सीधे बिना किसी लागलपेट के आम् के स्थान पर नाम् कर देते हैं।
__"सर्वेषाम्" की साधनिका में सर्वप्रथम पाणिनि ने 'आमि सर्वनाम्नः सुट्६ सूत्र द्वारा सुडागम करने का उपक्रम किया है। तदनन्तर प्रत्यय (आम्) के पूर्व आगम (स्) का विधान करके 'साम्' बनाया गया है, जबकि हेमचन्द्र ने 'अवर्णस्याम: साम" सूत्र द्वारा आम् के स्थान पर निःसंकोच साम् आदेश कर दिया है। यहाँ इन दोनों स्थलों (रामाणाम् एवं सर्वेषाम्) पर हेमचन्द्र ने आगमों का प्रयोग नहीं किया है, जिससे कि इनकी साधनिका पाणिनि की अपेक्षा सरल, सहज एवं सुबोध बन पड़ी है।
हलन्त पुंल्लिंग विद्वस् शब्द से जस् विभक्ति में बनने वाले रूप 'विदुषः' की Jain Education International For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org