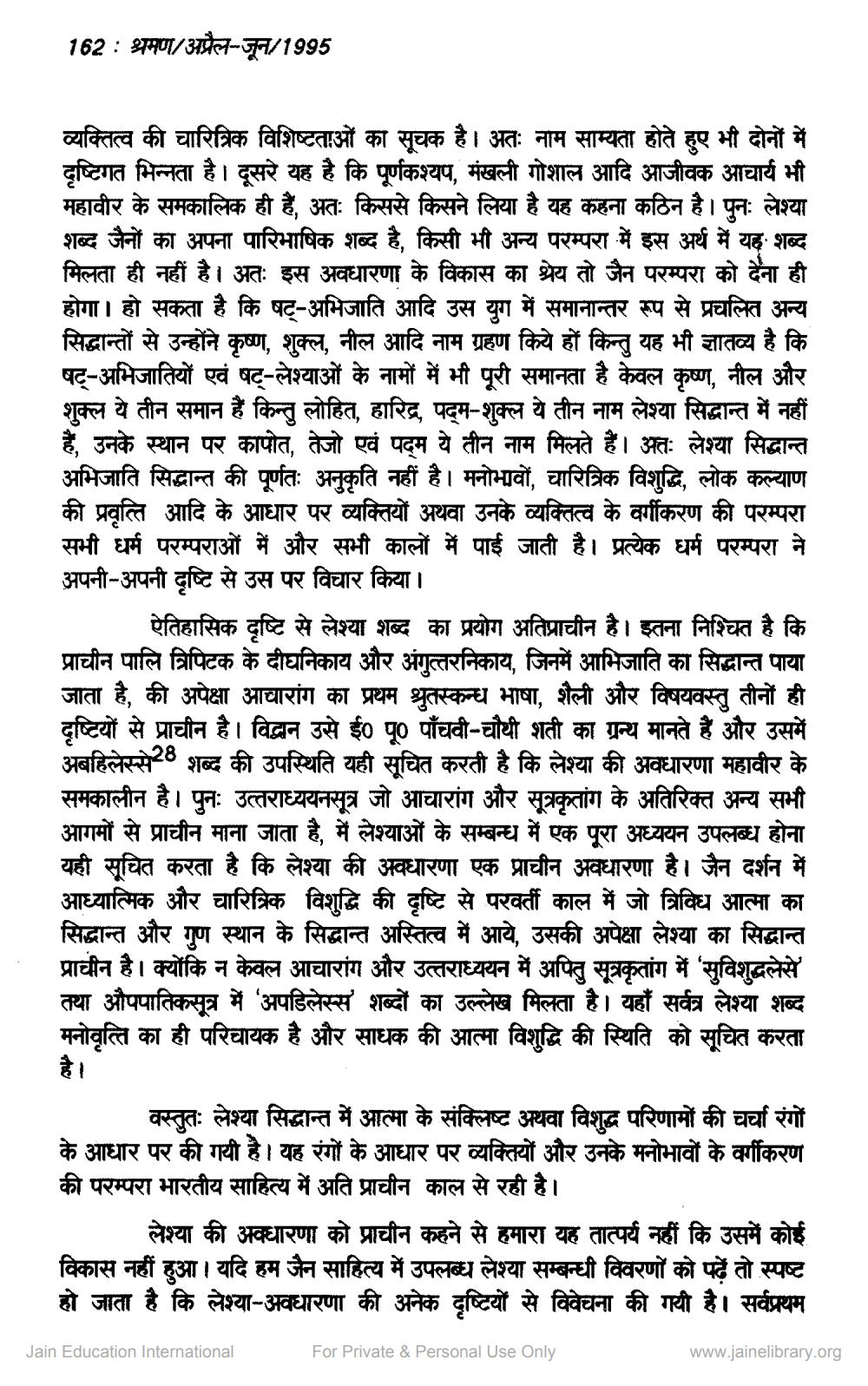________________
162: श्रमण / अप्रैल-जून/ 1995
व्यक्तित्व की चारित्रिक विशिष्टताओं का सूचक है। अतः नाम साम्यता होते हुए भी दोनों में दृष्टिगत भिन्नता है। दूसरे यह है कि पूर्णकश्यप, मंखली गोशाल आदि आजीवक आचार्य भी महावीर के समकालिक ही हैं, अतः किससे किसने लिया है यह कहना कठिन है । पुनः लेश्या शब्द जैनों का अपना पारिभाषिक शब्द है, किसी भी अन्य परम्परा में इस अर्थ में यह शब्द मिलता ही नहीं है । अतः इस अवधारणा के विकास का श्रेय तो जैन परम्परा को देना ही होगा। हो सकता है कि षट्-अभिजाति आदि उस युग में समानान्तर रूप से प्रचलित अन्य सिद्धान्तों से उन्होंने कृष्ण, शुक्ल, नील आदि नाम ग्रहण किये हों किन्तु यह भी ज्ञातव्य है कि षट्-अभिजातियों एवं षट् - लेश्याओं के नामों में भी पूरी समानता है केवल कृष्ण, नील और शुक्ल ये तीन समान हैं किन्तु लोहित, हारिद्र, पद्म- शुक्ल ये तीन नाम लेश्या सिद्धान्त में नहीं हैं, उनके स्थान पर कापोत, तेजो एवं पद्म ये तीन नाम मिलते हैं। अतः लेश्या सिद्धान्त अभिजाति सिद्धान्त की पूर्णतः अनुकृति नहीं है। मनोभावों, चारित्रिक विशुद्धि, लोक कल्याण की प्रवृत्ति आदि के आधार पर व्यक्तियों अथवा उनके व्यक्तित्व के वर्गीकरण की परम्परा सभी धर्म परम्पराओं में और सभी कालों में पाई जाती है । प्रत्येक धर्म परम्परा ने अपनी-अपनी दृष्टि से उस पर विचार किया ।
ऐतिहासिक दृष्टि से लेश्या शब्द का प्रयोग अतिप्राचीन है। इतना निश्चित है कि प्राचीन पालि त्रिपिटक के दीघनिकाय और अंगुत्तरनिकाय, जिनमें आभिजाति का सिद्धान्त पाया जाता है, की अपेक्षा आचारांग का प्रथम श्रुतस्कन्ध भाषा, शैली और विषयवस्तु तीनों ही दृष्टियों से प्राचीन है । विद्वान उसे ई० पू० पाँचवी - चौथी शती का ग्रन्थ मानते हैं और उसमें अबहिलेस्से 28 शब्द की उपस्थिति यही सूचित करती है कि लेश्या की अवधारणा महावीर के समकालीन है। पुनः उत्तराध्ययनसूत्र जो आचारांग और सूत्रकृतांग के अतिरिक्त अन्य सभी आगमों से प्राचीन माना जाता है, में लेश्याओं के सम्बन्ध में एक पूरा अध्ययन उपलब्ध होना यही सूचित करता है कि लेश्या की अवधारणा एक प्राचीन अवधारणा है। जैन दर्शन में आध्यात्मिक और चारित्रिक विशुद्धि की दृष्टि से परवर्ती काल में जो त्रिविध आत्मा का सिद्धान्त और गुण स्थान के सिद्धान्त अस्तित्व में आये, उसकी अपेक्षा लेश्या का सिद्धान्त प्राचीन है। क्योंकि न केवल आचारांग और उत्तराध्ययन में अपितु सूत्रकृतांग में 'सुविशुद्धले से' तथा औपपातिकसूत्र में 'अपडिलेस्स' शब्दों का उल्लेख मिलता है। यहाँ सर्वत्र लेश्या शब्द मनोवृत्ति का ही परिचायक है और साधक की आत्मा विशुद्धि की स्थिति को सूचित करता
है ।
वस्तुतः लेश्या सिद्धान्त में आत्मा के संक्लिष्ट अथवा विशुद्ध परिणामों की चर्चा रंगों के आधार पर की गयी है। यह रंगों के आधार पर व्यक्तियों और उनके मनोभावों के वर्गीकरण की परम्परा भारतीय साहित्य में अति प्राचीन काल से रही है।
लेश्या की अवधारणा को प्राचीन कहने से हमारा यह तात्पर्य नहीं कि उसमें कोई विकास नहीं हुआ। यदि हम जैन साहित्य में उपलब्ध लेश्या सम्बन्धी विवरणों को पढ़ें तो स्पष्ट हो जाता है कि लेश्या - अवधारणा की अनेक दृष्टियों से विवेचना की गयी है । सर्वप्रथम
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org
Jain Education International