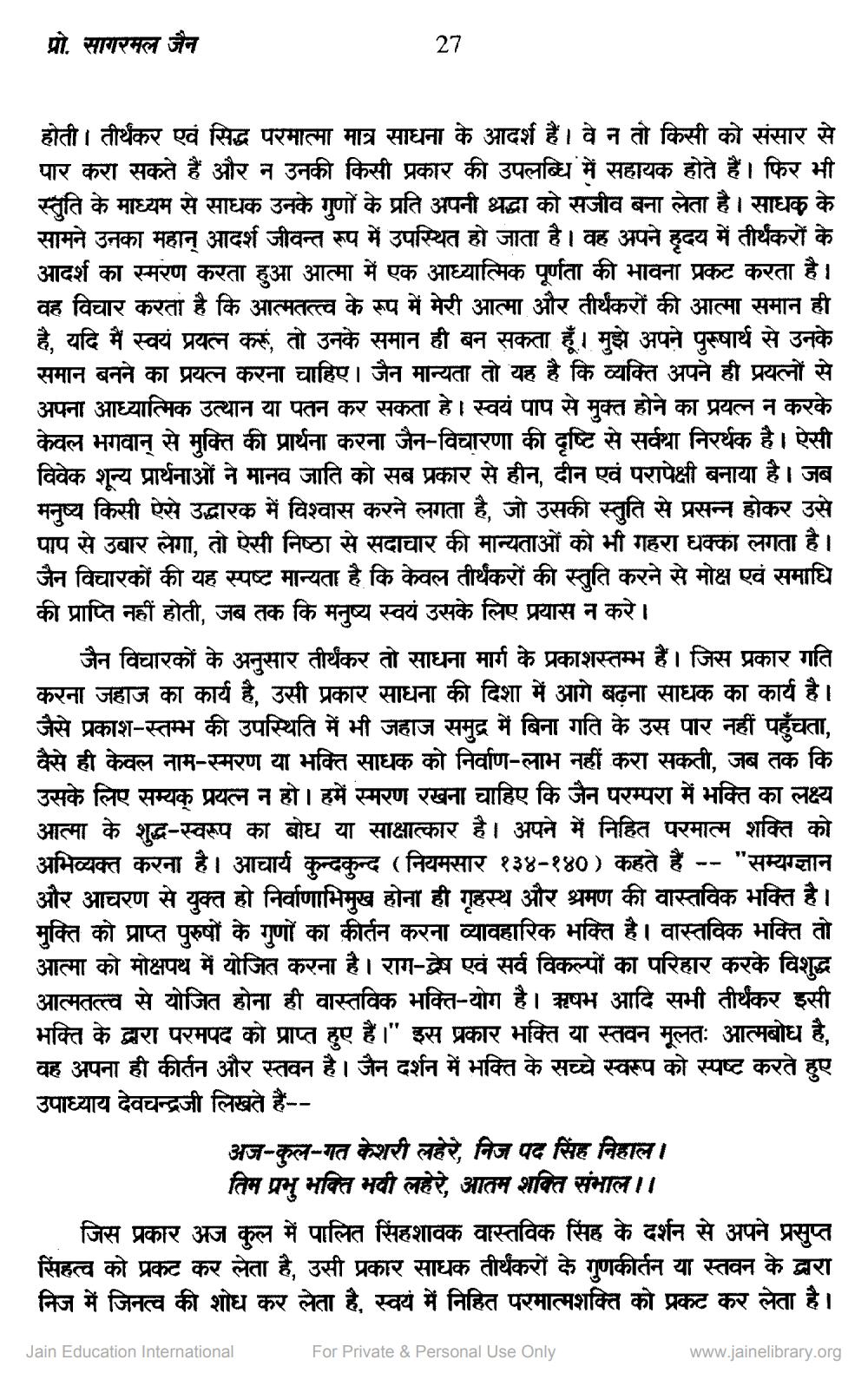________________
प्रो. सागरमल जैन
27
होती। तीर्थंकर एवं सिद्ध परमात्मा मात्र साधना के आदर्श हैं। वे न तो किसी को संसार से पार करा सकते हैं और न उनकी किसी प्रकार की उपलब्धि में सहायक होते हैं। फिर भी स्तुति के माध्यम से साधक उनके गुणों के प्रति अपनी श्रद्धा को सजीव बना लेता है। साधक के सामने उनका महान् आदर्श जीवन्त रूप में उपस्थित हो जाता है। वह अपने हृदय में तीर्थंकरों के आदर्श का स्मरण करता हुआ आत्मा में एक आध्यात्मिक पूर्णता की भावना प्रकट करता है। वह विचार करता है कि आत्मतत्त्व के रूप में मेरी आत्मा और तीर्थंकरों की आत्मा समान ही है, यदि मैं स्वयं प्रयत्न करूं, तो उनके समान ही बन सकता हूँ। मुझे अपने पुरुषार्थ से उनके समान बनने का प्रयत्न करना चाहिए। जैन मान्यता तो यह है कि व्यक्ति अपने ही प्रयत्नों से अपना आध्यात्मिक उत्थान या पतन कर सकता है। स्वयं पाप से मुक्त होने का प्रयत्न न करके केवल भगवान् से मुक्ति की प्रार्थना करना जैन-विचारणा की दृष्टि से सर्वथा निरर्थक है। ऐसी विवेक शून्य प्रार्थनाओं ने मानव जाति को सब प्रकार से हीन, दीन एवं परापेक्षी बनाया है। जब मनुष्य किसी ऐसे उद्धारक में विश्वास करने लगता है, जो उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर उसे पाप से उबार लेगा, तो ऐसी निष्ठा से सदाचार की मान्यताओं को भी गहरा धक्का लगता है। जैन विचारकों की यह स्पष्ट मान्यता है कि केवल तीर्थंकरों की स्तुति करने से मोक्ष एवं समाधि की प्राप्ति नहीं होती, जब तक कि मनुष्य स्वयं उसके लिए प्रयास न करे।
जैन विचारकों के अनुसार तीर्थंकर तो साधना मार्ग के प्रकाशस्तम्भ हैं। जिस प्रकार गति करना जहाज का कार्य है, उसी प्रकार साधना की दिशा में आगे बढ़ना साधक का कार्य है। जैसे प्रकाश-स्तम्भ की उपस्थिति में भी जहाज समुद्र में बिना गति के उस पार नहीं पहुँचता, वैसे ही केवल नाम-स्मरण या भक्ति साधक को निर्वाण-लाभ नहीं करा सकती, जब तक कि उसके लिए सम्यक् प्रयत्न न हो। हमें स्मरण रखना चाहिए कि जैन परम्परा में भक्ति का लक्ष्य आत्मा के शुद्ध-स्वरूप का बोध या साक्षात्कार है। अपने में निहित परमात्म शक्ति को अभिव्यक्त करना है। आचार्य कुन्दकुन्द (नियमसार १३४-१४०) कहते हैं -- "सम्यग्ज्ञान और आचरण से युक्त हो निर्वाणाभिमुख होना ही गृहस्थ और श्रमण की वास्तविक भक्ति है। मुक्ति को प्राप्त पुरुषों के गुणों का कीर्तन करना व्यावहारिक भक्ति है। वास्तविक भक्ति तो आत्मा को मोक्षपथ में योजित करना है। राग-द्वेष एवं सर्व विकल्पों का परिहार करके विशुद्ध आत्मतत्त्व से योजित होना ही वास्तविक भक्ति-योग है। ऋषभ आदि सभी तीर्थंकर इसी भक्ति के द्वारा परमपद को प्राप्त हुए हैं।" इस प्रकार भक्ति या स्तवन मूलतः आत्मबोध है, वह अपना ही कीर्तन और स्तवन है। जैन दर्शन में भक्ति के सच्चे स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उपाध्याय देवचन्द्रजी लिखते हैं--
अज-कुल-गत केशरी लहेरे, निज पद सिंह निहाल।
तिम प्रभु भक्ति भवी लहरे, आतम शक्ति संभाल।। जिस प्रकार अज कुल में पालित सिंहशावक वास्तविक सिंह के दर्शन से अपने प्रसुप्त सिंहत्व को प्रकट कर लेता है, उसी प्रकार साधक तीर्थंकरों के गुणकीर्तन या स्तवन के द्वारा निज में जिनत्व की शोध कर लेता है, स्वयं में निहित परमात्मशक्ति को प्रकट कर लेता है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org