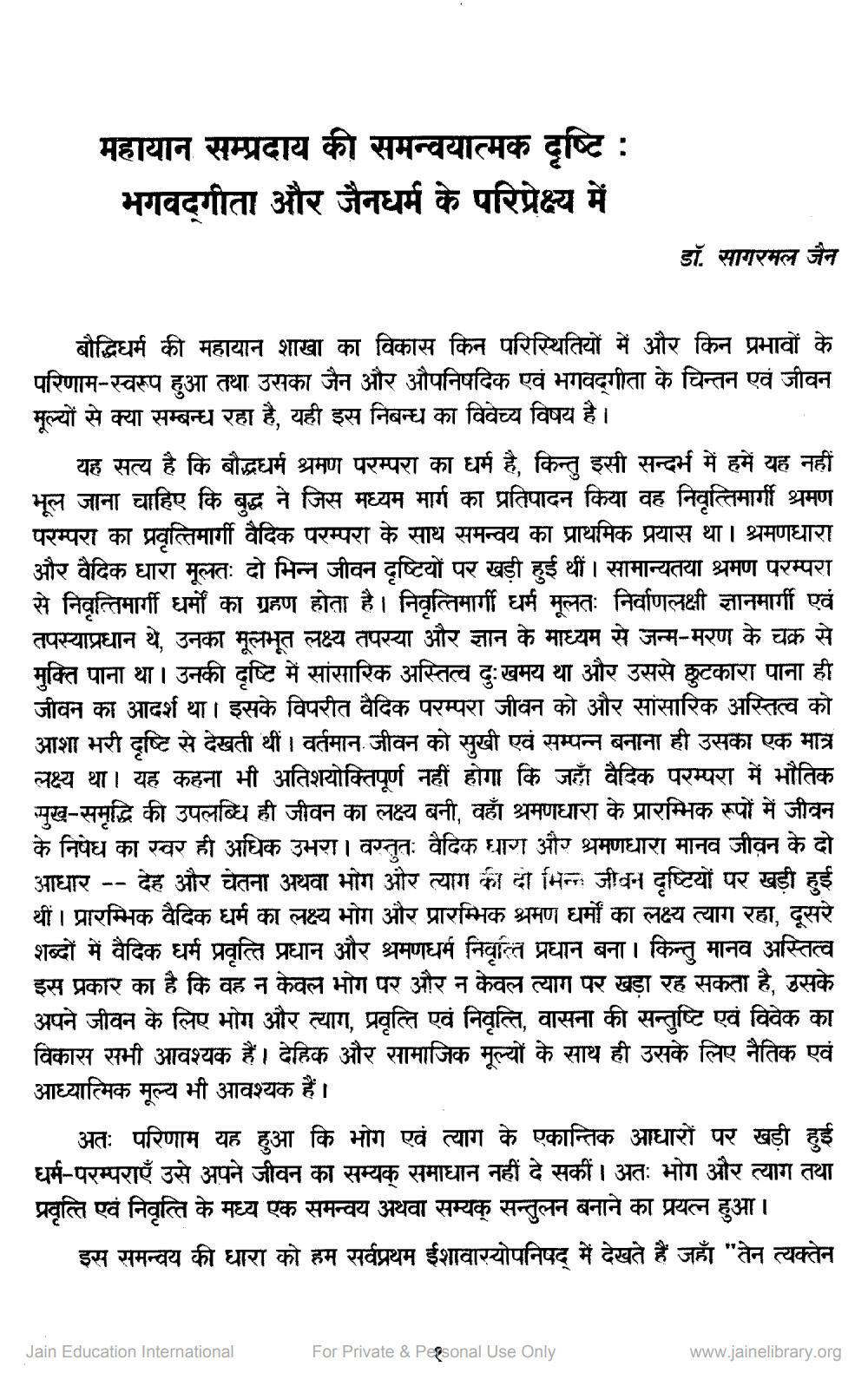________________
महायान सम्प्रदाय की समन्वयात्मक दृष्टि : भगवद्गीता और जैनधर्म के परिप्रेक्ष्य में
डॉ. सागरमल जैन
बौद्धिधर्म की महायान शाखा का विकास किन परिस्थितियों में और किन प्रभावों के परिणाम-स्वरूप हुआ तथा उसका जैन और औपनिषदिक एवं भगवदगीता के चिन्तन एवं जीवन मूल्यों से क्या सम्बन्ध रहा है, यही इस निबन्ध का विवेच्य विषय है।
यह सत्य है कि बौद्धधर्म श्रमण परम्परा का धर्म है, किन्तु इसी सन्दर्भ में हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि बुद्ध ने जिस मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया वह निवृत्तिमार्गी श्रमण परम्परा का प्रवृत्तिमार्गी वैदिक परम्परा के साथ समन्वय का प्राथमिक प्रयास था। श्रमणधारा और वैदिक धारा मूलतः दो भिन्न जीवन दृष्टियों पर खड़ी हुई थीं। सामान्यतया श्रमण परम्परा से निवृत्तिमार्गी धर्मों का ग्रहण होता है। निवृत्तिमार्गी धर्म मूलतः निर्वाणलक्षी ज्ञानमार्गी एवं तपस्याप्रधान थे, उनका मूलभूत लक्ष्य तपस्या और ज्ञान के माध्यम से जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति पाना था। उनकी दृष्टि में सांसारिक अस्तित्व दुःखमय था और उससे छुटकारा पाना ही जीवन का आदर्श था। इसके विपरीत वैदिक परम्परा जीवन को और सांसारिक अस्तित्व को आशा भरी दृष्टि से देखती थीं। वर्तमान जीवन को सुखी एवं सम्पन्न बनाना ही उसका एक मात्र लक्ष्य था। यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि जहाँ वैदिक परम्परा में भौतिक सुख-समृद्धि की उपलब्धि ही जीवन का लक्ष्य बनी, वहाँ श्रमणधारा के प्रारम्भिक रूपों में जीवन के निषेध का स्वर ही अधिक उभरा। वस्तुतः वैदिक धाग और श्रमणधारा मानव जीवन के दो आधार -- देह और चेतना अथवा भोग और त्याग की दो भिन्तः जीवन दृष्टियों पर खड़ी हुई थीं। प्रारम्भिक वैदिक धर्म का लक्ष्य भोग और प्रारम्भिक श्रमण धर्मों का लक्ष्य त्याग रहा, दूसरे शब्दों में वैदिक धर्म प्रवृत्ति प्रधान और श्रमणधर्म निवात्त प्रधान बना। किन्तु मानव अस्तित्व इस प्रकार का है कि वह न केवल भोग पर और न केवल त्याग पर खड़ा रह सकता है, उसके अपने जीवन के लिए भोग और त्याग, प्रवृत्ति एवं निवृत्ति, वासना की सन्तुष्टि एवं विवेक का विकास सभी आवश्यक हैं। देहिक और सामाजिक मूल्यों के साथ ही उसके लिए नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्य भी आवश्यक हैं।
अतः परिणाम यह हुआ कि भोग एवं त्याग के एकान्तिक आधारों पर खड़ी हुई धर्म-परम्पराएँ उसे अपने जीवन का सम्यक समाधान नहीं दे सकीं। अतः भोग और त्याग तथा प्रवृत्ति एवं निवृत्ति के मध्य एक समन्वय अथवा सम्यक् सन्तुलन बनाने का प्रयत्न हुआ।
इस समन्वय की धारा को हम सर्वप्रथम ईशावास्योपनिषद् में देखते हैं जहाँ "तेन त्यक्तेन
Jain Education International
For Private & Pepsonal Use Only
www.jainelibrary.org