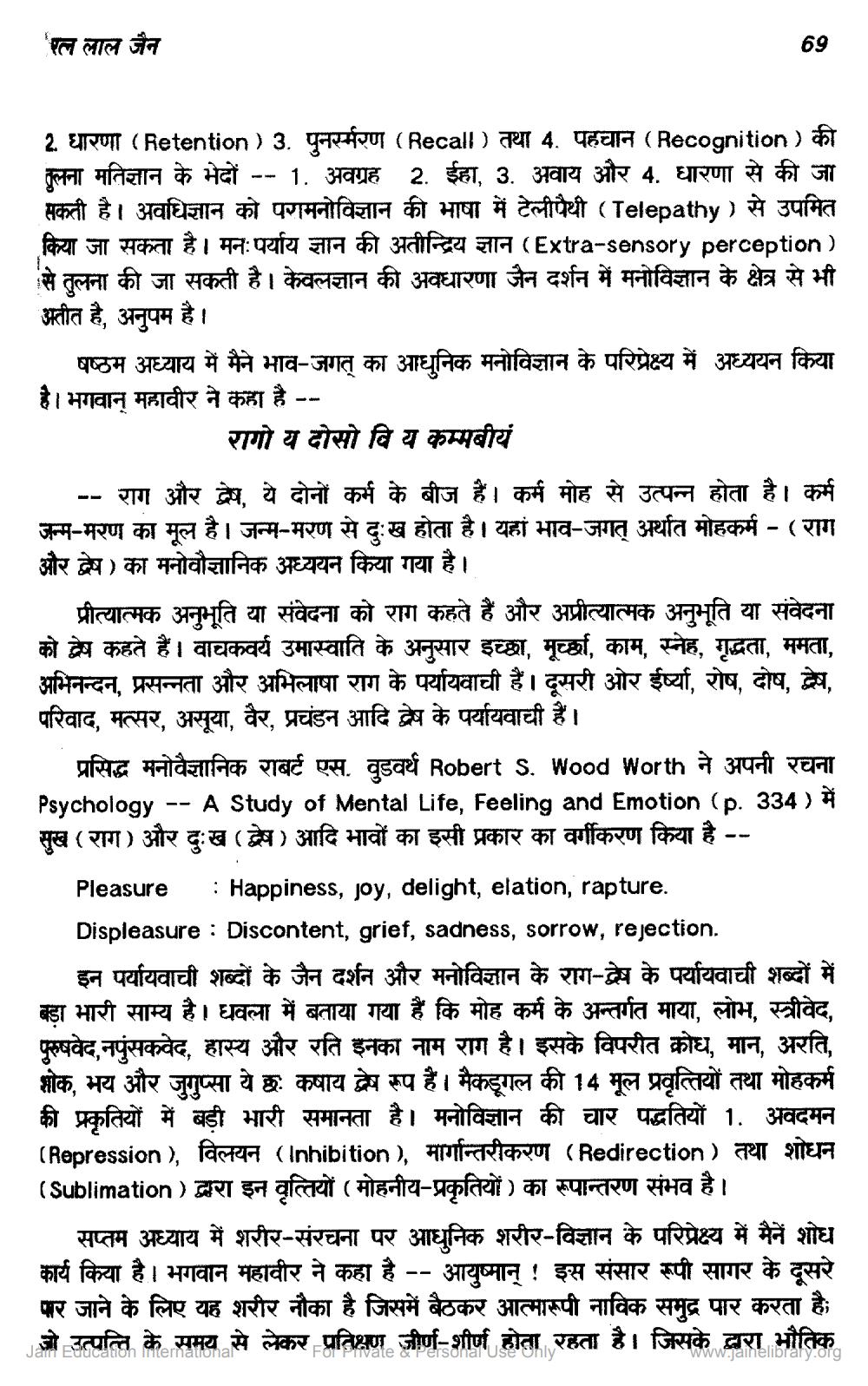________________
रत्न लाल जैन
2. धारणा (Retention ) 3. पुनर्मरण (Recall) तथा 4 पहचान (Recognition) की तुलना मतिज्ञान के भेदों 1. अवग्रह 2. ईहा 3. अवाय और 4. धारणा से की जा सकती है। अवधिज्ञान को परामनोविज्ञान की भाषा में टेलीपैथी (Telepathy ) से उपमित किया जा सकता है। मनः पर्याय ज्ञान की अतीन्द्रिय ज्ञान (Extra-sensory perception ) से तुलना की जा सकती है। केवलज्ञान की अवधारणा जैन दर्शन में मनोविज्ञान के क्षेत्र से भी अतीत है, अनुपम है।
षष्ठम अध्याय में मैने भाव - जगत् का आधुनिक मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया है। भगवान् महावीर ने कहा है
रागो य दोसो व य कम्मबीयं
69
--
राग और द्वेष, ये दोनों कर्म के बीज हैं। कर्म मोह से उत्पन्न होता है । कर्म जन्म-मरण का मूल है। जन्म-मरण से दुःख होता है। यहां भाव-जगत् अर्थात मोहकर्म - (राग और द्वेष ) का मनोवौज्ञानिक अध्ययन किया गया है।
प्रीत्यात्मक अनुभूति या संवेदना को राग कहते हैं और अप्रीत्यात्मक अनुभूति या संवेदना को द्वेष कहते हैं। वाचकवर्य उमास्वाति के अनुसार इच्छा, मूर्च्छा, काम, स्नेह, गृद्धता, ममता, अभिनन्दन, प्रसन्नता और अभिलाषा राग के पर्यायवाची हैं। दूसरी ओर ईर्ष्या, रोष, दोष, द्वेष, परिवाद, मत्सर, असूया, वैर, प्रचंडन आदि द्वेष के पर्यायवाची हैं।
--
प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक राबर्ट एस. वुडवर्थ Robert s. wood worth ने अपनी रचना Psychology A Study of Mental Life, Feeling and Emotion (p. 334 ) में सुख (राग) और दुःख (द्वेष) आदि भावों का इसी प्रकार का वर्गीकरण किया है।
--
Pleasure : Happiness, joy, delight, elation, rapture. Displeasure : Discontent, grief, sadness, sorrow, rejection.
इन पर्यायवाची शब्दों के जैन दर्शन और मनोविज्ञान के राग-द्वेष के पर्यायवाची शब्दों में बड़ा भारी साम्य है | धवला में बताया गया हैं कि मोह कर्म के अन्तर्गत माया, लोभ, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, हास्य और रति इनका नाम राग है। इसके विपरीत क्रोध, मान, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा ये छः कषाय द्वेष रूप हैं। मैक्डूगल की 14 मूल प्रवृत्तियों तथा मोहकर्म की प्रकृतियों में बड़ी भारी समानता है। मनोविज्ञान की चार पद्धतियों 1. अवदमन (Repression ), विलयन (Inhibition ), मार्गान्तरीकरण (Redirection) तथा शोधन (Sublimation) द्वारा इन वृत्तियों (मोहनीय - प्रकृतियों) का रूपान्तरण संभव है।
सप्तम अध्याय में शरीर - संरचना पर आधुनिक शरीर-विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में मैनें शोध कार्य किया है। भगवान महावीर ने कहा है आयुष्मान् ! इस संसार रूपी सागर के दूसरे पार जाने के लिए यह शरीर नौका है जिसमें बैठकर आत्मारूपी नाविक समुद्र पार करता है; जो उत्पत्ति के समय से लेकर प्रतिक्षण जीर्ण-शीर्ण होता रहता है। जिसके द्वारा भौतिक
——