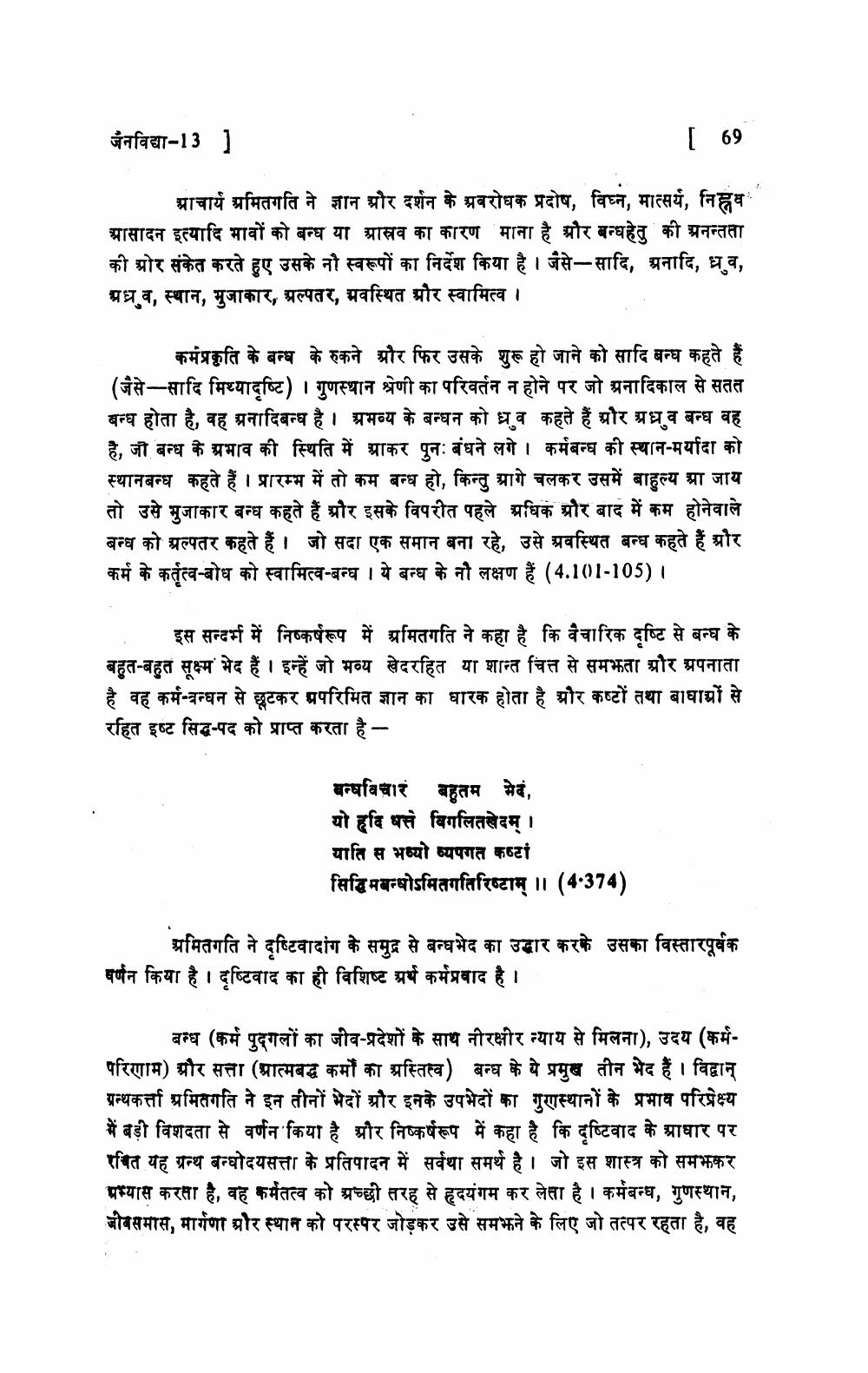________________
जनविद्या-13 ]
[ 69
आचार्य अमितगति ने ज्ञान और दर्शन के अवरोधक प्रदोष, विघ्न, मात्सर्य, निरव पासादन इत्यादि भावों को बन्ध या आस्रव का कारण माना है और बन्धहेतु की अनन्तता की ओर संकेत करते हुए उसके नौ स्वरूपों का निर्देश किया है । जैसे-सादि, अनादि, ध्रुव, अध्र व, स्थान, मुजाकार, अल्पतर, मवस्थित और स्वामित्व ।
कर्मप्रकृति के बन्ध के रुकने और फिर उसके शुरू हो जाने को सादि बन्ध कहते हैं (जैसे-सादि मिथ्यादृष्टि) । गुणस्थान श्रेणी का परिवर्तन न होने पर जो अनादिकाल से सतत बन्ध होता है, वह अनादिबन्ध है। अभव्य के बन्धन को ध्रुव कहते हैं और अध्र व बन्ध वह है, जो बन्ध के अभाव की स्थिति में आकर पुनः बंधने लगे। कर्मबन्ध की स्थान-मर्यादा को स्थानबन्ध कहते हैं । प्रारम्भ में तो कम बन्ध हो, किन्तु आगे चलकर उसमें बाहुल्य आ जाय तो उसे भुजाकार बन्ध कहते हैं और इसके विपरीत पहले अधिक और बाद में कम होनेवाले बन्ध को अल्पतर कहते हैं। जो सदा एक समान बना रहे, उसे अवस्थित बन्ध कहते हैं और कर्म के कर्तृत्व-बोध को स्वामित्व-बन्ध । ये बन्ध के नौ लक्षण हैं (4.101-105)।
इस सन्दर्भ में निष्कर्षरूप में अमितगति ने कहा है कि वैचारिक दृष्टि से बन्ध के बहुत-बहुत सूक्ष्म भेद हैं । इन्हें जो भव्य खेदरहित या शान्त चित्त से समझता और अपनाता है वह कर्म-बन्धन से छूटकर अपरिमित ज्ञान का धारक होता है और कष्टों तथा बाधामों से रहित इष्ट सिद्ध-पद को प्राप्त करता है -
बन्धविचारं बहुतम मेद, यो हृदि धत्ते विगलितखेदम् । याति स भव्यो व्यपगत कष्टां सिद्धिमबन्धोऽमितगतिरिष्टाम् ।। (4:374)
अमितगति ने दृष्टिवादांग के समुद्र से बन्धभेद का उद्धार करके उसका विस्तारपूर्वक वर्णन किया है । दृष्टिवाद का ही विशिष्ट अर्थ कर्मप्रवाद है ।
बन्ध (कर्म पुद्गलों का जीव-प्रदेशों के साथ नीरक्षीर न्याय से मिलना), उदय (कर्मपरिणाम) और सत्ता (प्रात्मबद्ध कर्मों का अस्तित्व) बन्ध के ये प्रमुख तीन भेद हैं । विद्वान् ग्रन्थकर्ता अमितगति ने इन तीनों भेदों और इनके उपभेदों का गुणस्थानों के प्रभाव परिप्रेक्ष्य में बड़ी विशदता से वर्णन किया है और निष्कर्षरूप में कहा है कि दृष्टिवाद के आधार पर रचित यह ग्रन्थ बन्धोदयसत्ता के प्रतिपादन में सर्वथा समर्थ है। जो इस शास्त्र को समझकर पभ्यास करता है, वह कर्मतत्व को अच्छी तरह से हृदयंगम कर लेता है । कर्मबन्ध, गुणस्थान, जीवसमास, मार्गणा और स्थान को परस्पर जोड़कर उसे समझने के लिए जो तत्पर रहता है, वह