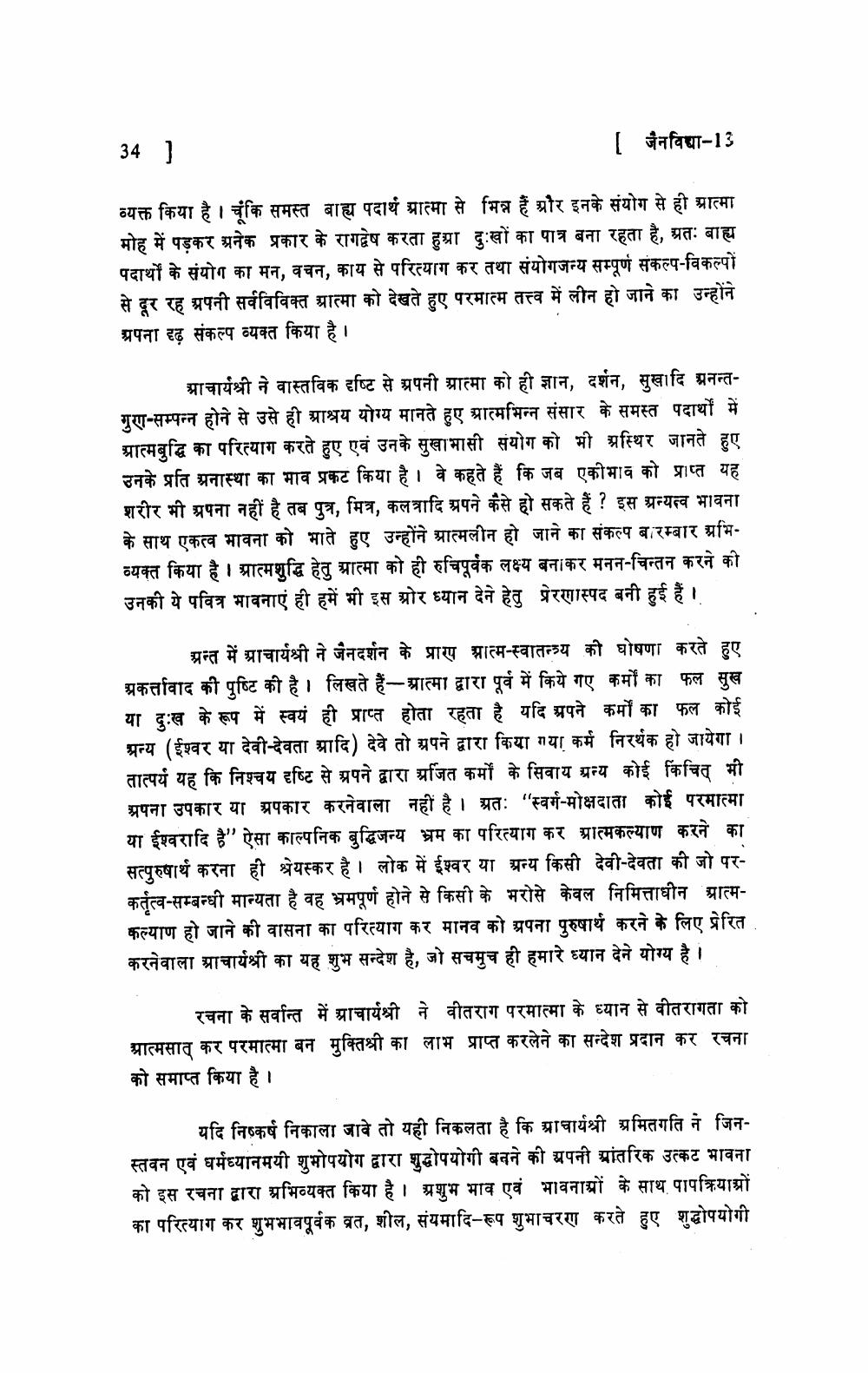________________
34 ]
[ जैनविद्या-13
व्यक्त किया है । चूंकि समस्त बाह्य पदार्थ आत्मा से भिन्न हैं और इनके संयोग से ही प्रात्मा मोह में पड़कर अनेक प्रकार के रागद्वेष करता हुआ दुःखों का पात्र बना रहता है, अतः बाह्य पदार्थों के संयोग का मन, वचन, काय से परित्याग कर तथा संयोगजन्य सम्पूर्ण संकल्प-विकल्पों से दूर रह अपनी सर्वविविक्त आत्मा को देखते हुए परमात्म तत्त्व में लीन हो जाने का उन्होंने अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त किया है।
आचार्यश्री ने वास्तविक दृष्टि से अपनी आत्मा को ही ज्ञान, दर्शन, सुखादि अनन्तगुण-सम्पन्न होने से उसे ही आश्रय योग्य मानते हुए प्रात्मभिन्न संसार के समस्त पदार्थों में प्रात्मबुद्धि का परित्याग करते हुए एवं उनके सुखाभासी संयोग को भी अस्थिर जानते हुए उनके प्रति अनास्था का भाव प्रकट किया है। वे कहते हैं कि जब एकीमाव को प्राप्त यह शरीर भी अपना नहीं है तब पुत्र, मित्र, कलत्रादि अपने कैसे हो सकते हैं ? इस अन्यत्व भावना के साथ एकत्व भावना को भाते हुए उन्होंने आत्मलीन हो जाने का संकल्प बारम्बार अभिव्यक्त किया है । आत्मशुद्धि हेतु आत्मा को ही रुचिपूर्वक लक्ष्य बनाकर मनन-चिन्तन करने की उनकी ये पवित्र भावनाएं ही हमें भी इस ओर ध्यान देने हेतु प्रेरणास्पद बनी हुई हैं।
अन्त में प्राचार्यश्री ने जैनदर्शन के प्राण प्रात्म-स्वातन्त्र्य की घोषणा करते हुए अकर्तावाद की पुष्टि की है। लिखते हैं-आत्मा द्वारा पूर्व में किये गए कर्मों का फल सुख या दुःख के रूप में स्वयं ही प्राप्त होता रहता है यदि अपने कर्मों का फल कोई अन्य (ईश्वर या देवी-देवता आदि) देवे तो अपने द्वारा किया गया कर्म निरर्थक हो जायेगा। तात्पर्य यह कि निश्चय दृष्टि से अपने द्वारा अजित कर्मों के सिवाय अन्य कोई किंचित् भी अपना उपकार या अपकार करनेवाला नहीं है । अतः "स्वर्ग-मोक्षदाता कोई परमात्मा या ईश्वरादि है" ऐसा काल्पनिक बुद्धिजन्य भ्रम का परित्याग कर आत्मकल्याण करने का सत्पुरुषार्थ करना ही श्रेयस्कर है। लोक में ईश्वर या अन्य किसी देवी-देवता की जो परकर्तृत्व-सम्बन्धी मान्यता है वह भ्रमपूर्ण होने से किसी के भरोसे केवल निमित्ताधीन प्रात्मकल्याण हो जाने की वासना का परित्याग कर मानव को अपना पुरुषार्थ करने के लिए प्रेरित करनेवाला आचार्यश्री का यह शुभ सन्देश है, जो सचमुच ही हमारे ध्यान देने योग्य है ।
रचना के सर्वान्त में आचार्यश्री ने वीतराग परमात्मा के ध्यान से वीतरागता को आत्मसात् कर परमात्मा बन मुक्तिश्री का लाभ प्राप्त करलेने का सन्देश प्रदान कर रचना को समाप्त किया है।
यदि निष्कर्ष निकाला जावे तो यही निकलता है कि प्राचार्यश्री अमितगति ने जिनस्तवन एवं धर्मध्यानमयी शुभोपयोग द्वारा शुद्धोपयोगी बनने की अपनी प्रांतरिक उत्कट भावना को इस रचना द्वारा अभिव्यक्त किया है। अशुभ भाव एवं भावनाओं के साथ पापक्रियाओं का परित्याग कर शुभभावपूर्वक व्रत, शील, संयमादि-रूप शुभाचरण करते हुए शुद्धोपयोगी