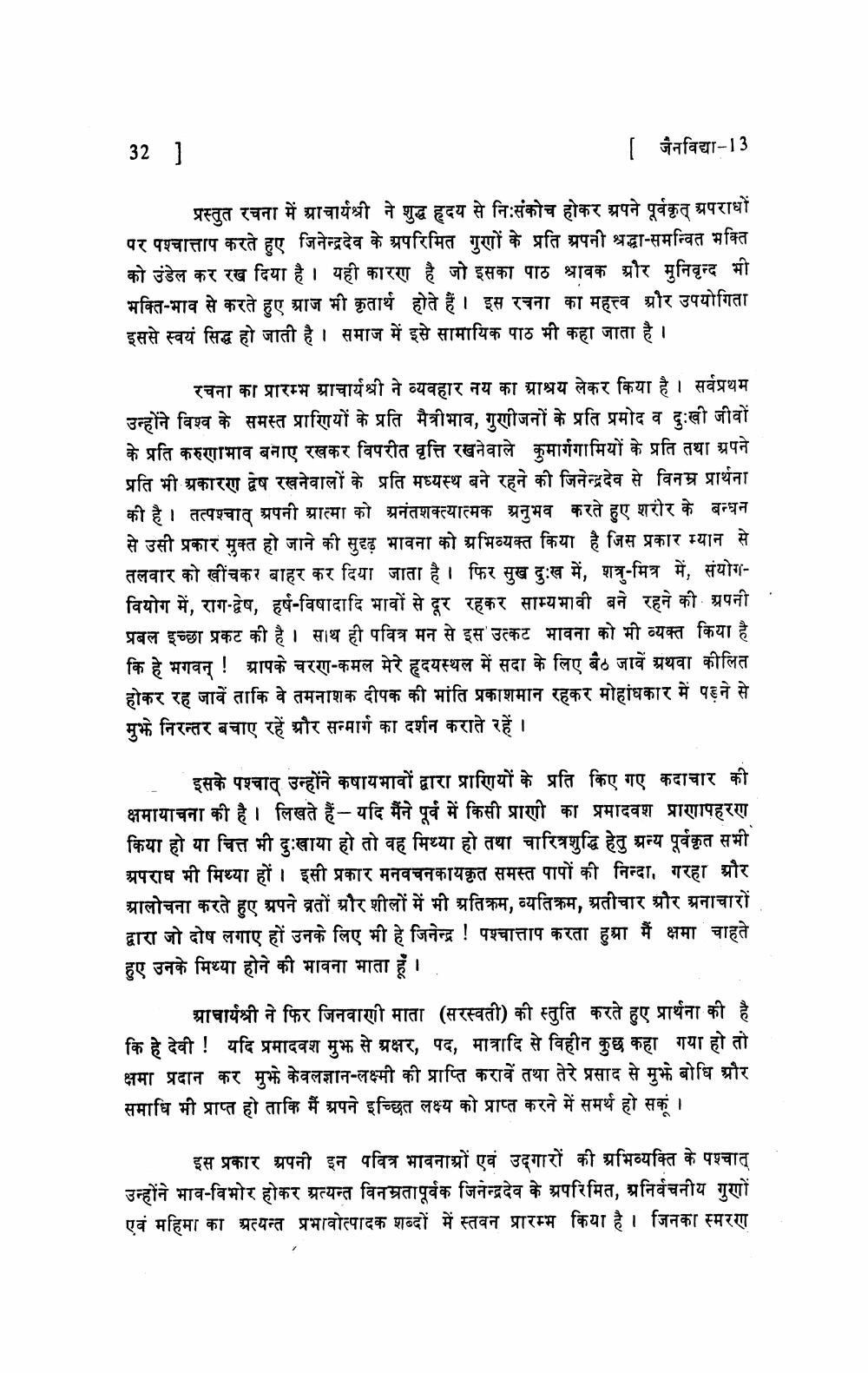________________
32 ]
[ जैनविद्या-13
प्रस्तुत रचना में प्राचार्यश्री ने शुद्ध हृदय से निःसंकोच होकर अपने पूर्वकृत् अपराधों पर पश्चात्ताप करते हुए जिनेन्द्रदेव के अपरिमित गुणों के प्रति अपनी श्रद्धा-समन्वित भक्ति को उंडेल कर रख दिया है। यही कारण है जो इसका पाठ श्रावक और मुनिवृन्द भी भक्ति-भाव से करते हुए आज भी कृतार्थ होते हैं । इस रचना का महत्त्व और उपयोगिता इससे स्वयं सिद्ध हो जाती है। समाज में इसे सामायिक पाठ भी कहा जाता है ।
रचना का प्रारम्भ प्राचार्यश्री ने व्यवहार नय का आश्रय लेकर किया है। सर्वप्रथम उन्होंने विश्व के समस्त प्राणियों के प्रति मैत्रीभाव, गुणीजनों के प्रति प्रमोद व दुःखी जीवों के प्रति करुणाभाव बनाए रखकर विपरीत वृत्ति रखनेवाले कुमार्गगामियों के प्रति तथा अपने प्रति भी अकारण द्वेष रखनेवालों के प्रति मध्यस्थ बने रहने की जिनेन्द्रदेव से विनम्र प्रार्थना की है। तत्पश्चात् अपनी आत्मा को अनंतशक्त्यात्मक अनुभव करते हुए शरीर के बन्धन से उसी प्रकार मुक्त हो जाने की सुदृढ़ भावना को अभिव्यक्त किया है जिस प्रकार म्यान से तलवार को खींचकर बाहर कर दिया जाता है। फिर सुख दुःख में, शत्रु-मित्र में, संयोगवियोग में, राग-द्वेष, हर्ष-विषादादि भावों से दूर रहकर साम्य भावी बने रहने की अपनी प्रबल इच्छा प्रकट की है। साथ ही पवित्र मन से इस' उत्कट भावना को भी व्यक्त किया है कि हे भगवन् ! आपके चरण-कमल मेरे हृदयस्थल में सदा के लिए बैठ जावे अथवा कीलित होकर रह जावें ताकि वे तमनाशक दीपक की भांति प्रकाशमान रहकर मोहांधकार में पड़ने से मुझे निरन्तर बचाए रहें और सन्मार्ग का दर्शन कराते रहें।
- इसके पश्चात् उन्होंने कषायभावों द्वारा प्राणियों के प्रति किए गए कदाचार की क्षमायाचना की है। लिखते हैं- यदि मैंने पूर्व में किसी प्राणी का प्रमादवश प्राणापहरण किया हो या चित्त भी दुःखाया हो तो वह मिथ्या हो तथा चारित्रशुद्धि हेतु अन्य पूर्वकृत सभी अपराध भी मिथ्या हों। इसी प्रकार मनवचनकायकृत समस्त पापों की निन्दा, गरहा और आलोचना करते हुए अपने व्रतों और शीलों में भी अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतीचार और अनाचारों द्वारा जो दोष लगाए हों उनके लिए भी हे जिनेन्द्र ! पश्चात्ताप करता हुआ मैं क्षमा चाहते हुए उनके मिथ्या होने की भावना भाता हूँ।
___ आचार्यश्री ने फिर जिनवाणी माता (सरस्वती) की स्तुति करते हुए प्रार्थना की है कि हे देवी ! यदि प्रमादवश मुझ से अक्षर, पद, मात्रादि से विहीन कुछ कहा गया हो तो क्षमा प्रदान कर मुझे केवलज्ञान-लक्ष्मी की प्राप्ति करावें तथा तेरे प्रसाद से मुझे बोधि और समाधि भी प्राप्त हो ताकि मैं अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ हो सकू।
इस प्रकार अपनी इन पवित्र भावनाओं एवं उद्गारों की अभिव्यक्ति के पश्चात् उन्होंने भाव-विभोर होकर अत्यन्त विनम्रतापूर्वक जिनेन्द्रदेव के अपरिमित, अनिर्वचनीय गुणों एवं महिमा का अत्यन्त प्रभावोत्पादक शब्दों में स्तवन प्रारम्भ किया है। जिनका स्मरण