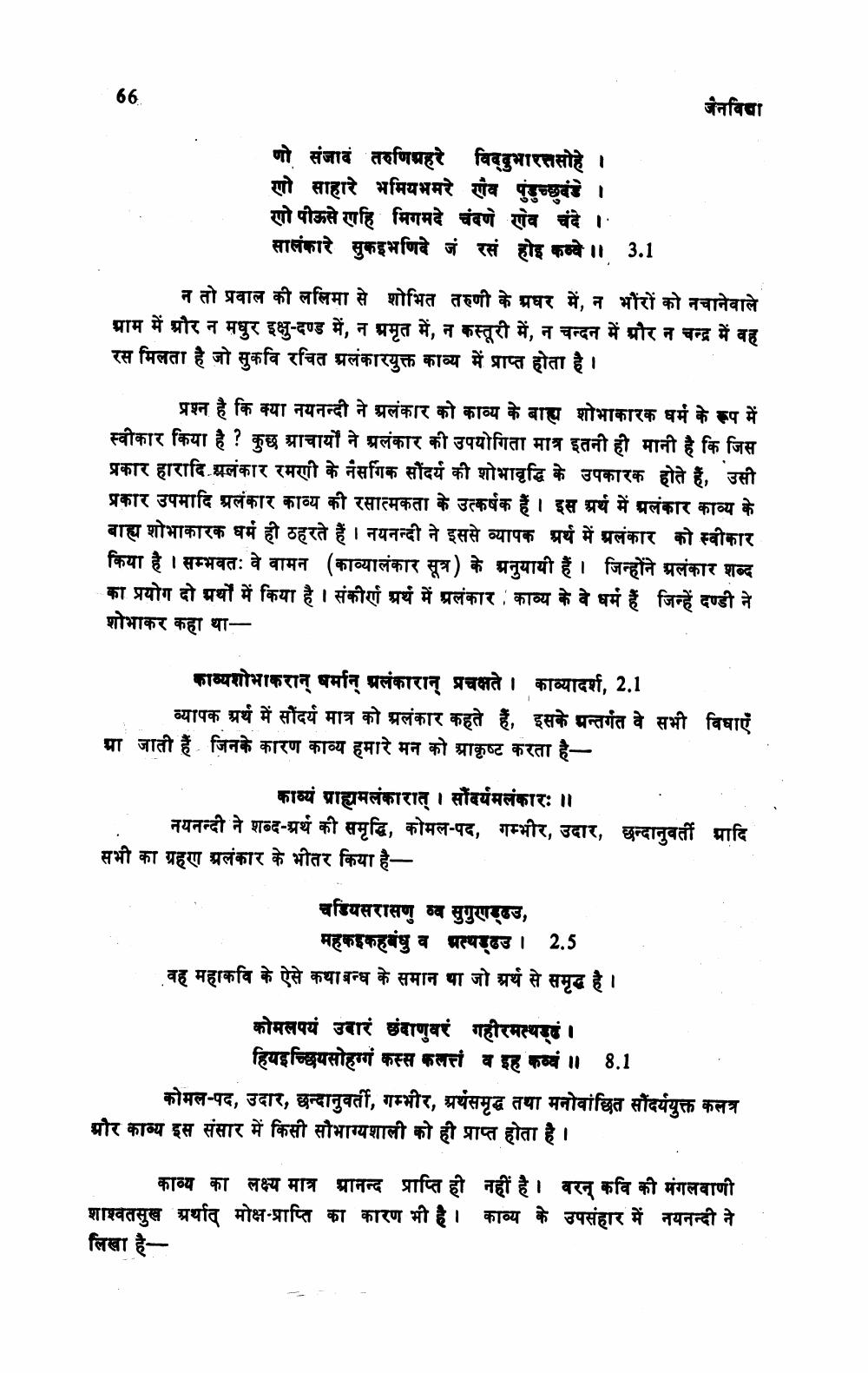________________
66
जैनविधा
णो संजावं तरुणिमहरे विभारतसोहे । णो साहारे भमियभमरे व पुंडच्छुवंरे । पो पीऊसे रणहि मिगमदे चंदणे रणेव चंदे । सालंकारे सुकइभणिदे जं रसं होइ कन्वे ॥ 3.1
न तो प्रवाल की ललिमा से शोभित तरुणी के अधर में, न भौंरों को नचानेवाले प्राम में और न मधुर इक्षु-दण्ड में, न अमृत में, न कस्तूरी में, न चन्दन में और न चन्द्र में वह रस मिलता है जो सुकवि रचित प्रलंकारयुक्त काव्य में प्राप्त होता है ।
प्रश्न है कि क्या नयनन्दी ने अलंकार को काव्य के बाह्य शोभाकारक धर्म के रूप में स्वीकार किया है ? कुछ प्राचार्यों ने अलंकार की उपयोगिता मात्र इतनी ही मानी है कि जिस प्रकार हारादि.अलंकार रमणी के नैसर्गिक सौंदर्य की शोभावृद्धि के उपकारक होते हैं, उसी प्रकार उपमादि अलंकार काव्य की रसात्मकता के उत्कर्षक हैं । इस अर्थ में प्रलंकार काव्य के बाह्य शोभाकारक धर्म ही ठहरते हैं । नयनन्दी ने इससे व्यापक अर्थ में अलंकार को स्वीकार किया है । सम्भवतः वे वामन (काव्यालंकार सूत्र) के अनुयायी हैं। जिन्होंने अलंकार शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया है । संकीर्ण अर्थ में प्रलंकार , काव्य के वे धर्म हैं जिन्हें दण्डी ने शोभाकर कहा था
काव्यशोभाकरान् धर्मान् अलंकारान् प्रचक्षते । काव्यादर्श, 2.1 ___ व्यापक अर्थ में सौंदर्य मात्र को अलंकार कहते हैं, इसके अन्तर्गत वे सभी विधाएँ मा जाती हैं जिनके कारण काव्य हमारे मन को आकृष्ट करता है
काव्यं प्राह्ममलंकारात् । सौंदर्यमलंकारः ॥ . नयनन्दी ने शब्द-अर्थ की समृद्धि, कोमल-पद, गम्भीर, उदार, छन्दानुवर्ती भादि सभी का ग्रहण अलंकार के भीतर किया है
चडियसरासणु व सुगुरगड्ढउ,
महकइकहबंधु व प्रत्यढउ । 2.5 वह महाकवि के ऐसे कथाबन्ध के समान था जो अर्थ से समृद्ध है।
कोमलपयं उपारं छंबाणुवरं गहीरमस्थळं ।
हियइच्छियसोहग्गं कस्स कलत्तं व इह कव्वं ॥ 8.1 कोमल-पद, उदार, छन्दानुवर्ती, गम्भीर, अर्थसमृद्ध तथा मनोवांछित सौंदर्ययुक्त कलत्र मौर काव्य इस संसार में किसी सौभाग्यशाली को ही प्राप्त होता है।
काव्य का लक्ष्य मात्र प्रानन्द प्राप्ति ही नहीं है। वरन् कवि की मंगलवाणी शाश्वतसुख अर्थात् मोक्ष-प्राप्ति का कारण भी है। काव्य के उपसंहार में नयनन्दी ने लिखा है