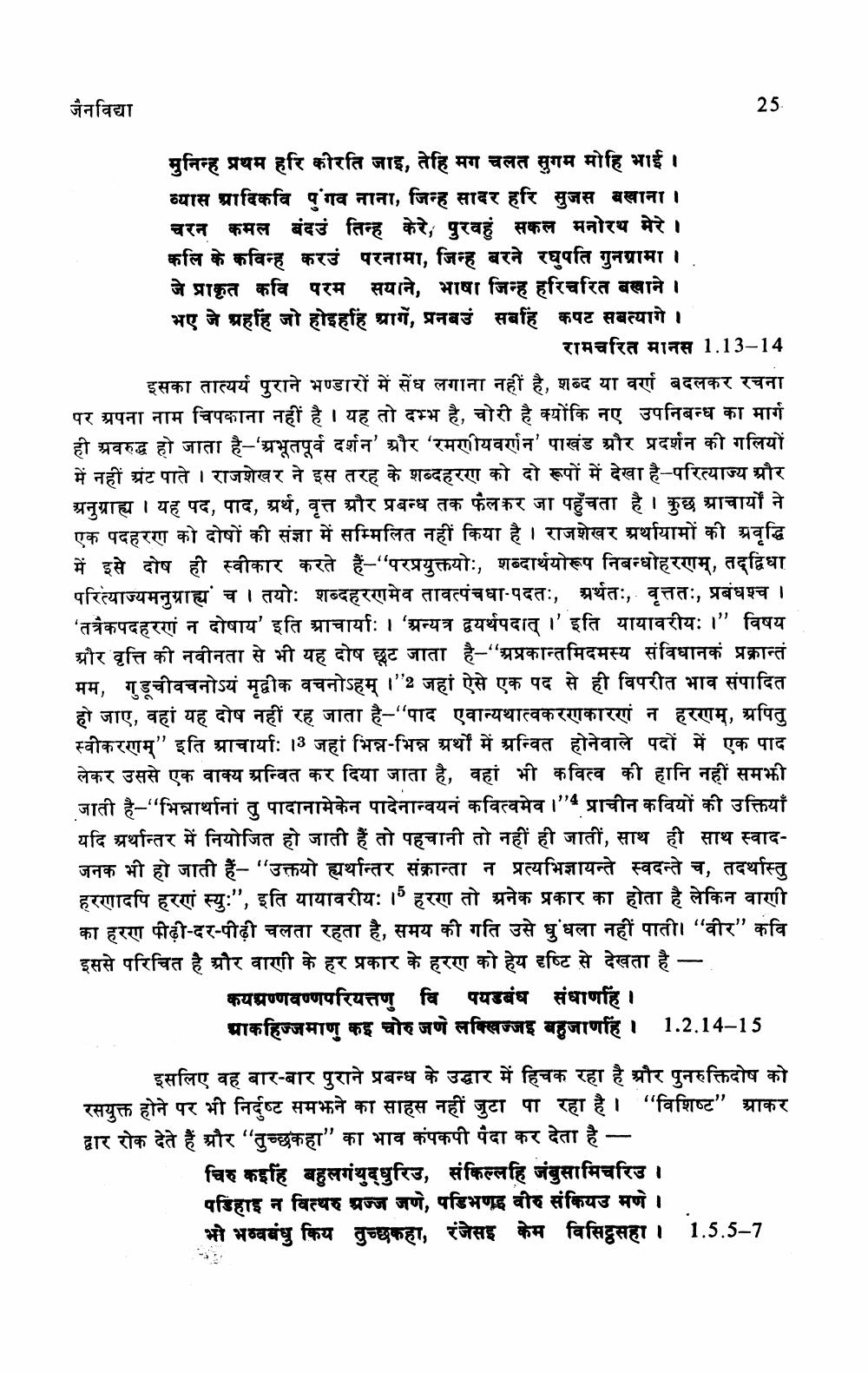________________
जैनविद्या
25.
मुनिन्ह प्रथम हरि कीरति जाइ, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। व्यास प्रादिकवि पुगव नाना, जिन्ह सादर हरि सुजस बखाना। चरन कमल बंदउं तिन्ह केरे, पुरवहुं सकल मनोरथ मेरे । कलि के कविन्ह करउं परनामा, जिन्ह बरने रघुपति गुनग्रामा । . जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन्ह हरिचरित बखाने । भए जे प्रहहिं जो होइहहिं प्रागें, प्रनबउं सबहिं कपट सबत्यागे ।
रामचरित मानस 1.13-14 इसका तात्यर्य पुराने भण्डारों में सेंध लगाना नहीं है, शब्द या वर्ण बदलकर रचना पर अपना नाम चिपकाना नहीं है । यह तो दम्भ है, चोरी है क्योंकि नए उपनिबन्ध का मार्ग ही अवरुद्ध हो जाता है-'अभूतपूर्व दर्शन' और 'रमणीयवर्णन' पाखंड और प्रदर्शन की गलियों में नहीं अंट पाते । राजशेखर ने इस तरह के शब्दहरण को दो रूपों में देखा है-परित्याज्य और अनुग्राह्य । यह पद, पाद, अर्थ, वृत्त और प्रबन्ध तक फैलकर जा पहुँचता है। कुछ आचार्यों ने एक पदहरण को दोषों की संज्ञा में सम्मिलित नहीं किया है । राजशेखर अर्थायामों की प्रवृद्धि में इसे दोष ही स्वीकार करते हैं-"परप्रयुक्तयोः, शब्दार्थयोरूप निबन्धोहरणम्, तद्विधा परित्याज्यमनुग्राह्य च । तयोः शब्दहरणमेव तावत्पंचधा-पदतः, अर्थतः, वृत्ततः, प्रबंधश्च । 'तत्रैकपदहरणं न दोषाय' इति प्राचार्याः । 'अन्यत्र द्वयर्थपदात् ।' इति यायावरीयः ।" विषय और वृत्ति की नवीनता से भी यह दोष छूट जाता है-"अप्रकान्तमिदमस्य संविधानकं प्रक्रान्तं मम, गुडूचीवचनोऽयं मृद्वीक वचनोऽहम् ।"2 जहां ऐसे एक पद से ही विपरीत भाव संपादित हो जाए, वहां यह दोष नहीं रह जाता है-“पाद एवान्यथात्वकरणकारणं न हरणम्, अपितु स्वीकरणम्" इति प्राचार्याः ।३ जहां भिन्न-भिन्न अर्थों में अन्वित होनेवाले पदों में एक पाद लेकर उससे एक वाक्य अन्वित कर दिया जाता है, वहां भी कवित्व की हानि नहीं समझी जाती है-"भिन्नार्थानां तु पादानामेकेन पादेनान्वयनं कवित्वमेव ।"4 प्राचीन कवियों की उक्तियाँ यदि अर्थान्तर में नियोजित हो जाती हैं तो पहचानी तो नहीं ही जातीं, साथ ही साथ स्वादजनक भी हो जाती हैं- "उक्तयो यर्थान्तर संक्रान्ता न प्रत्यभिज्ञायन्ते स्वदन्ते च, तदर्थास्तु हरणादपि हरणं स्युः", इति यायावरीयः । हरण तो अनेक प्रकार का होता है लेकिन वाणी का हरण पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलता रहता है, समय की गति उसे धुंधला नहीं पाती। "वीर" कवि इससे परिचित है और वाणी के हर प्रकार के हरण को हेय दृष्टि से देखता है -
कयमण्णवण्णपरियत्तणु वि पयडबंध संधाहिं ।
प्राकहिज्जमाणु कइ चोरु जणे लक्खिज्जइ बहुजाहिं। 1.2.14-15 इसलिए वह बार-बार पुराने प्रबन्ध के उद्धार में हिचक रहा है और पुनरुक्तिदोष को रसयुक्त होने पर भी निर्दुष्ट समझने का साहस नहीं जुटा पा रहा है। "विशिष्ट" आकर द्वार रोक देते हैं और "तुच्छकहा" का भाव कंपकपी पैदा कर देता है -
चिरु कहि बहुलगंथुधुरिउ, संकिल्लहि जंबुसामिचरिउ । पडिहाइ न वित्थर अज्ज जणे, पडिभणइ वीर संकियउ मणे । भो भव्वबंधु किय तुच्छकहा, रंजेसइ केम विसिट्ठसहा । 1.5.5-7