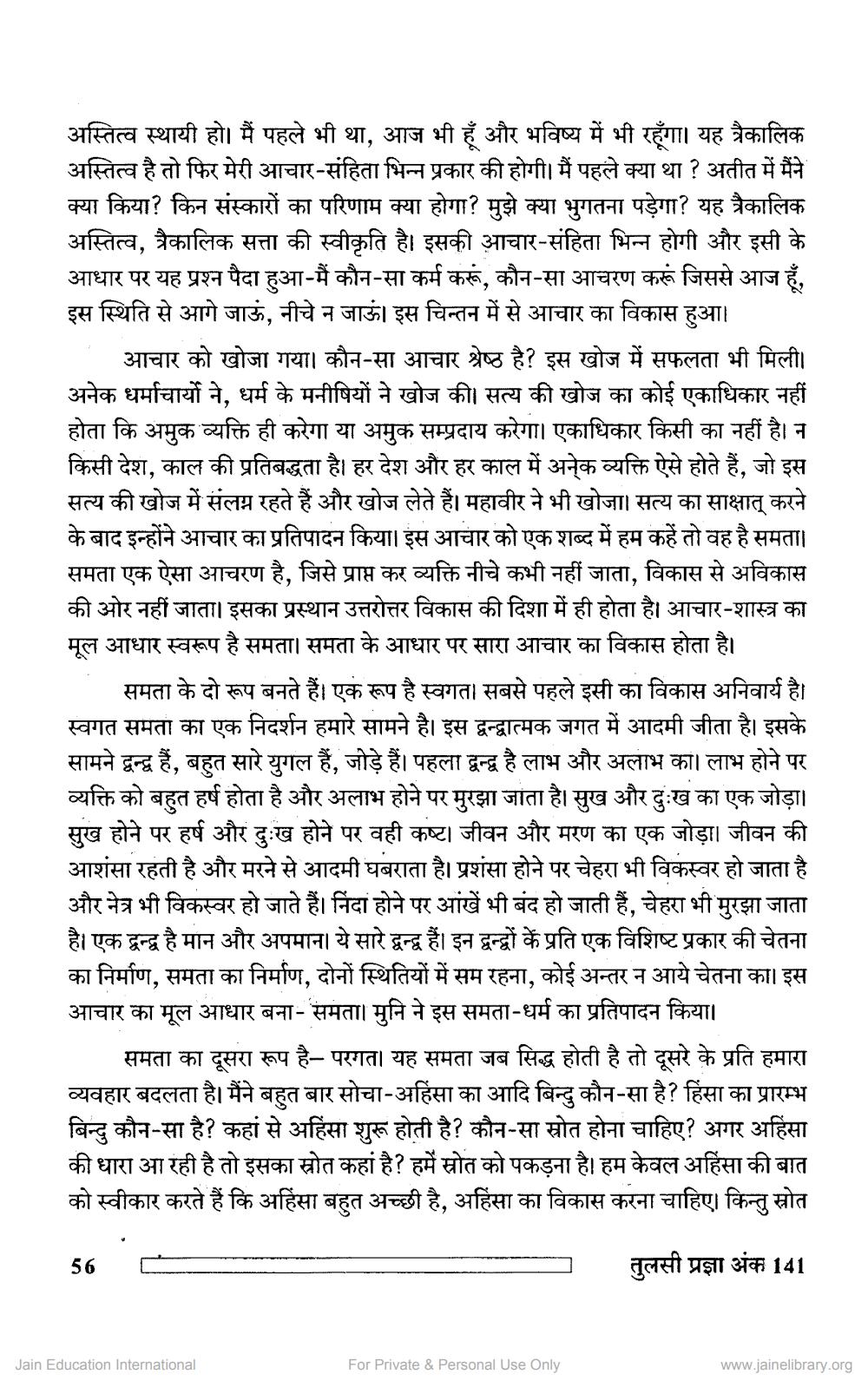________________
अस्तित्व स्थायी हो। मैं पहले भी था, आज भी हूँ और भविष्य में भी रहँगा। यह त्रैकालिक अस्तित्व है तो फिर मेरी आचार-संहिता भिन्न प्रकार की होगी। मैं पहले क्या था ? अतीत में मैंने क्या किया? किन संस्कारों का परिणाम क्या होगा? मुझे क्या भुगतना पड़ेगा? यह त्रैकालिक अस्तित्व, त्रैकालिक सत्ता की स्वीकृति है। इसकी आचार-संहिता भिन्न होगी और इसी के आधार पर यह प्रश्न पैदा हुआ-मैं कौन-सा कर्म करूं, कौन-सा आचरण करूं जिससे आज हैं, इस स्थिति से आगे जाऊं, नीचे न जाऊं। इस चिन्तन में से आचार का विकास हुआ।
आचार को खोजा गया। कौन-सा आचार श्रेष्ठ है? इस खोज में सफलता भी मिली। अनेक धर्माचार्यों ने, धर्म के मनीषियों ने खोज की। सत्य की खोज का कोई एकाधिकार नहीं होता कि अमुक व्यक्ति ही करेगा या अमुक सम्प्रदाय करेगा। एकाधिकार किसी का नहीं है। न किसी देश, काल की प्रतिबद्धता है। हर देश और हर काल में अनेक व्यक्ति ऐसे होते हैं, जो इस सत्य की खोज में संलग्न रहते हैं और खोज लेते हैं। महावीर ने भी खोजा। सत्य का साक्षात् करने के बाद इन्होंने आचार का प्रतिपादन किया। इस आचार को एक शब्द में हम कहें तो वह है समता। समता एक ऐसा आचरण है, जिसे प्राप्त कर व्यक्ति नीचे कभी नहीं जाता, विकास से अविकास की ओर नहीं जाता। इसका प्रस्थान उत्तरोत्तर विकास की दिशा में ही होता है। आचार-शास्त्र का मूल आधार स्वरूप है समता। समता के आधार पर सारा आचार का विकास होता है।
समता के दो रूप बनते हैं। एक रूप है स्वगत। सबसे पहले इसी का विकास अनिवार्य है। स्वगत समता का एक निदर्शन हमारे सामने है। इस द्वन्द्वात्मक जगत में आदमी जीता है। इसके सामने द्वन्द्व हैं, बहुत सारे युगल हैं, जोड़े हैं। पहला द्वन्द्व है लाभ और अलाभ का। लाभ होने पर व्यक्ति को बहुत हर्ष होता है और अलाभ होने पर मुरझा जाता है। सुख और दुःख का एक जोड़ा। सुख होने पर हर्ष और दुःख होने पर वही कष्ट। जीवन और मरण का एक जोड़ा। जीवन की आशंसा रहती है और मरने से आदमी घबराता है। प्रशंसा होने पर चेहरा भी विकस्वर हो जाता है
और नेत्र भी विकस्वर हो जाते हैं। निंदा होने पर आंखें भी बंद हो जाती हैं, चेहरा भी मुरझा जाता है। एक द्वन्द्व है मान और अपमान। ये सारे द्वन्द्व हैं। इन द्वन्द्वों के प्रति एक विशिष्ट प्रकार की चेतना का निर्माण, समता का निर्माण, दोनों स्थितियों में सम रहना, कोई अन्तर न आये चेतना का। इस आचार का मूल आधार बना- समता। मुनि ने इस समता-धर्म का प्रतिपादन किया।
समता का दूसरा रूप है- परगत। यह समता जब सिद्ध होती है तो दूसरे के प्रति हमारा व्यवहार बदलता है। मैंने बहुत बार सोचा-अहिंसा का आदि बिन्दु कौन-सा है? हिंसा का प्रारम्भ बिन्दु कौन-सा है? कहां से अहिंसा शुरू होती है? कौन-सा स्रोत होना चाहिए? अगर अहिंसा की धारा आ रही है तो इसका स्रोत कहां है? हमें स्रोत को पकड़ना है। हम केवल अहिंसा की बात को स्वीकार करते हैं कि अहिंसा बहुत अच्छी है, अहिंसा का विकास करना चाहिए। किन्तु स्रोत
56
-
तुलसी प्रज्ञा अंक 141
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org