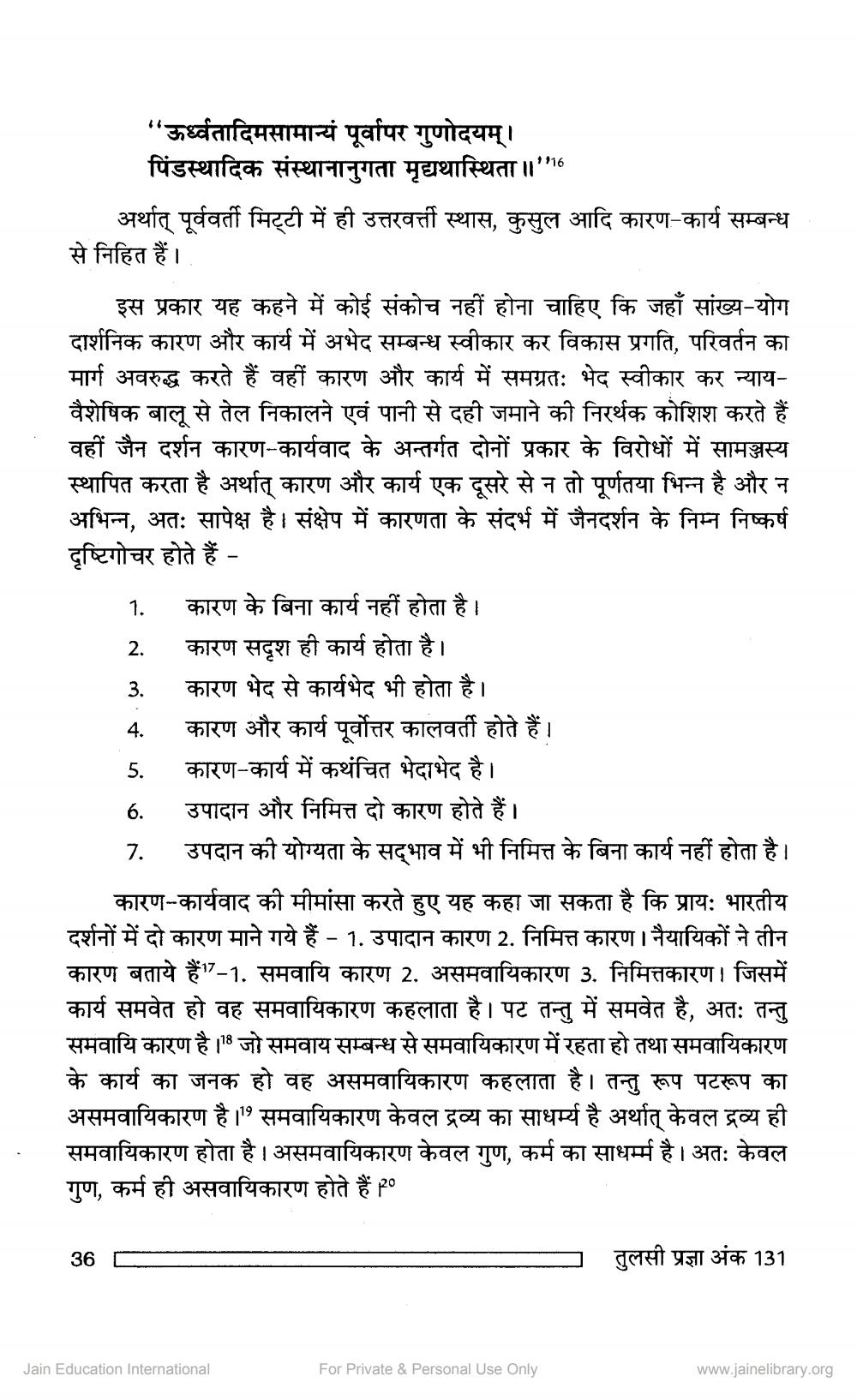________________
"ऊर्ध्वतादिमसामान्यं पूर्वापर गुणोदयम्। पिंडस्थादिक संस्थानानुगता मृद्यथास्थिता ।।16
अर्थात् पूर्ववर्ती मिट्टी में ही उत्तरवर्ती स्थास, कुसुल आदि कारण-कार्य सम्बन्ध से निहित हैं।
इस प्रकार यह कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि जहाँ सांख्य-योग दार्शनिक कारण और कार्य में अभेद सम्बन्ध स्वीकार कर विकास प्रगति, परिवर्तन का मार्ग अवरुद्ध करते हैं वहीं कारण और कार्य में समग्रतः भेद स्वीकार कर न्यायवैशेषिक बालू से तेल निकालने एवं पानी से दही जमाने की निरर्थक कोशिश करते हैं वहीं जैन दर्शन कारण-कार्यवाद के अन्तर्गत दोनों प्रकार के विरोधों में सामञ्जस्य स्थापित करता है अर्थात् कारण और कार्य एक दूसरे से न तो पूर्णतया भिन्न है और न अभिन्न, अतः सापेक्ष है। संक्षेप में कारणता के संदर्भ में जैनदर्शन के निम्न निष्कर्ष दृष्टिगोचर होते हैं -
1. कारण के बिना कार्य नहीं होता है। 2. कारण सदृश ही कार्य होता है।
कारण भेद से कार्यभेद भी होता है।
कारण और कार्य पूर्वोत्तर कालवर्ती होते हैं। 5. कारण-कार्य में कथंचित भेदाभेद है। 6. उपादान और निमित्त दो कारण होते हैं। 7. उपदान की योग्यता के सद्भाव में भी निमित्त के बिना कार्य नहीं होता है।
कारण-कार्यवाद की मीमांसा करते हुए यह कहा जा सकता है कि प्रायः भारतीय दर्शनों में दो कारण माने गये हैं - 1. उपादान कारण 2. निमित्त कारण। नैयायिकों ने तीन कारण बताये हैं7-1. समवायि कारण 2. असमवायिकारण 3. निमित्तकारण। जिसमें कार्य समवेत हो वह समवायिकारण कहलाता है। पट तन्तु में समवेत है, अतः तन्तु समवायि कारण है। जो समवाय सम्बन्ध से समवायिकारण में रहता हो तथा समवायिकारण के कार्य का जनक हो वह असमवायिकारण कहलाता है। तन्तु रूप पटरूप का असमवायिकारण है। समवायिकारण केवल द्रव्य का साधर्म्य है अर्थात् केवल द्रव्य ही समवायिकारण होता है। असमवायिकारण केवल गुण, कर्म का साधर्म है। अतः केवल गुण, कर्म ही असवायिकारण होते हैं ।
36
-
तुलसी प्रज्ञा अंक 131
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org