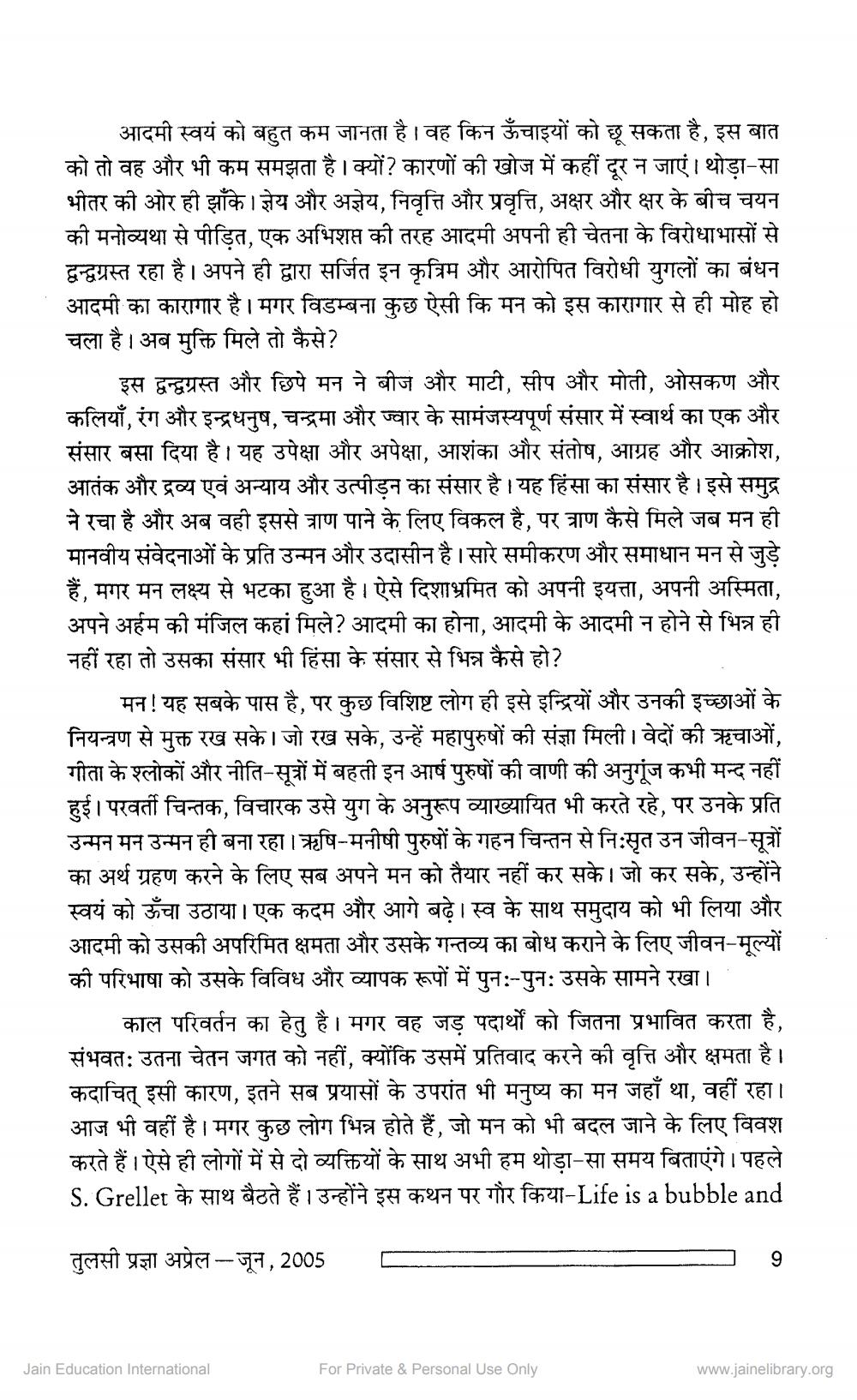________________
आदमी स्वयं को बहुत कम जानता है। वह किन ऊँचाइयों को छू सकता है, इस बात को तो वह और भी कम समझता है। क्यों? कारणों की खोज में कहीं दूर न जाएं। थोड़ा-सा भीतर की ओर ही झाँके । ज्ञेय और अज्ञेय, निवृत्ति और प्रवृत्ति, अक्षर और क्षर के बीच चयन की मनोव्यथा से पीड़ित, एक अभिशप्त की तरह आदमी अपनी ही चेतना के विरोधाभासों से द्वन्द्वग्रस्त रहा है। अपने ही द्वारा सर्जित इन कृत्रिम और आरोपित विरोधी युगलों का बंधन आदमी का कारागार है। मगर विडम्बना कुछ ऐसी कि मन को इस कारागार से ही मोह हो चला है। अब मुक्ति मिले तो कैसे?
इस द्वन्द्वग्रस्त और छिपे मन ने बीज और माटी, सीप और मोती, ओसकण और कलियाँ, रंग और इन्द्रधनुष, चन्द्रमा और ज्वार के सामंजस्यपूर्ण संसार में स्वार्थ का एक और संसार बसा दिया है। यह उपेक्षा और अपेक्षा, आशंका और संतोष, आग्रह और आक्रोश, आतंक और द्रव्य एवं अन्याय और उत्पीड़न का संसार है। यह हिंसा का संसार है। इसे समुद्र ने रचा है और अब वही इससे त्राण पाने के लिए विकल है, पर त्राण कैसे मिले जब मन ही मानवीय संवेदनाओं के प्रति उन्मन और उदासीन है। सारे समीकरण और समाधान मन से जुड़े हैं, मगर मन लक्ष्य से भटका हुआ है। ऐसे दिशाभ्रमित को अपनी इयत्ता, अपनी अस्मिता, अपने अहम की मंजिल कहां मिले? आदमी का होना, आदमी के आदमी न होने से भिन्न ही नहीं रहा तो उसका संसार भी हिंसा के संसार से भिन्न कैसे हो?
मन ! यह सबके पास है, पर कुछ विशिष्ट लोग ही इसे इन्द्रियों और उनकी इच्छाओं के नियन्त्रण से मुक्त रख सके। जो रख सके, उन्हें महापुरुषों की संज्ञा मिली। वेदों की ऋचाओं, गीता के श्लोकों और नीति-सूत्रों में बहती इन आर्ष पुरुषों की वाणी की अनुगूंज कभी मन्द नहीं हुई। परवर्ती चिन्तक, विचारक उसे युग के अनुरूप व्याख्यायित भी करते रहे, पर उनके प्रति उन्मन मन उन्मन ही बना रहा। ऋषि-मनीषी पुरुषों के गहन चिन्तन से निःसृत उन जीवन-सूत्रों का अर्थ ग्रहण करने के लिए सब अपने मन को तैयार नहीं कर सके। जो कर सके, उन्होंने स्वयं को ऊँचा उठाया। एक कदम और आगे बढ़े। स्व के साथ समुदाय को भी लिया और आदमी को उसकी अपरिमित क्षमता और उसके गन्तव्य का बोध कराने के लिए जीवन-मूल्यों की परिभाषा को उसके विविध और व्यापक रूपों में पुन:-पुनः उसके सामने रखा।
काल परिवर्तन का हेतु है। मगर वह जड़ पदार्थों को जितना प्रभावित करता है, संभवत: उतना चेतन जगत को नहीं, क्योंकि उसमें प्रतिवाद करने की वृत्ति और क्षमता है। कदाचित् इसी कारण, इतने सब प्रयासों के उपरांत भी मनुष्य का मन जहाँ था, वहीं रहा। आज भी वहीं है। मगर कुछ लोग भिन्न होते हैं, जो मन को भी बदल जाने के लिए विवश करते हैं। ऐसे ही लोगों में से दो व्यक्तियों के साथ अभी हम थोड़ा-सा समय बिताएंगे। पहले S. Grellet के साथ बैठते हैं। उन्होंने इस कथन पर गौर किया-Life is a bubble and
तुलसी प्रज्ञा अप्रेल-जून, 2005
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org