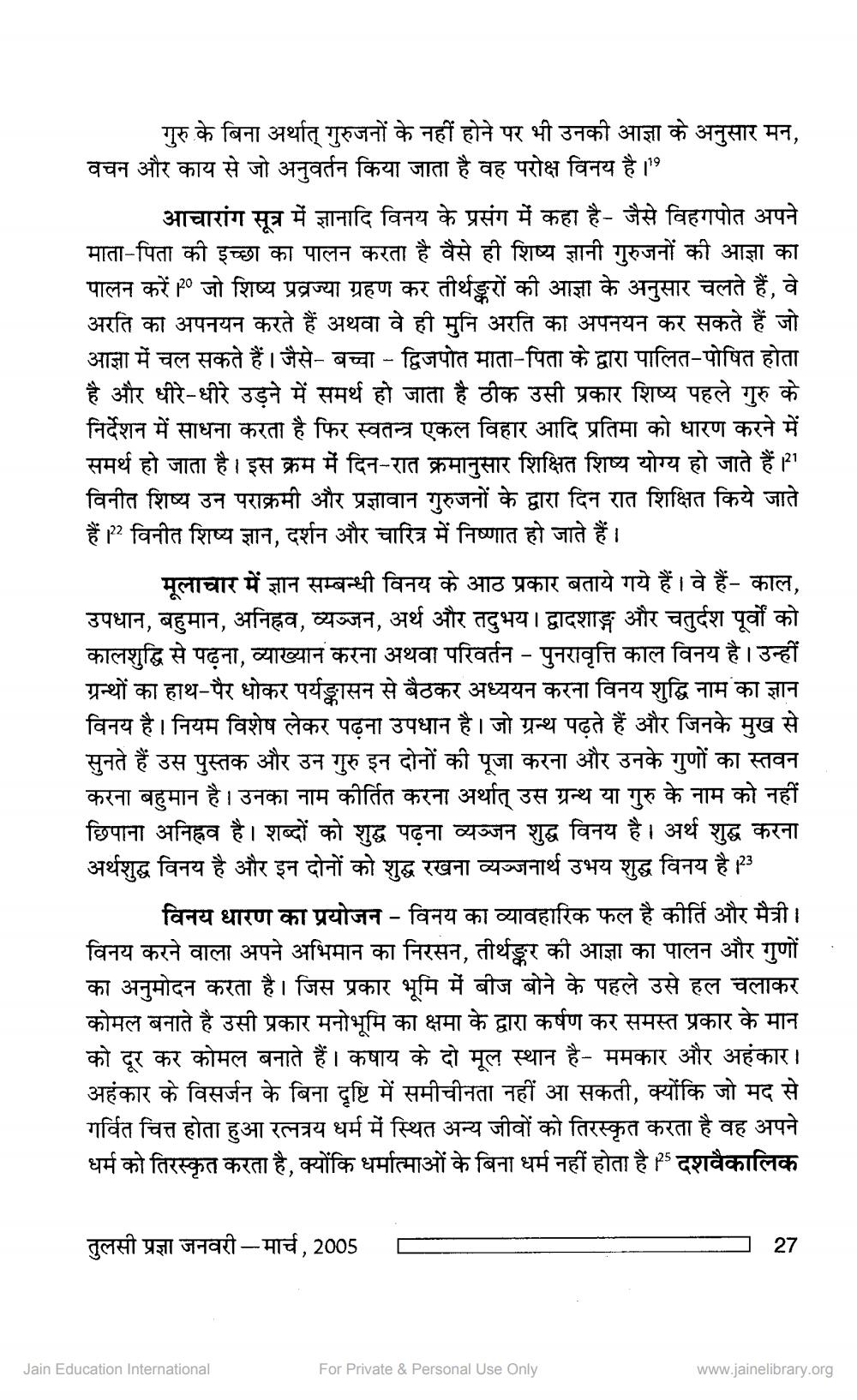________________
गुरु के बिना अर्थात् गुरुजनों के नहीं होने पर भी उनकी आज्ञा के अनुसार मन, वचन और काय से जो अनुवर्तन किया जाता है वह परोक्ष विनय है।
आचारांग सूत्र में ज्ञानादि विनय के प्रसंग में कहा है- जैसे विहगपोत अपने माता-पिता की इच्छा का पालन करता है वैसे ही शिष्य ज्ञानी गुरुजनों की आज्ञा का पालन करें। जो शिष्य प्रव्रज्या ग्रहण कर तीर्थङ्करों की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, वे अरति का अपनयन करते हैं अथवा वे ही मुनि अरति का अपनयन कर सकते हैं जो आज्ञा में चल सकते हैं। जैसे- बच्चा - द्विजपोत माता-पिता के द्वारा पालित-पोषित होता है और धीरे-धीरे उड़ने में समर्थ हो जाता है ठीक उसी प्रकार शिष्य पहले गुरु के निर्देशन में साधना करता है फिर स्वतन्त्र एकल विहार आदि प्रतिमा को धारण करने में समर्थ हो जाता है। इस क्रम में दिन-रात क्रमानुसार शिक्षित शिष्य योग्य हो जाते हैं। विनीत शिष्य उन पराक्रमी और प्रज्ञावान गुरुजनों के द्वारा दिन रात शिक्षित किये जाते हैं। विनीत शिष्य ज्ञान, दर्शन और चारित्र में निष्णात हो जाते हैं।
मूलाचार में ज्ञान सम्बन्धी विनय के आठ प्रकार बताये गये हैं। वे हैं- काल, उपधान, बहुमान, अनिह्नव, व्यञ्जन, अर्थ और तदुभय। द्वादशाङ्ग और चतुर्दश पूर्वो को कालशुद्धि से पढ़ना, व्याख्यान करना अथवा परिवर्तन - पुनरावृत्ति काल विनय है। उन्हीं ग्रन्थों का हाथ-पैर धोकर पर्यङ्कासन से बैठकर अध्ययन करना विनय शुद्धि नाम का ज्ञान विनय है। नियम विशेष लेकर पढ़ना उपधान है। जो ग्रन्थ पढ़ते हैं और जिनके मुख से सुनते हैं उस पुस्तक और उन गुरु इन दोनों की पूजा करना और उनके गुणों का स्तवन करना बहुमान है। उनका नाम कीर्तित करना अर्थात् उस ग्रन्थ या गुरु के नाम को नहीं छिपाना अनिह्नव है। शब्दों को शुद्ध पढ़ना व्यञ्जन शुद्ध विनय है। अर्थ शुद्ध करना अर्थशुद्ध विनय है और इन दोनों को शुद्ध रखना व्यञ्जनार्थ उभय शुद्ध विनय है।23
विनय धारण का प्रयोजन - विनय का व्यावहारिक फल है कीर्ति और मैत्री। विनय करने वाला अपने अभिमान का निरसन, तीर्थङ्कर की आज्ञा का पालन और गुणों का अनुमोदन करता है। जिस प्रकार भूमि में बीज बोने के पहले उसे हल चलाकर कोमल बनाते है उसी प्रकार मनोभूमि का क्षमा के द्वारा कर्षण कर समस्त प्रकार के मान को दूर कर कोमल बनाते हैं। कषाय के दो मूल स्थान है- ममकार और अहंकार। अहंकार के विसर्जन के बिना दृष्टि में समीचीनता नहीं आ सकती, क्योंकि जो मद से गर्वित चित्त होता हुआ रत्नत्रय धर्म में स्थित अन्य जीवों को तिरस्कृत करता है वह अपने धर्म को तिरस्कृत करता है, क्योंकि धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं होता है । दशवैकालिक
तुलसी प्रज्ञा जनवरी-मार्च, 2005
-
27
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org