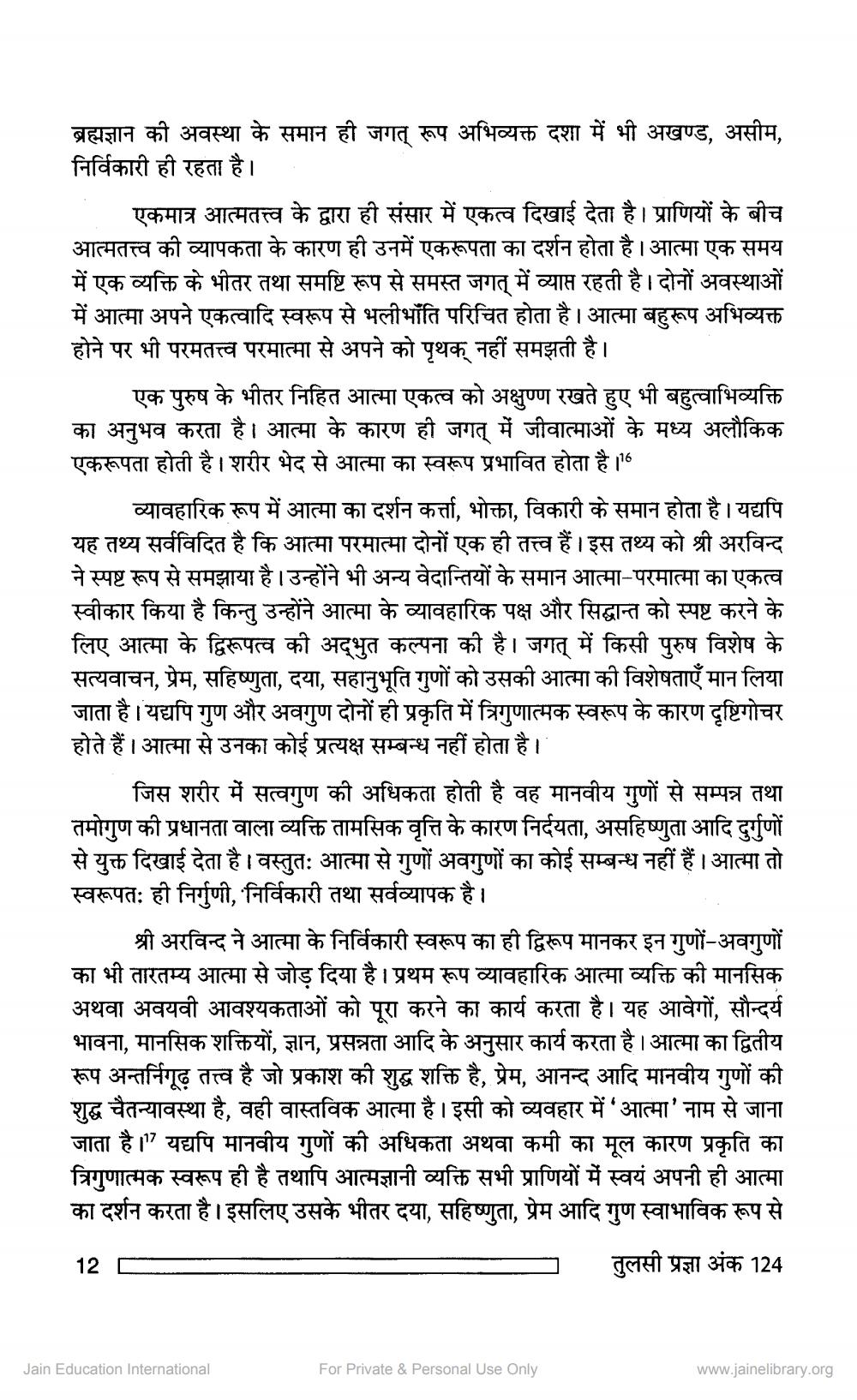________________
ब्रह्मज्ञान की अवस्था के समान ही जगत् रूप अभिव्यक्त दशा में भी अखण्ड, असीम, निर्विकारी ही रहता है।
___ एकमात्र आत्मतत्त्व के द्वारा ही संसार में एकत्व दिखाई देता है। प्राणियों के बीच आत्मतत्त्व की व्यापकता के कारण ही उनमें एकरूपता का दर्शन होता है। आत्मा एक समय में एक व्यक्ति के भीतर तथा समष्टि रूप से समस्त जगत् में व्याप्त रहती है। दोनों अवस्थाओं में आत्मा अपने एकत्वादि स्वरूप से भलीभाँति परिचित होता है। आत्मा बहुरूप अभिव्यक्त होने पर भी परमतत्त्व परमात्मा से अपने को पृथक् नहीं समझती है।
एक पुरुष के भीतर निहित आत्मा एकत्व को अक्षुण्ण रखते हुए भी बहुत्वाभिव्यक्ति का अनुभव करता है। आत्मा के कारण ही जगत् में जीवात्माओं के मध्य अलौकिक एकरूपता होती है। शरीर भेद से आत्मा का स्वरूप प्रभावित होता है।
व्यावहारिक रूप में आत्मा का दर्शन कर्ता, भोक्ता, विकारी के समान होता है। यद्यपि यह तथ्य सर्वविदित है कि आत्मा परमात्मा दोनों एक ही तत्त्व हैं। इस तथ्य को श्री अरविन्द ने स्पष्ट रूप से समझाया है। उन्होंने भी अन्य वेदान्तियों के समान आत्मा-परमात्मा का एकत्व स्वीकार किया है किन्तु उन्होंने आत्मा के व्यावहारिक पक्ष और सिद्धान्त को स्पष्ट करने के लिए आत्मा के द्विरूपत्व की अद्भुत कल्पना की है। जगत् में किसी पुरुष विशेष के सत्यवाचन, प्रेम, सहिष्णुता, दया, सहानुभूति गुणों को उसकी आत्मा की विशेषताएँ मान लिया जाता है । यद्यपि गुण और अवगुण दोनों ही प्रकृति में त्रिगुणात्मक स्वरूप के कारण दृष्टिगोचर होते हैं। आत्मा से उनका कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता है।
जिस शरीर में सत्वगुण की अधिकता होती है वह मानवीय गुणों से सम्पन्न तथा तमोगुण की प्रधानता वाला व्यक्ति तामसिक वृत्ति के कारण निर्दयता, असहिष्णुता आदि दुर्गुणों से युक्त दिखाई देता है। वस्तुतः आत्मा से गुणों अवगुणों का कोई सम्बन्ध नहीं हैं। आत्मा तो स्वरूपतः ही निर्गुणी, निर्विकारी तथा सर्वव्यापक है।
श्री अरविन्द ने आत्मा के निर्विकारी स्वरूप का ही द्विरूप मानकर इन गुणों-अवगुणों का भी तारतम्य आत्मा से जोड़ दिया है। प्रथम रूप व्यावहारिक आत्मा व्यक्ति की मानसिक अथवा अवयवी आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य करता है। यह आवेगों, सौन्दर्य भावना, मानसिक शक्तियों, ज्ञान, प्रसन्नता आदि के अनुसार कार्य करता है। आत्मा का द्वितीय रूप अन्तर्निगूढ तत्त्व है जो प्रकाश की शुद्ध शक्ति है, प्रेम, आनन्द आदि मानवीय गुणों की शुद्ध चैतन्यावस्था है, वही वास्तविक आत्मा है। इसी को व्यवहार में 'आत्मा' नाम से जाना जाता है।” यद्यपि मानवीय गुणों की अधिकता अथवा कमी का मूल कारण प्रकृति का त्रिगुणात्मक स्वरूप ही है तथापि आत्मज्ञानी व्यक्ति सभी प्राणियों में स्वयं अपनी ही आत्मा का दर्शन करता है। इसलिए उसके भीतर दया, सहिष्णुता, प्रेम आदि गुण स्वाभाविक रूप से
- तुलसी प्रज्ञा अंक 124
12
-
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org