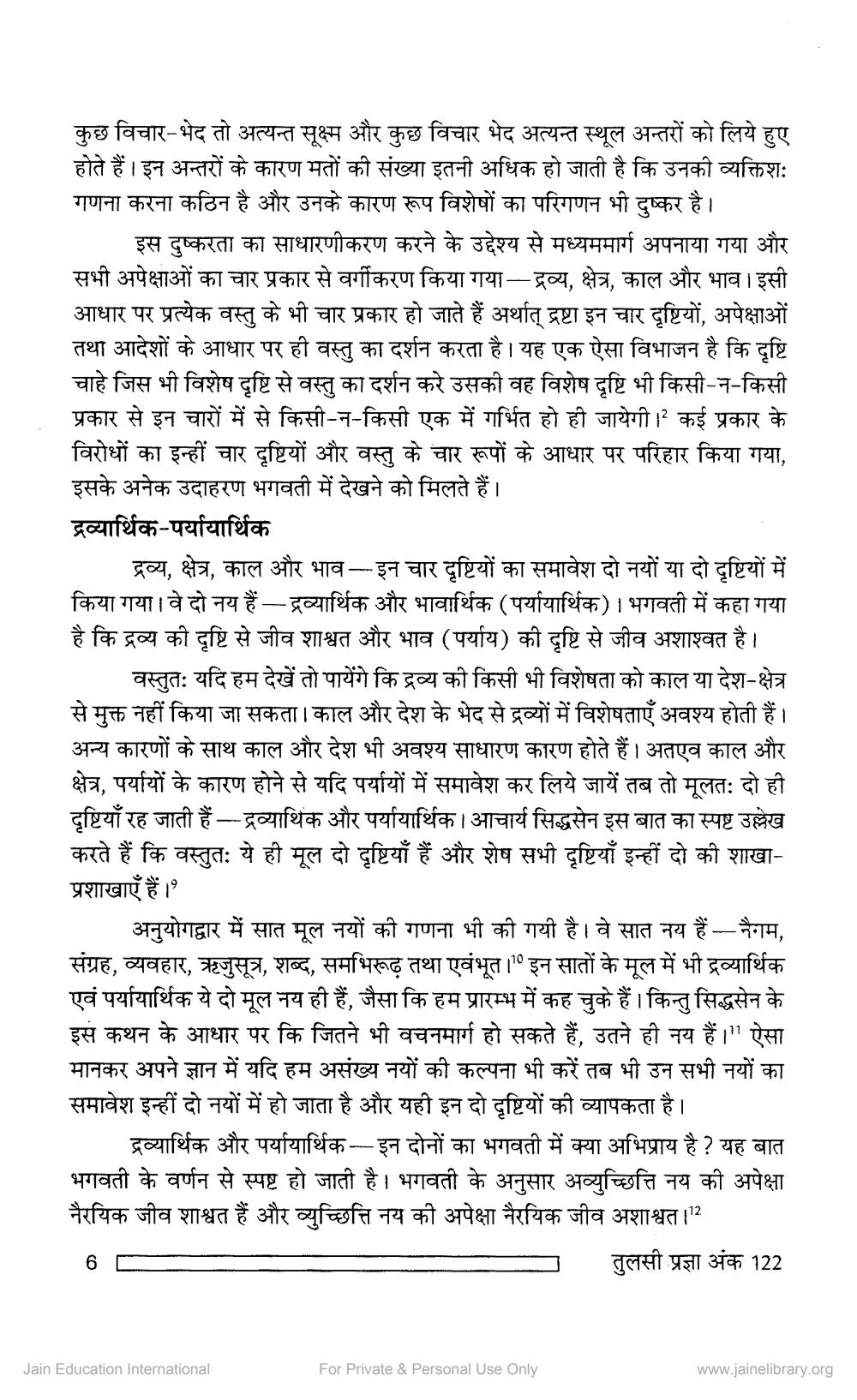________________
कुछ विचार-भेद तो अत्यन्त सूक्ष्म और कुछ विचार भेद अत्यन्त स्थूल अन्तरों को लिये हुए होते हैं। इन अन्तरों के कारण मतों की संख्या इतनी अधिक हो जाती है कि उनकी व्यक्तिशः गणना करना कठिन है और उनके कारण रूप विशेषों का परिगणन भी दुष्कर है।
__ इस दुष्करता का साधारणीकरण करने के उद्देश्य से मध्यममार्ग अपनाया गया और सभी अपेक्षाओं का चार प्रकार से वर्गीकरण किया गया-द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव । इसी आधार पर प्रत्येक वस्तु के भी चार प्रकार हो जाते हैं अर्थात् द्रष्टा इन चार दृष्टियों, अपेक्षाओं तथा आदेशों के आधार पर ही वस्तु का दर्शन करता है। यह एक ऐसा विभाजन है कि दृष्टि चाहे जिस भी विशेष दृष्टि से वस्तु का दर्शन करे उसकी वह विशेष दृष्टि भी किसी-न-किसी प्रकार से इन चारों में से किसी-न-किसी एक में गर्भित हो ही जायेगी। कई प्रकार के विरोधों का इन्हीं चार दृष्टियों और वस्तु के चार रूपों के आधार पर परिहार किया गया, इसके अनेक उदाहरण भगवती में देखने को मिलते हैं। द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक
द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव-इन चार दृष्टियों का समावेश दो नयों या दो दृष्टियों में किया गया। वे दो नय हैं-द्रव्यार्थिक और भावार्थिक (पर्यायार्थिक)। भगवती में कहा गया है कि द्रव्य की दृष्टि से जीव शाश्वत और भाव (पर्याय) की दृष्टि से जीव अशाश्वत है।
वस्तुत: यदि हम देखें तो पायेंगे कि द्रव्य की किसी भी विशेषता को काल या देश-क्षेत्र से मुक्त नहीं किया जा सकता। काल और देश के भेद से द्रव्यों में विशेषताएँ अवश्य होती हैं। अन्य कारणों के साथ काल और देश भी अवश्य साधारण कारण होते हैं। अतएव काल और क्षेत्र, पर्यायों के कारण होने से यदि पर्यायों में समावेश कर लिये जायें तब तो मूलतः दो ही दृष्टियाँ रह जाती हैं --द्रव्याथिक और पर्यायार्थिक। आचार्य सिद्धसेन इस बात का स्पष्ट उल्लेख करते हैं कि वस्तुतः ये ही मूल दो दृष्टियाँ हैं और शेष सभी दृष्टियाँ इन्हीं दो की शाखाप्रशाखाएँ हैं।'
___ अनुयोगद्वार में सात मूल नयों की गणना भी की गयी है। वे सात नय हैं—नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ तथा एवंभूत। इन सातों के मूल में भी द्रव्यार्थिक एवं पर्यायार्थिक ये दो मूल नय ही हैं, जैसा कि हम प्रारम्भ में कह चुके हैं। किन्तु सिद्धसेन के इस कथन के आधार पर कि जितने भी वचनमार्ग हो सकते हैं, उतने ही नय हैं। ऐसा मानकर अपने ज्ञान में यदि हम असंख्य नयों की कल्पना भी करें तब भी उन सभी नयों का समावेश इन्हीं दो नयों में हो जाता है और यही इन दो दृष्टियों की व्यापकता है।
द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक-इन दोनों का भगवती में क्या अभिप्राय है? यह बात भगवती के वर्णन से स्पष्ट हो जाती है। भगवती के अनुसार अव्युच्छित्ति नय की अपेक्षा नैरयिक जीव शाश्वत हैं और व्युच्छित्ति नय की अपेक्षा नैरयिक जीव अशाश्वत ।12 6
- तुलसी प्रज्ञा अंक 122
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org