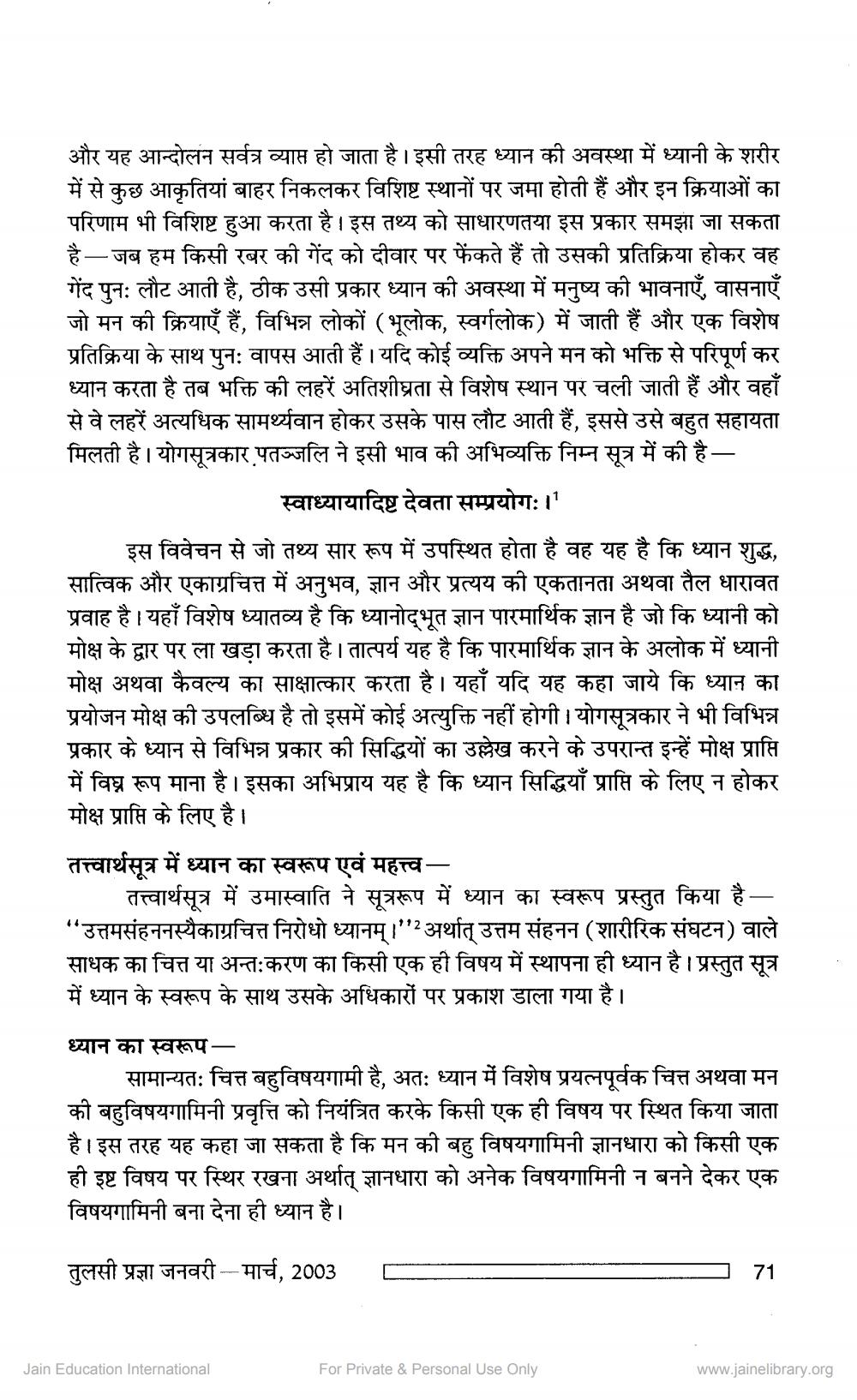________________
और यह आन्दोलन सर्वत्र व्याप्त हो जाता है। इसी तरह ध्यान की अवस्था में ध्यानी के शरीर में से कुछ आकृतियां बाहर निकलकर विशिष्ट स्थानों पर जमा होती हैं और इन क्रियाओं का परिणाम भी विशिष्ट हुआ करता है। इस तथ्य को साधारणतया इस प्रकार समझा जा सकता है— जब हम किसी रबर की गेंद को दीवार पर फेंकते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया होकर वह गेंद पुनः लौट आती है, ठीक उसी प्रकार ध्यान की अवस्था में मनुष्य की भावनाएँ, वासनाएँ जो मन की क्रियाएँ हैं, विभिन्न लोकों (भूलोक, स्वर्गलोक) में जाती हैं और एक विशेष प्रतिक्रिया के साथ पुनः वापस आती हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने मन को भक्ति से परिपूर्ण कर ध्यान करता है तब भक्ति की लहरें अतिशीघ्रता से विशेष स्थान पर चली जाती हैं और वहाँ से वे लहरें अत्यधिक सामर्थ्यवान होकर उसके पास लौट आती हैं, इससे उसे बहुत सहायता मिलती है। योगसूत्रकार पतञ्जलि ने इसी भाव की अभिव्यक्ति निम्न सूत्र में की है
स्वाध्यायादिष्ट देवता सम्प्रयोगः।' इस विवेचन से जो तथ्य सार रूप में उपस्थित होता है वह यह है कि ध्यान शुद्ध, सात्विक और एकाग्रचित्त में अनुभव, ज्ञान और प्रत्यय की एकतानता अथवा तैल धारावत प्रवाह है। यहाँ विशेष ध्यातव्य है कि ध्यानोद्भूत ज्ञान पारमार्थिक ज्ञान है जो कि ध्यानी को मोक्ष के द्वार पर ला खड़ा करता है । तात्पर्य यह है कि पारमार्थिक ज्ञान के अलोक में ध्यानी मोक्ष अथवा कैवल्य का साक्षात्कार करता है। यहाँ यदि यह कहा जाये कि ध्यान का प्रयोजन मोक्ष की उपलब्धि है तो इसमें कोई अत्युक्ति नहीं होगी। योगसूत्रकार ने भी विभिन्न प्रकार के ध्यान से विभिन्न प्रकार की सिद्धियों का उल्लेख करने के उपरान्त इन्हें मोक्ष प्राप्ति में विघ्न रूप माना है। इसका अभिप्राय यह है कि ध्यान सिद्धियाँ प्राप्ति के लिए न होकर मोक्ष प्राप्ति के लिए है। तत्त्वार्थसूत्र में ध्यान का स्वरूप एवं महत्त्व
तत्त्वार्थसूत्र में उमास्वाति ने सूत्ररूप में ध्यान का स्वरूप प्रस्तुत किया है"उत्तमसंहननस्यैकाग्रचित्त निरोधो ध्यानम्।" अर्थात् उत्तम संहनन (शारीरिक संघटन) वाले साधक का चित्त या अन्तःकरण का किसी एक ही विषय में स्थापना ही ध्यान है। प्रस्तुत सूत्र में ध्यान के स्वरूप के साथ उसके अधिकारों पर प्रकाश डाला गया है।
ध्यान का स्वरूप
सामान्यतः चित्त बहुविषयगामी है, अतः ध्यान में विशेष प्रयत्नपूर्वक चित्त अथवा मन की बहुविषयगामिनी प्रवृत्ति को नियंत्रित करके किसी एक ही विषय पर स्थित किया जाता है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि मन की बहु विषयगामिनी ज्ञानधारा को किसी एक ही इष्ट विषय पर स्थिर रखना अर्थात् ज्ञानधारा को अनेक विषयगामिनी न बनने देकर एक विषयगामिनी बना देना ही ध्यान है।
तुलसी प्रज्ञा जनवरी-मार्च, 2003
-
71
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org