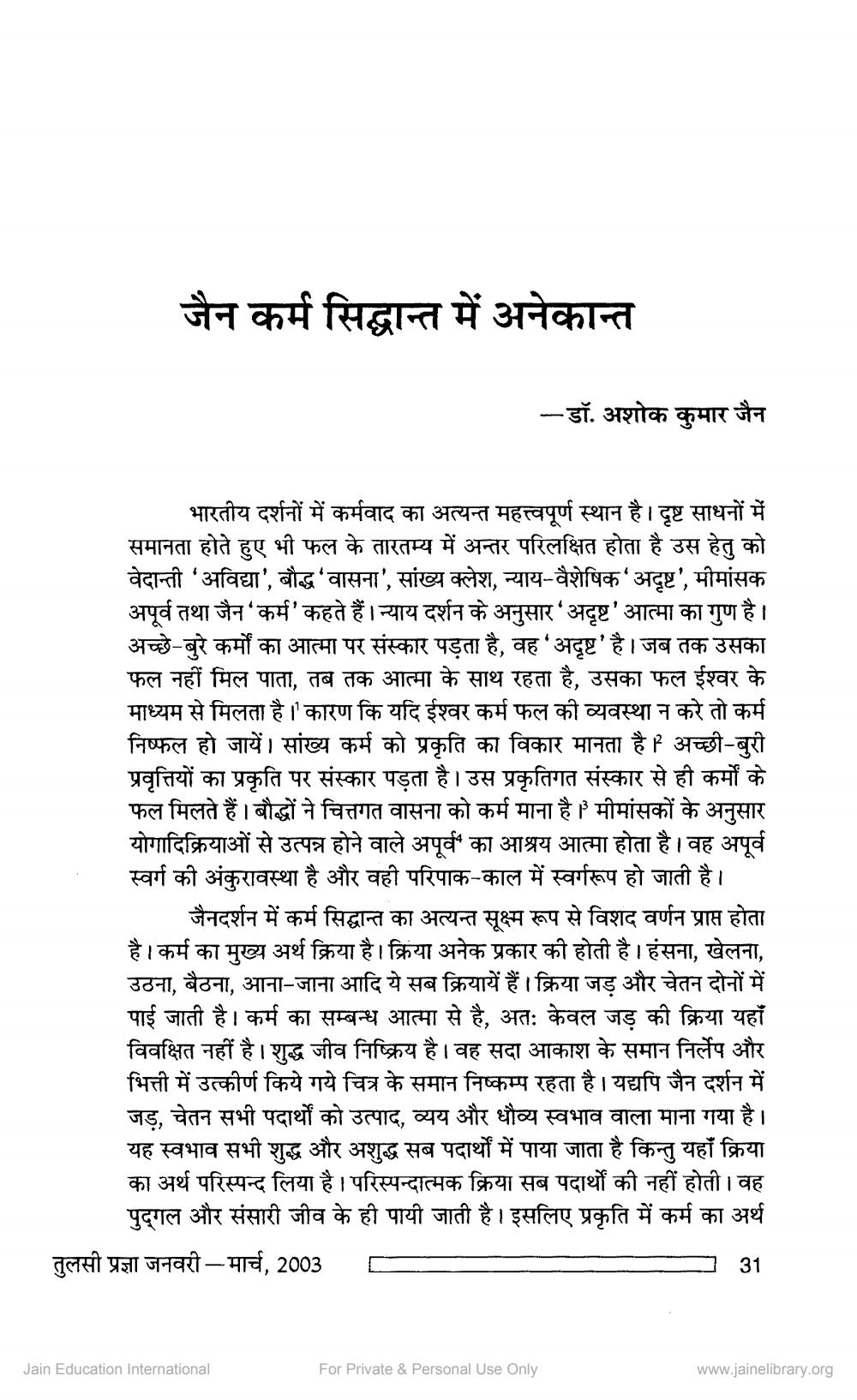________________
जैन कर्म सिद्धान्त में अनेकान्त
-डॉ. अशोक कुमार जैन
भारतीय दर्शनों में कर्मवाद का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। दृष्ट साधनों में समानता होते हुए भी फल के तारतम्य में अन्तर परिलक्षित होता है उस हेतु को वेदान्ती 'अविद्या', बौद्ध 'वासना', सांख्य क्लेश, न्याय-वैशेषिक 'अदृष्ट', मीमांसक अपूर्व तथा जैन 'कर्म' कहते हैं। न्याय दर्शन के अनुसार 'अदृष्ट' आत्मा का गुण है। अच्छे-बुरे कर्मों का आत्मा पर संस्कार पड़ता है, वह 'अदृष्ट' है। जब तक उसका फल नहीं मिल पाता, तब तक आत्मा के साथ रहता है, उसका फल ईश्वर के माध्यम से मिलता है। कारण कि यदि ईश्वर कर्म फल की व्यवस्था न करे तो कर्म निष्फल हो जायें। सांख्य कर्म को प्रकृति का विकार मानता है। अच्छी-बुरी प्रवृत्तियों का प्रकृति पर संस्कार पड़ता है। उस प्रकृतिगत संस्कार से ही कर्मों के फल मिलते हैं। बौद्धों ने चित्तगत वासना को कर्म माना है। मीमांसकों के अनुसार योगादिक्रियाओं से उत्पन्न होने वाले अपूर्व का आश्रय आत्मा होता है। वह अपूर्व स्वर्ग की अंकुरावस्था है और वही परिपाक-काल में स्वर्गरूप हो जाती है।
जैनदर्शन में कर्म सिद्धान्त का अत्यन्त सूक्ष्म रूप से विशद वर्णन प्राप्त होता है। कर्म का मुख्य अर्थ क्रिया है। क्रिया अनेक प्रकार की होती है। हंसना, खेलना, उठना, बैठना, आना-जाना आदि ये सब क्रियायें हैं। क्रिया जड़ और चेतन दोनों में पाई जाती है। कर्म का सम्बन्ध आत्मा से है, अत: केवल जड़ की क्रिया यहाँ विवक्षित नहीं है। शुद्ध जीव निष्क्रिय है। वह सदा आकाश के समान निर्लेप और भित्ती में उत्कीर्ण किये गये चित्र के समान निष्कम्प रहता है। यद्यपि जैन दर्शन में जड़, चेतन सभी पदार्थों को उत्पाद, व्यय और धौव्य स्वभाव वाला माना गया है। यह स्वभाव सभी शुद्ध और अशुद्ध सब पदार्थों में पाया जाता है किन्तु यहाँ क्रिया का अर्थ परिस्पन्द लिया है। परिस्पन्दात्मक क्रिया सब पदार्थों की नहीं होती। वह
पुद्गल और संसारी जीव के ही पायी जाती है। इसलिए प्रकृति में कर्म का अर्थ तुलसी प्रज्ञा जनवरी-मार्च, 2003
- 31
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org