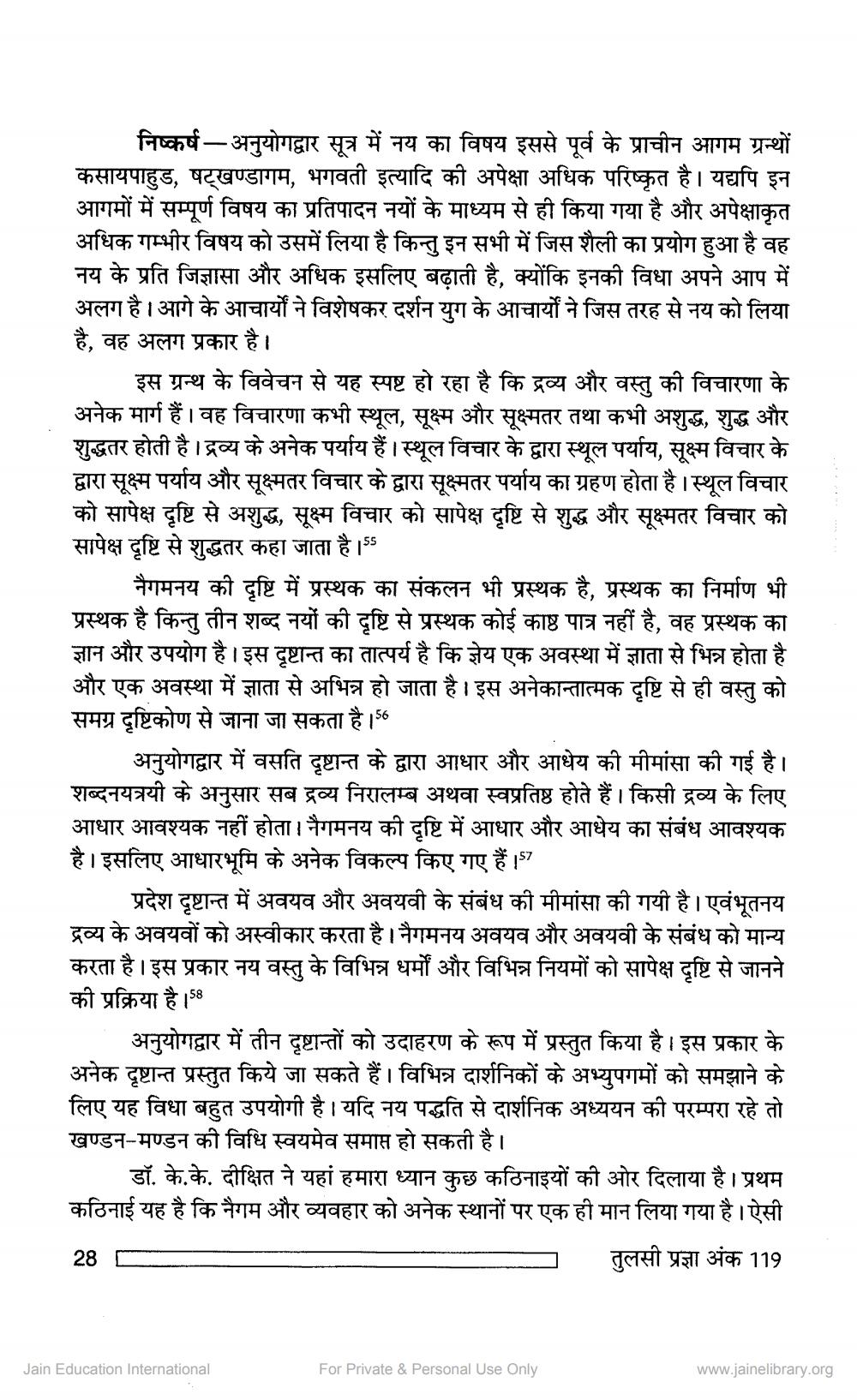________________
निष्कर्ष-अनुयोगद्वार सूत्र में नय का विषय इससे पूर्व के प्राचीन आगम ग्रन्थों कसायपाहुड, षट्खण्डागम, भगवती इत्यादि की अपेक्षा अधिक परिष्कृत है। यद्यपि इन आगमों में सम्पूर्ण विषय का प्रतिपादन नयों के माध्यम से ही किया गया है और अपेक्षाकृत अधिक गम्भीर विषय को उसमें लिया है किन्तु इन सभी में जिस शैली का प्रयोग हुआ है वह नय के प्रति जिज्ञासा और अधिक इसलिए बढ़ाती है, क्योंकि इनकी विधा अपने आप में अलग है। आगे के आचार्यों ने विशेषकर दर्शन युग के आचार्यों ने जिस तरह से नय को लिया है, वह अलग प्रकार है।
इस ग्रन्थ के विवेचन से यह स्पष्ट हो रहा है कि द्रव्य और वस्तु की विचारणा के अनेक मार्ग हैं। वह विचारणा कभी स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्मतर तथा कभी अशुद्ध, शुद्ध और शुद्धतर होती है। द्रव्य के अनेक पर्याय हैं । स्थूल विचार के द्वारा स्थूल पर्याय, सूक्ष्म विचार के द्वारा सूक्ष्म पर्याय और सूक्ष्मतर विचार के द्वारा सूक्ष्मतर पर्याय का ग्रहण होता है। स्थूल विचार को सापेक्ष दृष्टि से अशुद्ध, सूक्ष्म विचार को सापेक्ष दृष्टि से शुद्ध और सूक्ष्मतर विचार को सापेक्ष दृष्टि से शुद्धतर कहा जाता है। ___नैगमनय की दृष्टि में प्रस्थक का संकलन भी प्रस्थक है, प्रस्थक का निर्माण भी प्रस्थक है किन्तु तीन शब्द नयों की दृष्टि से प्रस्थक कोई काष्ठ पात्र नहीं है, वह प्रस्थक का ज्ञान और उपयोग है। इस दृष्टान्त का तात्पर्य है कि ज्ञेय एक अवस्था में ज्ञाता से भिन्न होता है और एक अवस्था में ज्ञाता से अभिन्न हो जाता है। इस अनेकान्तात्मक दृष्टि से ही वस्तु को समग्र दृष्टिकोण से जाना जा सकता है।
अनुयोगद्वार में वसति दृष्टान्त के द्वारा आधार और आधेय की मीमांसा की गई है। शब्दनयत्रयी के अनुसार सब द्रव्य निरालम्ब अथवा स्वप्रतिष्ठ होते हैं। किसी द्रव्य के लिए आधार आवश्यक नहीं होता। नैगमनय की दृष्टि में आधार और आधेय का संबंध आवश्यक है। इसलिए आधारभूमि के अनेक विकल्प किए गए हैं।"
प्रदेश दृष्टान्त में अवयव और अवयवी के संबंध की मीमांसा की गयी है। एवंभूतनय द्रव्य के अवयवों को अस्वीकार करता है। नैगमनय अवयव और अवयवी के संबंध को मान्य करता है। इस प्रकार नय वस्तु के विभिन्न धर्मों और विभिन्न नियमों को सापेक्ष दृष्टि से जानने की प्रक्रिया है।58 ___अनुयोगद्वार में तीन दृष्टान्तों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। इस प्रकार के अनेक दृष्टान्त प्रस्तुत किये जा सकते हैं। विभिन्न दार्शनिकों के अभ्युपगमों को समझाने के लिए यह विधा बहुत उपयोगी है। यदि नय पद्धति से दार्शनिक अध्ययन की परम्परा रहे तो खण्डन-मण्डन की विधि स्वयमेव समाप्त हो सकती है।
डॉ. के.के. दीक्षित ने यहां हमारा ध्यान कुछ कठिनाइयों की ओर दिलाया है। प्रथम कठिनाई यह है कि नैगम और व्यवहार को अनेक स्थानों पर एक ही मान लिया गया है। ऐसी 28 -
- तुलसी प्रज्ञा अंक 119
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org