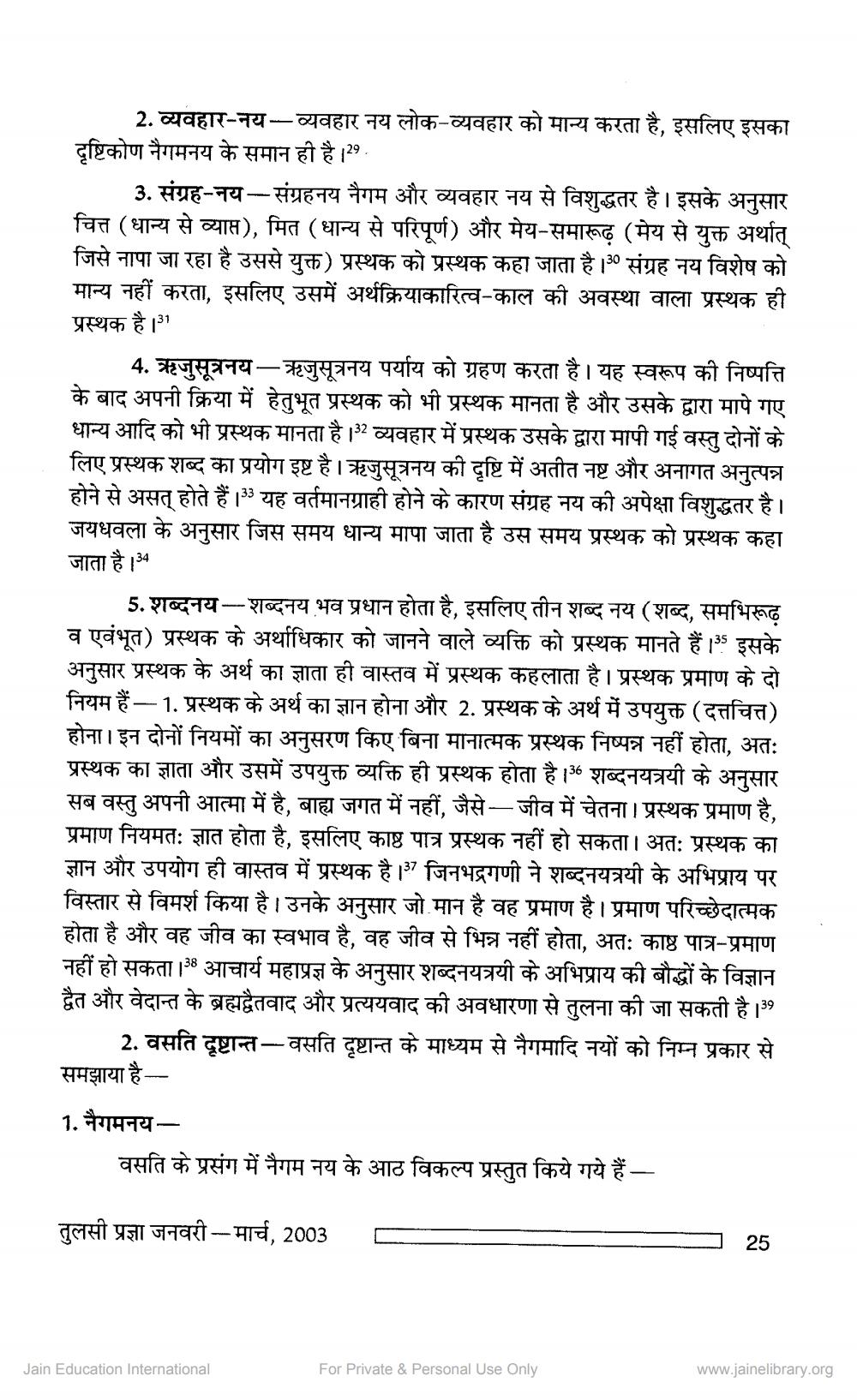________________
2. व्यवहार-नय-व्यवहार नय लोक-व्यवहार को मान्य करता है, इसलिए इसका दृष्टिकोण नैगमनय के समान ही है। .
3. संग्रह-नय-संग्रहनय नैगम और व्यवहार नय से विशुद्धतर है। इसके अनुसार चित्त (धान्य से व्याप्त), मित (धान्य से परिपूर्ण) और मेय-समारूढ़ (मेय से युक्त अर्थात् जिसे नापा जा रहा है उससे युक्त) प्रस्थक को प्रस्थक कहा जाता है। संग्रह नय विशेष को मान्य नहीं करता, इसलिए उसमें अर्थक्रियाकारित्व-काल की अवस्था वाला प्रस्थक ही प्रस्थक है।
___4. ऋजुसूत्रनय-ऋजुसूत्रनय पर्याय को ग्रहण करता है। यह स्वरूप की निष्पत्ति के बाद अपनी क्रिया में हेतुभूत प्रस्थक को भी प्रस्थक मानता है और उसके द्वारा मापे गए धान्य आदि को भी प्रस्थक मानता है। व्यवहार में प्रस्थक उसके द्वारा मापी गई वस्तु दोनों के लिए प्रस्थक शब्द का प्रयोग इष्ट है। ऋजुसूत्रनय की दृष्टि में अतीत नष्ट और अनागत अनुत्पन्न होने से असत् होते हैं। यह वर्तमानग्राही होने के कारण संग्रह नय की अपेक्षा विशुद्धतर है। जयधवला के अनुसार जिस समय धान्य मापा जाता है उस समय प्रस्थक को प्रस्थक कहा जाता है।34
5.शब्दनय-शब्दनय भव प्रधान होता है, इसलिए तीन शब्द नय (शब्द, समभिरूढ़ व एवंभूत) प्रस्थक के अर्थाधिकार को जानने वाले व्यक्ति को प्रस्थक मानते हैं। इसके अनुसार प्रस्थक के अर्थ का ज्ञाता ही वास्तव में प्रस्थक कहलाता है। प्रस्थक प्रमाण के दो नियम हैं - 1. प्रस्थक के अर्थ का ज्ञान होना और 2. प्रस्थक के अर्थ में उपयुक्त (दत्तचित्त) होना। इन दोनों नियमों का अनुसरण किए बिना मानात्मक प्रस्थक निष्पन्न नहीं होता, अत: प्रस्थक का ज्ञाता और उसमें उपयुक्त व्यक्ति ही प्रस्थक होता है। शब्दनयत्रयी के अनुसार सब वस्तु अपनी आत्मा में है, बाह्य जगत में नहीं, जैसे- जीव में चेतना। प्रस्थक प्रमाण है, प्रमाण नियमतः ज्ञात होता है, इसलिए काष्ठ पात्र प्रस्थक नहीं हो सकता। अतः प्रस्थक का ज्ञान और उपयोग ही वास्तव में प्रस्थक है। जिनभद्रगणी ने शब्दनयत्रयी के अभिप्राय पर विस्तार से विमर्श किया है। उनके अनुसार जो मान है वह प्रमाण है। प्रमाण परिच्छेदात्मक होता है और वह जीव का स्वभाव है, वह जीव से भिन्न नहीं होता, अतः काष्ठ पात्र-प्रमाण नहीं हो सकता। आचार्य महाप्रज्ञ के अनुसार शब्दनयत्रयी के अभिप्राय की बौद्धों के विज्ञान द्वैत और वेदान्त के ब्रह्मद्वैतवाद और प्रत्ययवाद की अवधारणा से तुलना की जा सकती है।
2. वसति दृष्टान्त-वसति दृष्टान्त के माध्यम से नैगमादि नयों को निम्न प्रकार से समझाया है1. नैगमनय
वसति के प्रसंग में नैगम नय के आठ विकल्प प्रस्तुत किये गये हैं -
तुलसी प्रज्ञा जनवरी-मार्च, 2003
- 25
For Private & Personal Use Only
Jain Education International
www.jainelibrary.org