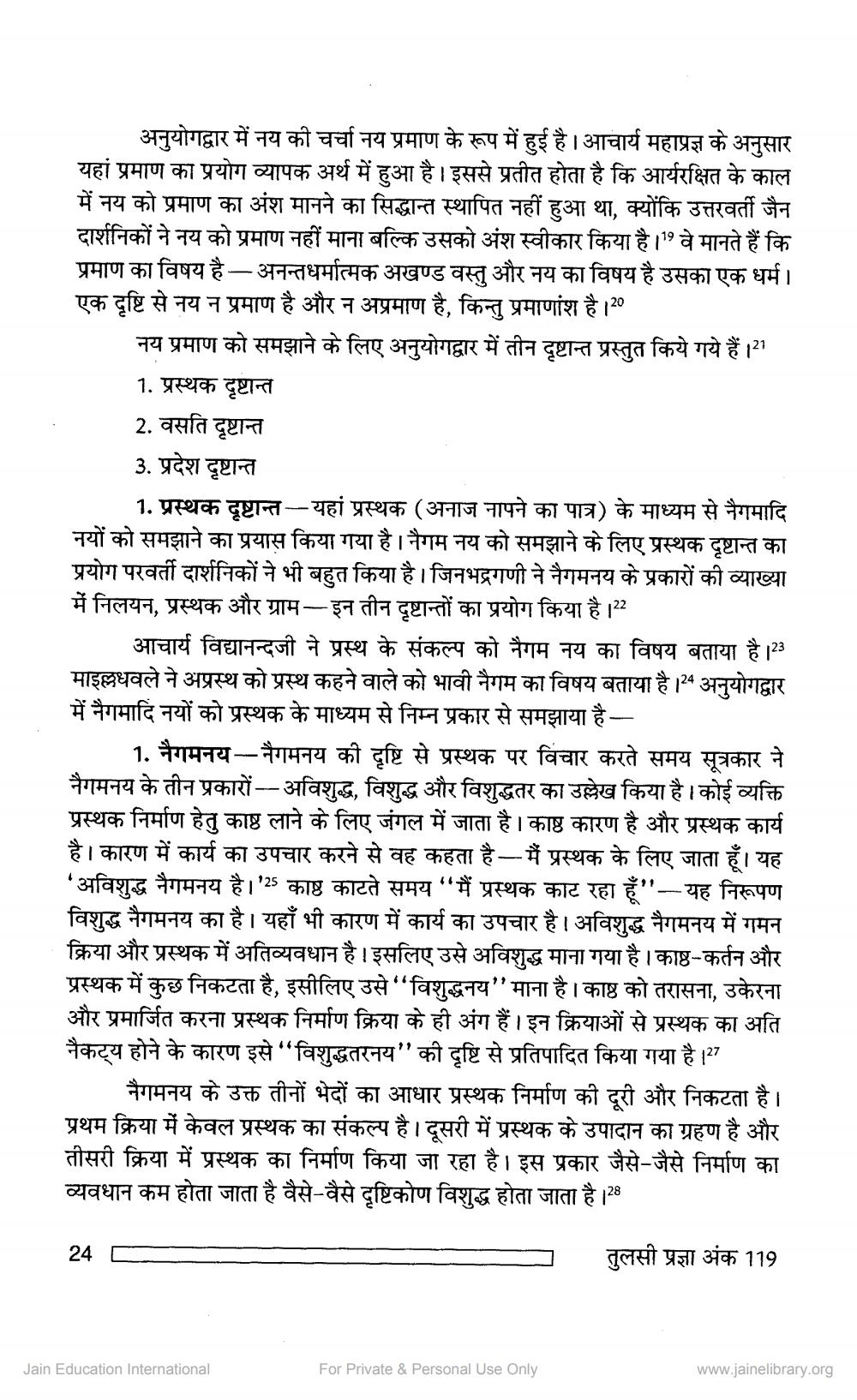________________
अनुयोगद्वार में नय की चर्चा नय प्रमाण के रूप में हुई है। आचार्य महाप्रज्ञ के अनुसार यहां प्रमाण का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है। इससे प्रतीत होता है कि आर्यरक्षित के काल में नय को प्रमाण का अंश मानने का सिद्धान्त स्थापित नहीं हुआ था, क्योंकि उत्तरवर्ती जैन दार्शनिकों ने नय को प्रमाण नहीं माना बल्कि उसको अंश स्वीकार किया है।" वे मानते हैं कि प्रमाण का विषय है - अनन्तधर्मात्मक अखण्ड वस्तु और नय का विषय है उसका एक धर्म । एक दृष्टि से नयन प्रमाण है और न अप्रमाण है, किन्तु प्रमाणांश है | 20
1
नय प्रमाण को समझाने के लिए अनुयोगद्वार में तीन दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये हैं 121
1. प्रस्थक दृष्टान्त
2. वसति दृष्टान्त
3. प्रदेश दृष्टान्त
1. प्रस्थक दृष्टान्त - यहां प्रस्थक (अनाज नापने का पात्र) के माध्यम से नैगमादि नयों को समझाने का प्रयास किया गया है। नैगम नय को समझाने के लिए प्रस्थक दृष्टान्त का प्रयोग परवर्ती दार्शनिकों ने भी बहुत किया है। जिनभद्रगणी ने नैगमनय के प्रकारों की व्याख्या में निलयन, प्रस्थक और ग्राम- -इन तीन दृष्टान्तों का प्रयोग किया है। 22
आचार्य विद्यानन्दजी ने प्रस्थ के संकल्प को नैगम नय का विषय बताया है। 23 माइल्लधवले ने अप्रस्थ को प्रस्थ कहने वाले को भावी नैगम का विषय बताया है। 24 अनुयोगद्वार में नैगमादि नयों को प्रस्थक के माध्यम से निम्न प्रकार से समझाया है
1. नैगमनय – नैगमनय की दृष्टि से प्रस्थक पर विचार करते समय सूत्रकार ने नैगमनय के तीन प्रकारों - अविशुद्ध, विशुद्ध और विशुद्धतर का उल्लेख किया है। कोई व्यक्ति प्रस्थक निर्माण हेतु काष्ठ लाने के लिए जंगल में जाता है। काष्ठ कारण है और प्रस्थक कार्य
। कारण में कार्य का उपचार करने से वह कहता है – मैं प्रस्थक के लिए जाता हूँ। यह 'अविशुद्ध नैगमनय है । '25 काष्ठ काटते समय "मैं प्रस्थक काट रहा हूँ" - यह निरूपण विशुद्ध नैगमन का है। यहाँ भी कारण में कार्य का उपचार है। अविशुद्ध नैगमनय में गमन क्रिया और प्रस्थक में अतिव्यवधान है। इसलिए उसे अविशुद्ध माना गया है। काष्ठ-कर्तन और प्रस्थक में कुछ निकटता है, इसीलिए उसे "विशुद्धनय" माना है। काष्ठ को तरासना, उकेरना और प्रमार्जित करना प्रस्थक निर्माण क्रिया के ही अंग हैं। इन क्रियाओं से प्रस्थक का अति नैकट्य होने के कारण इसे "विशुद्धतरनय" की दृष्टि से प्रतिपादित किया गया है। 27
नैगमनय के उक्त तीनों भेदों का आधार प्रस्थक निर्माण की दूरी और निकटता है । प्रथम क्रिया में केवल प्रस्थक का संकल्प है। दूसरी में प्रस्थक के उपादान का ग्रहण है और तीसरी क्रिया में प्रस्थक का निर्माण किया जा रहा है। इस प्रकार जैसे-जैसे निर्माण का व्यवधान कम होता जाता है वैसे-वैसे दृष्टिकोण विशुद्ध होता जाता है। 28
तुलसी प्रज्ञा अंक 119
24
-
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org