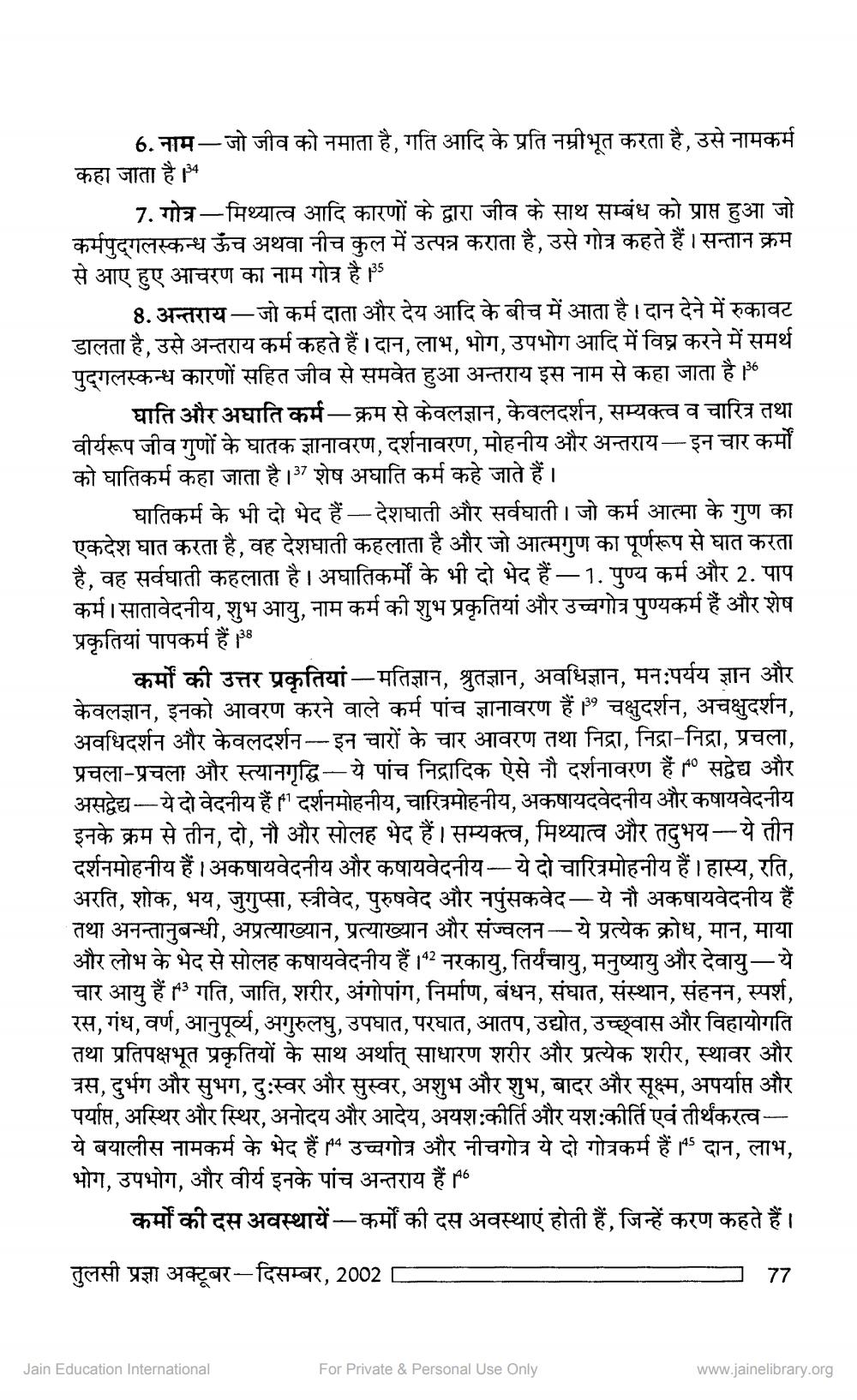________________
6. नाम- जो जीव को नमाता है, गति आदि के प्रति नम्रीभूत करता है, उसे नामकर्म कहा जाता है।
7. गोत्र-मिथ्यात्व आदि कारणों के द्वारा जीव के साथ सम्बंध को प्राप्त हुआ जो कर्मपुद्गलस्कन्ध ऊँच अथवा नीच कुल में उत्पन्न कराता है, उसे गोत्र कहते हैं । सन्तान क्रम से आए हुए आचरण का नाम गोत्र है।
8. अन्तराय-जो कर्म दाता और देय आदि के बीच में आता है। दान देने में रुकावट डालता है, उसे अन्तराय कर्म कहते हैं। दान, लाभ, भोग, उपभोग आदि में विघ्न करने में समर्थ पुद्गलस्कन्ध कारणों सहित जीव से समवेत हुआ अन्तराय इस नाम से कहा जाता है।
घाति और अघाति कर्म-क्रम से केवलज्ञान, केवलदर्शन, सम्यक्त्व व चारित्र तथा वीर्यरूप जीव गुणों के घातक ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अन्तराय- इन चार कर्मों को घातिकर्म कहा जाता है। शेष अघाति कर्म कहे जाते हैं।
घातिकर्म के भी दो भेद हैं - देशघाती और सर्वघाती। जो कर्म आत्मा के गुण का एकदेश घात करता है, वह देशघाती कहलाता है और जो आत्मगुण का पूर्णरूप से घात करता है, वह सर्वघाती कहलाता है। अघातिकर्मों के भी दो भेद हैं - 1. पुण्य कर्म और 2. पाप कर्म। सातावेदनीय, शुभ आयु, नाम कर्म की शुभ प्रकृतियां और उच्चगोत्र पुण्यकर्म हैं और शेष प्रकृतियां पापकर्म हैं।
कर्मों की उत्तर प्रकृतियां-मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवलज्ञान, इनको आवरण करने वाले कर्म पांच ज्ञानावरण हैं।” चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन, अवधिदर्शन और केवलदर्शन - इन चारों के चार आवरण तथा निद्रा, निद्रा-निद्रा, प्रचला, प्रचला-प्रचला और स्त्यानगृद्धि– ये पांच निद्रादिक ऐसे नौ दर्शनावरण हैं। सद्वेद्य और असद्वेद्य-ये दो वेदनीय हैं।" दर्शनमोहनीय, चारित्रमोहनीय, अकषायदवेदनीय और कषायवेदनीय इनके क्रम से तीन, दो, नौ और सोलह भेद हैं। सम्यक्त्व, मिथ्यात्व और तदुभय-ये तीन दर्शनमोहनीय हैं। अकषायवेदनीय और कषायवेदनीय- ये दो चारित्रमोहनीय हैं। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद-ये नौ अकषायवेदनीय हैं तथा अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन-ये प्रत्येक क्रोध, मान, माया
और लोभ के भेद से सोलह कषायवेदनीय हैं। नरकायु, तिर्यंचायु, मनुष्यायु और देवायु-ये चार आयु हैं। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, संहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, आनुपूर्व्य, अगुरुलघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास और विहायोगति तथा प्रतिपक्षभूत प्रकृतियों के साथ अर्थात् साधारण शरीर और प्रत्येक शरीर, स्थावर और त्रस, दुर्भग और सुभग, दुःस्वर और सुस्वर, अशुभ और शुभ, बादर और सूक्ष्म, अपर्याप्त और पर्याप्त, अस्थिर और स्थिर, अनोदय और आदेय, अयश:कीर्ति और यश:कीर्ति एवं तीर्थंकरत्वये बयालीस नामकर्म के भेद हैं। उच्चगोत्र और नीचगोत्र ये दो गोत्रकर्म हैं। दान, लाभ, भोग, उपभोग, और वीर्य इनके पांच अन्तराय हैं।
कर्मों की दस अवस्थायें-कर्मों की दस अवस्थाएं होती हैं, जिन्हें करण कहते हैं।
तुलसी प्रज्ञा अक्टूबर-दिसम्बर, 2002 0
-
77
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org