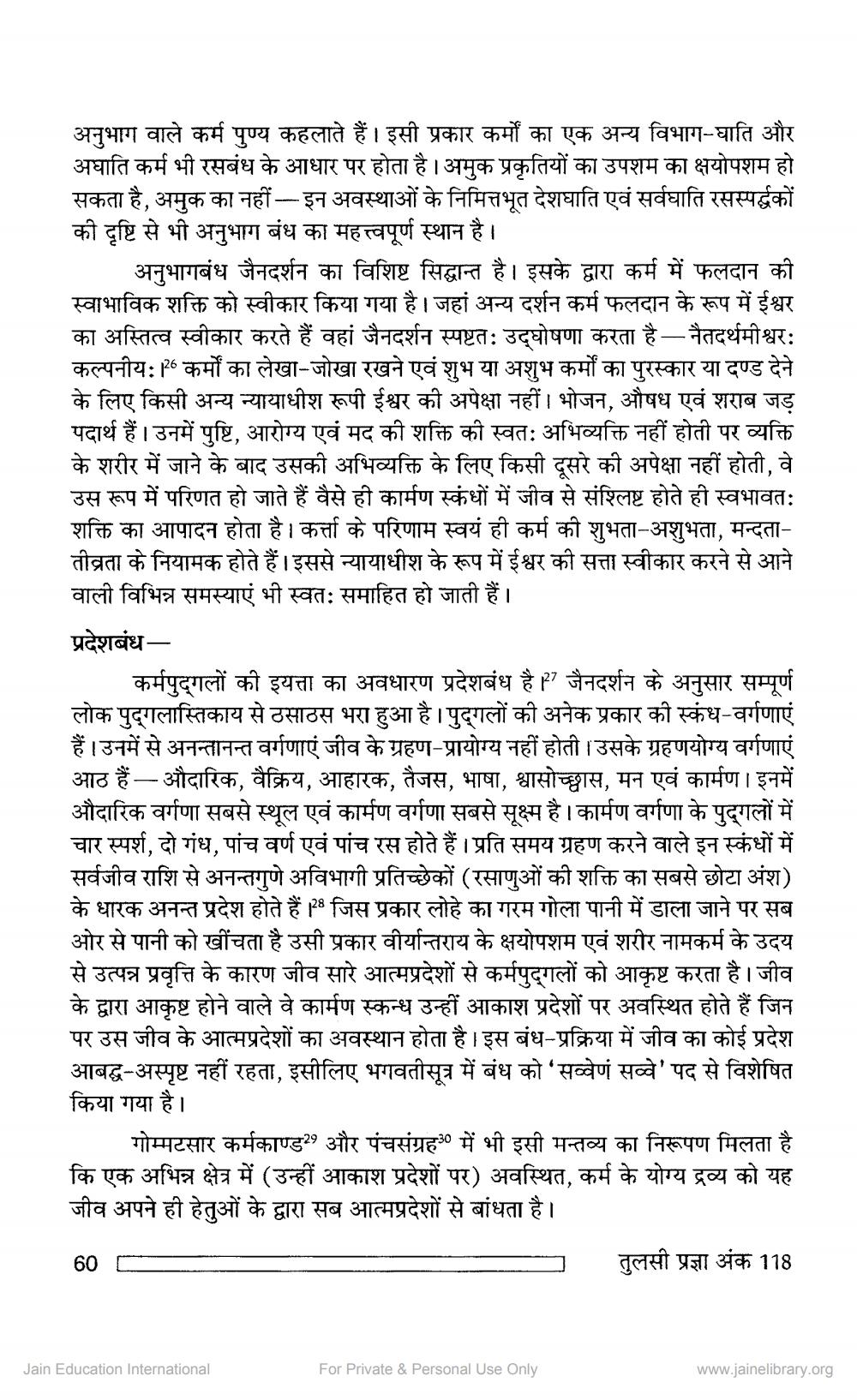________________
अनुभाग वाले कर्म पुण्य कहलाते हैं। इसी प्रकार कर्मों का एक अन्य विभाग-घाति और अघाति कर्म भी रसबंध के आधार पर होता है। अमुक प्रकृतियों का उपशम का क्षयोपशम हो सकता है, अमुक का नहीं- इन अवस्थाओं के निमित्तभूत देशघाति एवं सर्वघाति रसस्पर्द्धकों की दृष्टि से भी अनुभाग बंध का महत्त्वपूर्ण स्थान है।
अनुभागबंध जैनदर्शन का विशिष्ट सिद्धान्त है। इसके द्वारा कर्म में फलदान की स्वाभाविक शक्ति को स्वीकार किया गया है। जहां अन्य दर्शन कर्म फलदान के रूप में ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार करते हैं वहां जैनदर्शन स्पष्टत: उद्घोषणा करता है— नैतदर्थमीश्वरः कल्पनीयः। कर्मों का लेखा-जोखा रखने एवं शुभ या अशुभ कर्मों का पुरस्कार या दण्ड देने के लिए किसी अन्य न्यायाधीश रूपी ईश्वर की अपेक्षा नहीं। भोजन, औषध एवं शराब जड़ पदार्थ हैं। उनमें पुष्टि, आरोग्य एवं मद की शक्ति की स्वतः अभिव्यक्ति नहीं होती पर व्यक्ति के शरीर में जाने के बाद उसकी अभिव्यक्ति के लिए किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं होती, वे उस रूप में परिणत हो जाते हैं वैसे ही कार्मण स्कंधों में जीव से संश्लिष्ट होते ही स्वभावतः शक्ति का आपादन होता है। कर्ता के परिणाम स्वयं ही कर्म की शुभता-अशुभता, मन्दतातीव्रता के नियामक होते हैं। इससे न्यायाधीश के रूप में ईश्वर की सत्ता स्वीकार करने से आने वाली विभिन्न समस्याएं भी स्वतः समाहित हो जाती हैं। प्रदेशबंध
कर्मपुद्गलों की इयत्ता का अवधारण प्रदेशबंध है? जैनदर्शन के अनुसार सम्पूर्ण लोक पुद्गलास्तिकाय से ठसाठस भरा हुआ है। पुद्गलों की अनेक प्रकार की स्कंध-वर्गणाएं हैं। उनमें से अनन्तानन्त वर्गणाएं जीव के ग्रहण-प्रायोग्य नहीं होती। उसके ग्रहणयोग्य वर्गणाएं आठ हैं - औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तैजस, भाषा, श्वासोच्छ्वास, मन एवं कार्मण। इनमें औदारिक वर्गणा सबसे स्थूल एवं कार्मण वर्गणा सबसे सूक्ष्म है। कार्मण वर्गणा के पुद्गलों में चार स्पर्श, दो गंध, पांच वर्ण एवं पांच रस होते हैं । प्रति समय ग्रहण करने वाले इन स्कंधों में सर्वजीव राशि से अनन्तगुणे अविभागी प्रतिच्छेकों (रसाणुओं की शक्ति का सबसे छोटा अंश) के धारक अनन्त प्रदेश होते हैं। जिस प्रकार लोहे का गरम गोला पानी में डाला जाने पर सब ओर से पानी को खींचता है उसी प्रकार वीर्यान्तराय के क्षयोपशम एवं शरीर नामकर्म के उदय से उत्पन्न प्रवृत्ति के कारण जीव सारे आत्मप्रदेशों से कर्मपुद्गलों को आकृष्ट करता है। जीव के द्वारा आकृष्ट होने वाले वे कार्मण स्कन्ध उन्हीं आकाश प्रदेशों पर अवस्थित होते हैं जिन पर उस जीव के आत्मप्रदेशों का अवस्थान होता है। इस बंध-प्रक्रिया में जीव का कोई प्रदेश आबद्ध-अस्पृष्ट नहीं रहता, इसीलिए भगवतीसूत्र में बंध को 'सव्वेणं सव्वे' पद से विशेषित किया गया है।
गोम्मटसार कर्मकाण्ड और पंचसंग्रह में भी इसी मन्तव्य का निरूपण मिलता है कि एक अभिन्न क्षेत्र में (उन्हीं आकाश प्रदेशों पर) अवस्थित, कर्म के योग्य द्रव्य को यह जीव अपने ही हेतुओं के द्वारा सब आत्मप्रदेशों से बांधता है।
- तुलसी प्रज्ञा अंक 118
60
-
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org