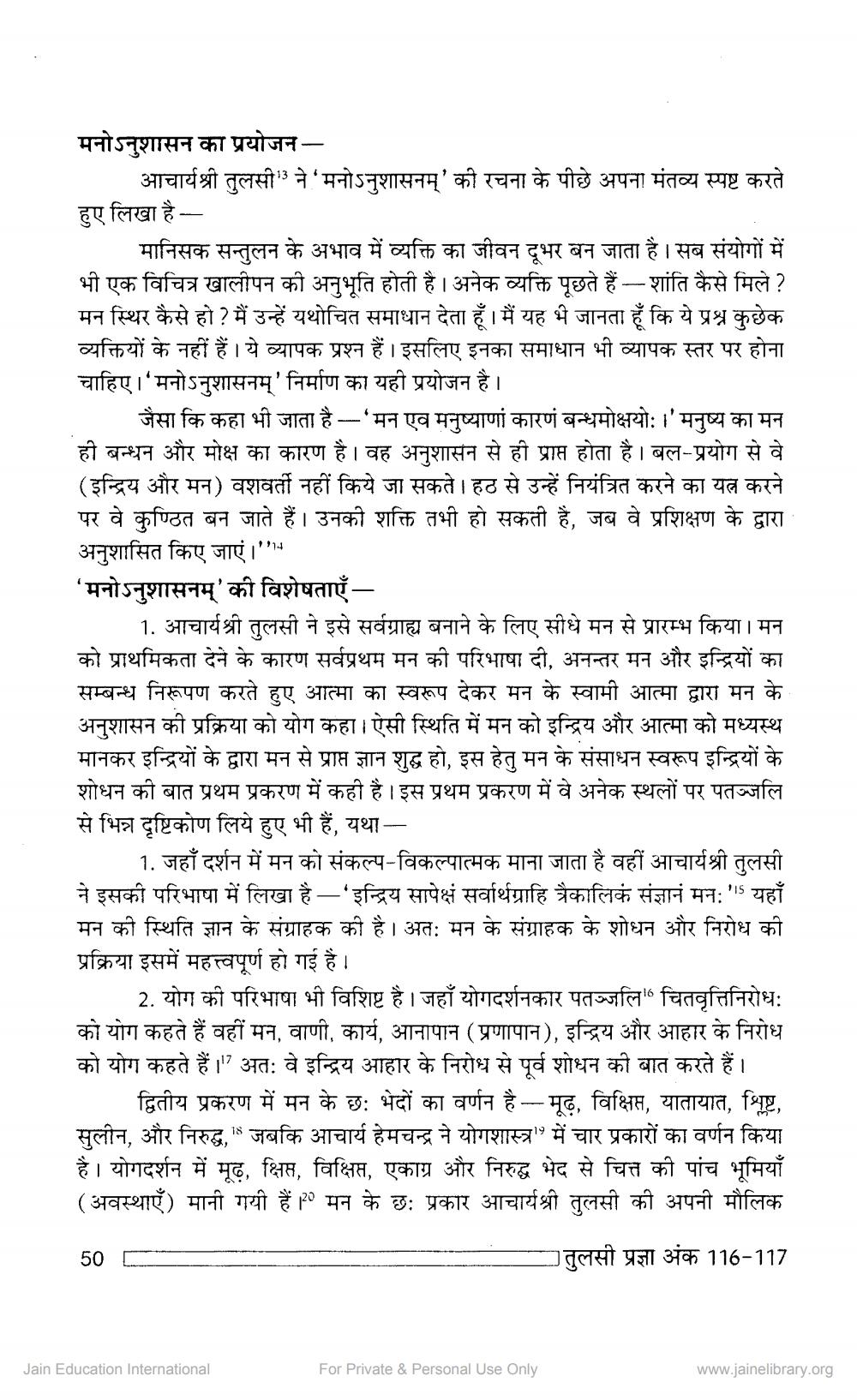________________
मनोऽनुशासन का प्रयोजन
आचार्यश्री तुलसी' ने 'मनोऽनुशासनम्' की रचना के पीछे अपना मंतव्य स्पष्ट करते हुए लिखा है -
मानिसक सन्तुलन के अभाव में व्यक्ति का जीवन दूभर बन जाता है । सब संयोगों में भी एक विचित्र खालीपन की अनुभूति होती है। अनेक व्यक्ति पूछते हैं - शांति कैसे मिले? मन स्थिर कैसे हो? मैं उन्हें यथोचित समाधान देता हूँ। मैं यह भ जानता हूँ कि ये प्रश्र कुछेक व्यक्तियों के नहीं हैं। ये व्यापक प्रश्न हैं। इसलिए इनका समाधान भी व्यापक स्तर पर होना चाहिए । 'मनोऽनुशासनम्' निर्माण का यही प्रयोजन है।
___ जैसा कि कहा भी जाता है - 'मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।' मनुष्य का मन ही बन्धन और मोक्ष का कारण है। वह अनुशासन से ही प्राप्त होता है। बल-प्रयोग से वे (इन्द्रिय और मन) वशवर्ती नहीं किये जा सकते। हठ से उन्हें नियंत्रित करने का यत्न करने पर वे कुण्ठित बन जाते हैं। उनकी शक्ति तभी हो सकती है, जब वे प्रशिक्षण के द्वारा अनुशासित किए जाएं।'' 'मनोऽनुशासनम्' की विशेषताएँ
1. आचार्य श्री तुलसी ने इसे सर्वग्राह्य बनाने के लिए सीधे मन से प्रारम्भ किया। मन को प्राथमिकता देने के कारण सर्वप्रथम मन की परिभाषा दी, अनन्तर मन और इन्द्रियों का सम्बन्ध निरूपण करते हुए आत्मा का स्वरूप देकर मन के स्वामी आत्मा द्वारा मन के अनुशासन की प्रक्रिया को योग कहा। ऐसी स्थिति में मन को इन्द्रिय और आत्मा को मध्यस्थ मानकर इन्द्रियों के द्वारा मन से प्राप्त ज्ञान शुद्ध हो, इस हेतु मन के संसाधन स्वरूप इन्द्रियों के शोधन की बात प्रथम प्रकरण में कही है। इस प्रथम प्रकरण में वे अनेक स्थलों पर पतञ्जलि से भिन्न दृष्टिकोण लिये हुए भी हैं, यथा
1. जहाँ दर्शन में मन को संकल्प-विकल्पात्मक माना जाता है वहीं आचार्यश्री तुलसी ने इसकी परिभाषा में लिखा है - 'इन्द्रिय सापेक्षं सर्वार्थग्राहि त्रैकालिकं संज्ञानं मनः'। यहाँ मन की स्थिति ज्ञान के संग्राहक की है। अतः मन के संग्राहक के शोधन और निरोध की प्रक्रिया इसमें महत्त्वपूर्ण हो गई है।
2. योग की परिभाषा भी विशिष्ट है। जहाँ योगदर्शनकार पतञ्जलि चितवृत्तिनिरोधः को योग कहते हैं वहीं मन, वाणी, कार्य, आनापान (प्रणापान), इन्द्रिय और आहार के निरोध को योग कहते हैं।” अत: वे इन्द्रिय आहार के निरोध से पूर्व शोधन की बात करते हैं।
द्वितीय प्रकरण में मन के छः भेदों का वर्णन है-मूढ़, विक्षिप्त, यातायात, शिष्ट, सुलीन, और निरुद्ध, जबकि आचार्य हेमचन्द्र ने योगशास्त्र में चार प्रकारों का वर्णन किया है। योगदर्शन में मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध भेद से चित्त की पांच भूमियाँ (अवस्थाएँ) मानी गयी हैं। मन के छः प्रकार आचार्यश्री तुलसी की अपनी मौलिक
50
तुलसी प्रज्ञा अंक 116-117
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org