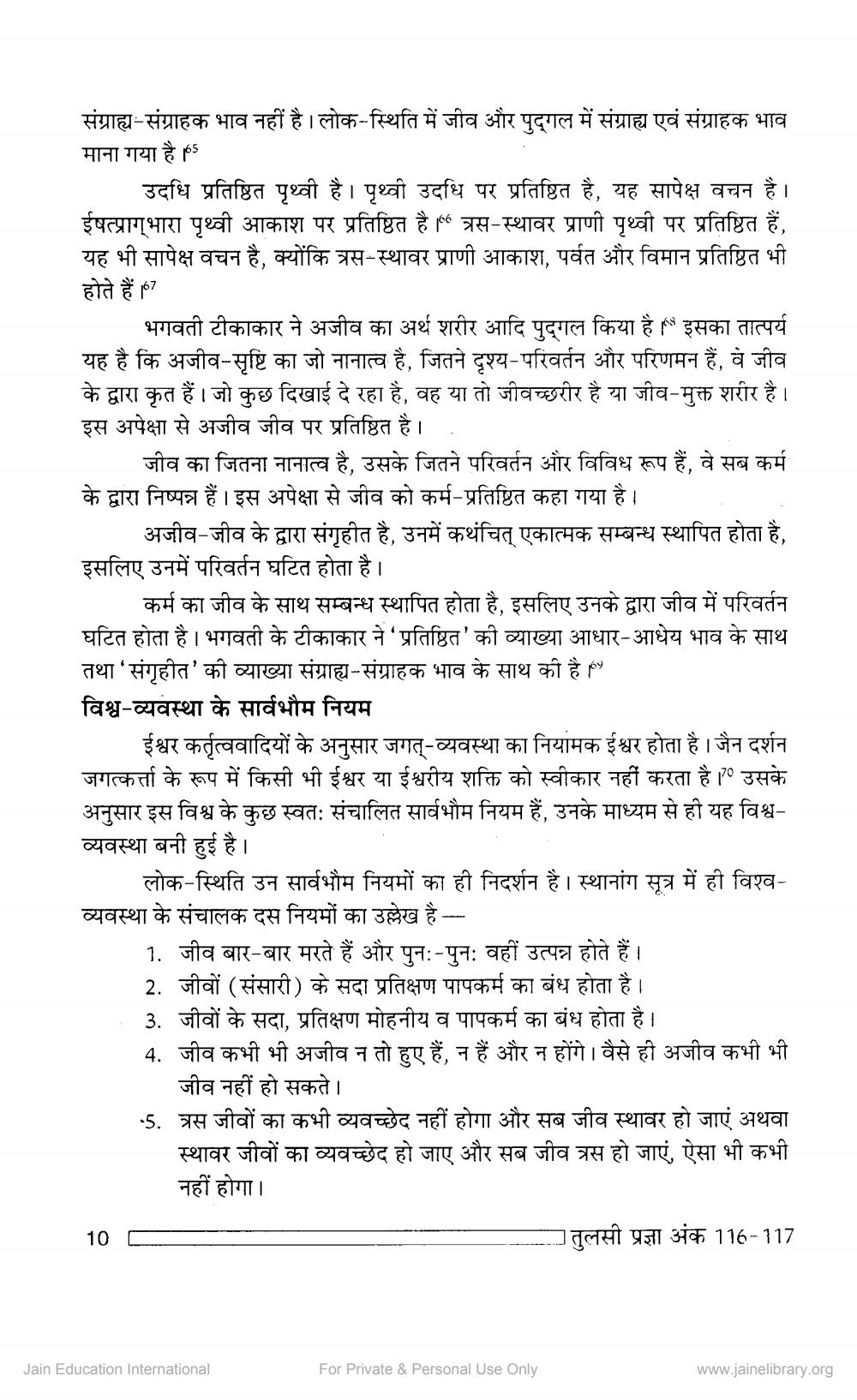________________
संग्राह्य-संग्राहक भाव नहीं है। लोक-स्थिति में जीव और पुद्गल में संग्राह्य एवं संग्राहक भाव माना गया है 65
उदधि प्रतिष्ठित पृथ्वी है। पृथ्वी उदधि पर प्रतिष्ठित है, यह सापेक्ष वचन है। ईषत्प्राग्भारा पृथ्वी आकाश पर प्रतिष्ठित है ।" त्रस - स्थावर प्राणी पृथ्वी पर प्रतिष्ठित हैं, यह भी सापेक्ष वचन है, क्योंकि त्रस - स्थावर प्राणी आकाश, पर्वत और विमान प्रतिष्ठित भी होते हैं 17
भगवती टीकाकार ने अजीव का अर्थ शरीर आदि पुद्गल किया है। इसका तात्पर्य यह है कि अजीव सृष्टि का जो नानात्व है, जितने दृश्य परिवर्तन और परिणमन हैं, वे जीव द्वारा कृत हैं। जो कुछ दिखाई दे रहा है, वह या तो जीवच्छरीर है या जीव- मुक्त शरीर है। इस अपेक्षा से अजीव जीव पर प्रतिष्ठित है ।
जीव का जितना नानात्व है, उसके जितने परिवर्तन और विविध रूप हैं, वे सब कर्म के द्वारा निष्पन्न हैं । इस अपेक्षा से जीव को कर्म-प्रतिष्ठित कहा गया है 4
अजीव-जीव के द्वारा संगृहीत है, उनमें कथंचित् एकात्मक सम्बन्ध स्थापित होता है, इसलिए उनमें परिवर्तन घटित होता है ।
कर्म का जीव के साथ सम्बन्ध स्थापित होता है, इसलिए उनके द्वारा जीव में परिवर्तन घटित होता है । भगवती के टीकाकार ने 'प्रतिष्ठित' की व्याख्या आधार-आधेय भाव के साथ तथा 'संगृहीत' की व्याख्या संग्राह्य-संग्राहक भाव के साथ की है। विश्व व्यवस्था के सार्वभौम नियम
ईश्वर कर्तृत्ववादियों के अनुसार जगत्-व्यवस्था का नियामक ईश्वर होता है। जैन दर्शन जगत्कर्त्ता के रूप में किसी भी ईश्वर या ईश्वरीय शक्ति को स्वीकार नहीं करता है ।° उसके अनुसार इस विश्व के कुछ स्वतः संचालित सार्वभौम नियम हैं, उनके माध्यम से ही यह विश्वव्यवस्था बनी हुई है ।
लोक-स्थिति उन सार्वभौम नियमों का ही निदर्शन है। स्थानांग सूत्र में ही विश्वव्यवस्था के संचालक दस नियमों का उल्लेख है.
10
1. जीव बार-बार मरते हैं और पुनः पुनः वहीं उत्पन्न होते हैं ।
2. जीवों (संसारी) के सदा प्रतिक्षण पापकर्म का बंध होता है ।
3. जीवों के सदा, प्रतिक्षण मोहनीय व पापकर्म का बंध होता है ।
4. जीव कभी भी अजीव न तो हुए हैं, न हैं और न होंगे। वैसे ही अजीव कभी भी जीव नहीं हो सकते ।
• 5. त्रस जीवों का कभी व्यवच्छेद नहीं होगा और सब जीव स्थावर हो जाएं अथवा स्थावर जीवों का व्यवच्छेद हो जाए और सब जीव त्रस हो जाएं, ऐसा भी कभी नहीं होगा ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
1 तुलसी प्रज्ञा अंक 116 117
www.jainelibrary.org