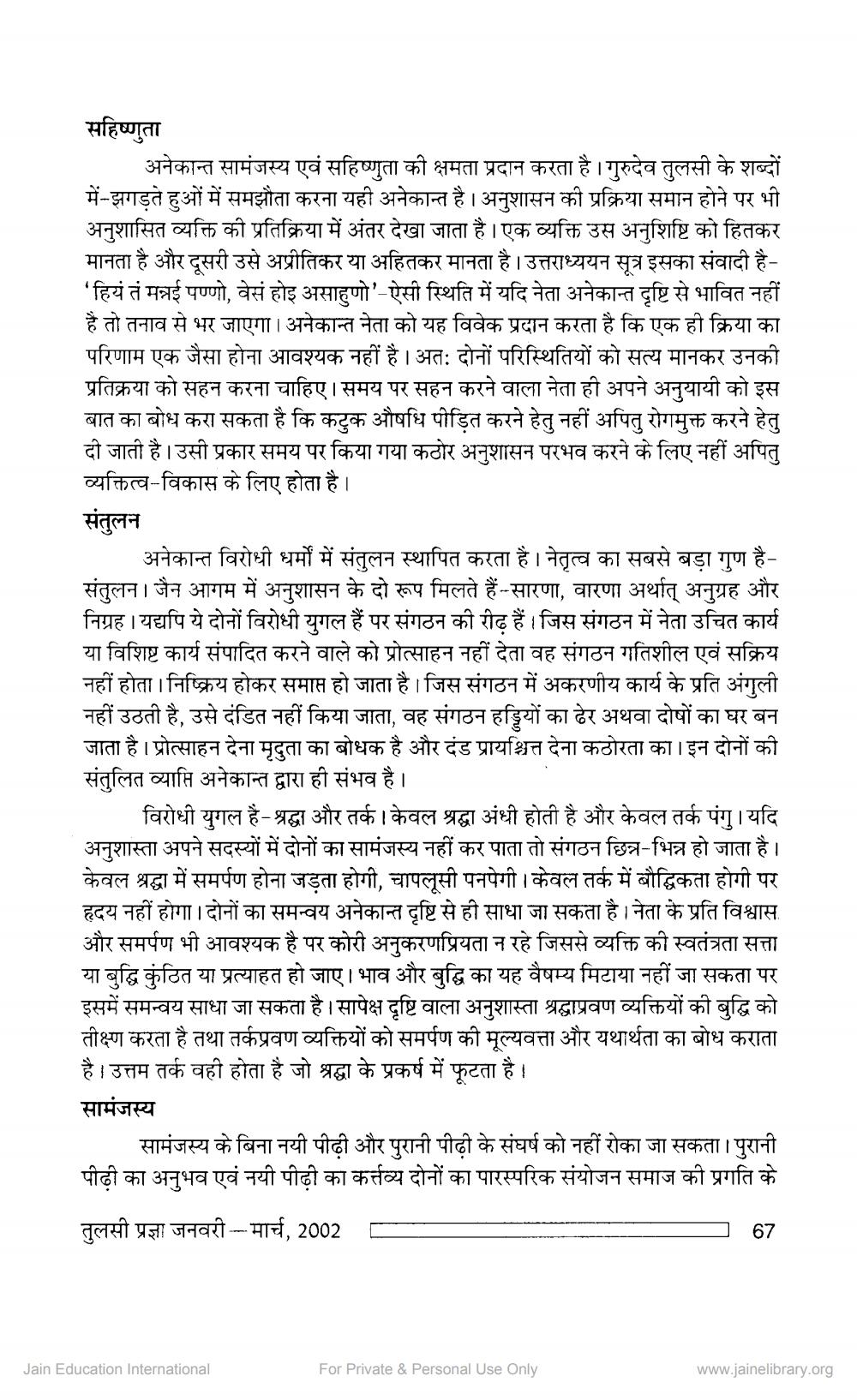________________
सहिष्णुता
अनेकान्त सामंजस्य एवं सहिष्णुता की क्षमता प्रदान करता है। गुरुदेव तुलसी के शब्दों में-झगड़ते हुओं में समझौता करना यही अनेकान्त है। अनुशासन की प्रक्रिया समान होने पर भी अनुशासित व्यक्ति की प्रतिक्रिया में अंतर देखा जाता है। एक व्यक्ति उस अनुशिष्टि को हितकर मानता है और दूसरी उसे अप्रीतिकर या अहितकर मानता है । उत्तराध्ययन सूत्र इसका संवादी है'हियं तं मन्नई पण्णो, वेसं होइ असाहुणो' ऐसी स्थिति में यदि नेता अनेकान्त दृष्टि से भावित नहीं है तो तनाव से भर जाएगा। अनेकान्त नेता को यह विवेक प्रदान करता है कि एक ही क्रिया का परिणाम एक जैसा होना आवश्यक नहीं है । अतः दोनों परिस्थितियों को सत्य मानकर उनकी प्रतिक्रया को सहन करना चाहिए। समय पर सहन करने वाला नेता ही अपने अनुयायी को इस बात का बोध करा सकता है कि कटुक औषधि पीड़ित करने हेतु नहीं अपितु रोगमुक्त करने हेतु जाती है । उसी प्रकार समय पर किया गया कठोर अनुशासन परभव करने के लिए नहीं अपितु व्यक्तित्व विकास के लिए होता है ।
संतुलन
अनेकान्त विरोधी धर्मों में संतुलन स्थापित करता है। नेतृत्व का सबसे बड़ा गुण हैसंतुलन। जैन आगम में अनुशासन के दो रूप मिलते हैं--सारणा, वारणा अर्थात् अनुग्रह और निग्रह । यद्यपि ये दोनों विरोधी युगल हैं पर संगठन की रीढ़ हैं। जिस संगठन में नेता उचित कार्य या विशिष्ट कार्य संपादित करने वाले को प्रोत्साहन नहीं देता वह संगठन गतिशील एवं सक्रिय नहीं होता । निष्क्रिय होकर समाप्त हो जाता है। जिस संगठन में अकरणीय कार्य के प्रति अंगुली नहीं उठती है, उसे दंडित नहीं किया जाता, वह संगठन हड्डियों का ढेर अथवा दोषों का घर बन जाता है। प्रोत्साहन देना मृदुता का बोधक है और दंड प्रायश्चित्त देना कठोरता का । इन दोनों की संतुलित व्याप्ति अनेकान्त द्वारा ही संभव है ।
विरोधी युगल है- श्रद्धा और तर्क । केवल श्रद्धा अंधी होती है और केवल तर्क पंगु । यदि अनुशास्ता अपने सदस्यों में दोनों का सामंजस्य नहीं कर पाता तो संगठन छिन्न-भिन्न हो जाता है। केवल श्रद्धा में समर्पण होना जड़ता होगी, चापलूसी पनपेगी। केवल तर्क में बौद्धिकता होगी पर हृदय नहीं होगा। दोनों का समन्वय अनेकान्त दृष्टि से ही साधा जा सकता है। नेता के प्रति विश्वास और समर्पण भी आवश्यक है पर कोरी अनुकरणप्रियता न रहे जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता सत्ता या बुद्धि कुंठित या प्रत्याहत हो जाए। भाव और बुद्धि का यह वैषम्य मिटाया नहीं जा सकता पर इसमें समन्वय साधा जा सकता है। सापेक्ष दृष्टि वाला अनुशास्ता श्रद्धाप्रवण व्यक्तियों की बुद्धि को तीक्ष्ण करता है तथा तर्कप्रवण व्यक्तियों को समर्पण की मूल्यवत्ता और यथार्थता का बोध कराता है। उत्तम तर्क वही होता है जो श्रद्धा के प्रकर्ष में फूटता है ।
सामंजस्य
सामंजस्य के बिना नयी पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के संघर्ष को नहीं रोका जा सकता। पुरानी पीढ़ी का अनुभव एवं नयी पीढ़ी का कर्त्तव्य दोनों का पारस्परिक संयोजन समाज की प्रगति के
तुलसी प्रज्ञा जनवरी-मार्च, 2002
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
67
www.jainelibrary.org