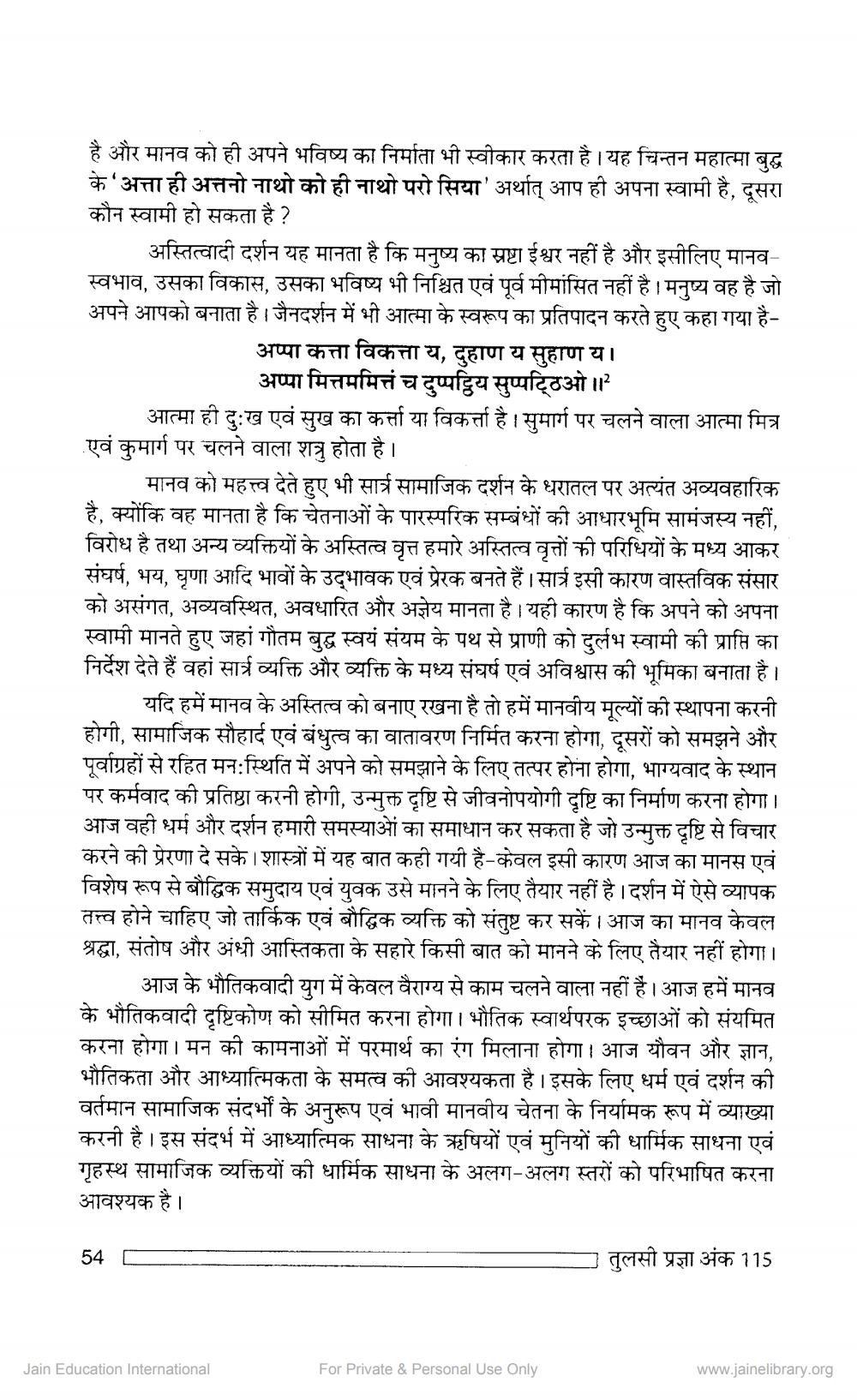________________
है और मानव को ही अपने भविष्य का निर्माता भी स्वीकार करता है । यह चिन्तन महात्मा बुद्ध के 'अत्ता ही अत्तनो नाथो को ही नाथो परो सिया' अर्थात् आप ही अपना स्वामी है, दूसरा कौन स्वामी हो सकता है?
अस्तित्वादी दर्शन यह मानता है कि मनुष्य का स्रष्टा ईश्वर नहीं है और इसीलिए मानवस्वभाव, उसका विकास, उसका भविष्य भी निश्चित एवं पूर्व मीमांसित नहीं है। मनुष्य वह है जो अपने आपको बनाता है। जैनदर्शन में भी आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है
अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुहाण य सुहाण य।
अप्पा मित्तममित्तं च दुप्पट्ठिय सुप्पट्ठिओ॥ आत्मा ही दुःख एवं सुख का कर्ता या विकर्ता है। सुमार्ग पर चलने वाला आत्मा मित्र एवं कुमार्ग पर चलने वाला शत्रु होता है।
मानव को महत्त्व देते हुए भी सार्च सामाजिक दर्शन के धरातल पर अत्यंत अव्यवहारिक है, क्योंकि वह मानता है कि चेतनाओं के पारस्परिक सम्बंधों की आधारभूमि सामंजस्य नहीं, विरोध है तथा अन्य व्यक्तियों के अस्तित्व वृत्त हमारे अस्तित्व वृत्तों की परिधियों के मध्य आकर संघर्ष, भय, घृणा आदि भावों के उद्भावक एवं प्रेरक बनते हैं । सार्च इसी कारण वास्तविक संसार को असंगत, अव्यवस्थित, अवधारित और अज्ञेय मानता है। यही कारण है कि अपने को अपना स्वामी मानते हुए जहां गौतम बुद्ध स्वयं संयम के पथ से प्राणी को दुर्लभ स्वामी की प्राप्ति का निर्देश देते हैं वहां सात्र व्यक्ति और व्यक्ति के मध्य संघर्ष एवं अविश्वास की भूमिका बनाता है।
___यदि हमें मानव के अस्तित्व को बनाए रखना है तो हमें मानवीय मूल्यों की स्थापना करनी होगी, सामाजिक सौहार्द एवं बंधुत्व का वातावरण निर्मित करना होगा, दूसरों को समझने और पूर्वाग्रहों से रहित मन:स्थिति में अपने को समझाने के लिए तत्पर होना होगा, भाग्यवाद के स्थान पर कर्मवाद की प्रतिष्ठा करनी होगी, उन्मुक्त दृष्टि से जीवनोपयोगी दृष्टि का निर्माण करना होगा। आज वही धर्म और दर्शन हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है जो उन्मुक्त दृष्टि से विचार करने की प्रेरणा दे सके। शास्त्रों में यह बात कही गयी है-केवल इसी कारण आज का मानस एवं विशेष रूप से बौद्धिक समुदाय एवं युवक उसे मानने के लिए तैयार नहीं है । दर्शन में ऐसे व्यापक तत्त्व होने चाहिए जो तार्किक एवं बौद्धिक व्यक्ति को संतुष्ट कर सकें । आज का मानव केवल श्रद्धा, संतोष और अंधी आस्तिकता के सहारे किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा।
आज के भौतिकवादी युग में केवल वैराग्य से काम चलने वाला नहीं है। आज हमें मानव के भौतिकवादी दृष्टिकोण को सीमित करना होगा। भौतिक स्वार्थपरक इच्छाओं को संयमित करना होगा। मन की कामनाओं में परमार्थ का रंग मिलाना होगा। आज यौवन और ज्ञान, भौतिकता और आध्यात्मिकता के समत्व की आवश्यकता है। इसके लिए धर्म एवं दर्शन की वर्तमान सामाजिक संदर्भो के अनुरूप एवं भावी मानवीय चेतना के निर्यामक रूप में व्याख्या करनी है। इस संदर्भ में आध्यात्मिक साधना के ऋषियों एवं मुनियों की धार्मिक साधना एवं गृहस्थ सामाजिक व्यक्तियों की धार्मिक साधना के अलग-अलग स्तरों को परिभाषित करना आवश्यक है।
54
- तुलसी प्रज्ञा अंक 115
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org