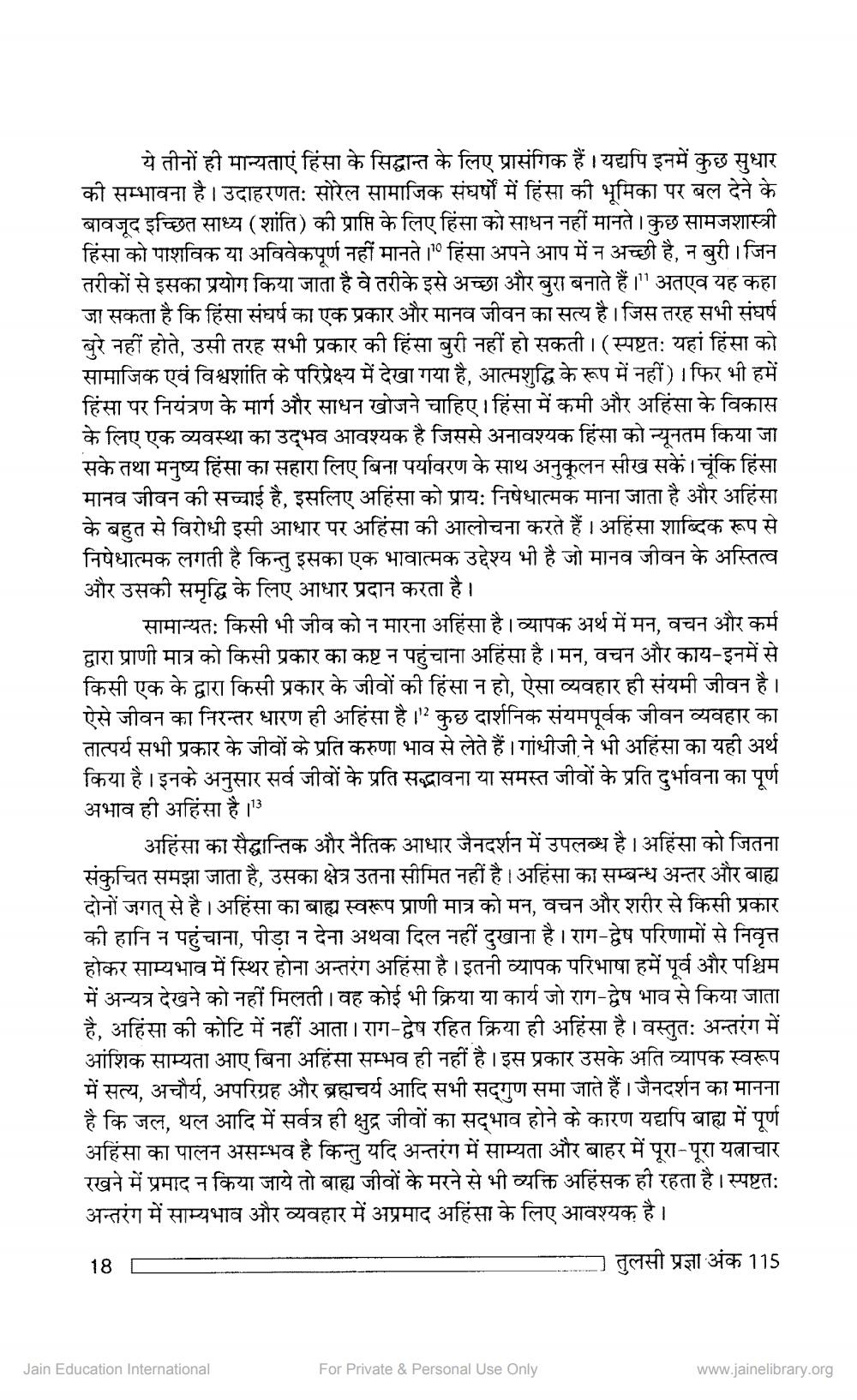________________
ये तीनों ही मान्यताएं हिंसा के सिद्धान्त के लिए प्रासंगिक हैं। यद्यपि इनमें कुछ सुधार की सम्भावना है। उदाहरणत: सोरेल सामाजिक संघर्षों में हिंसा की भूमिका पर बल देने के बावजूद इच्छित साध्य (शांति) की प्राप्ति के लिए हिंसा को साधन नहीं मानते। कुछ सामजशास्त्री हिंसा को पाशविक या अविवेकपूर्ण नहीं मानते।" हिंसा अपने आप में न अच्छी है, न बुरी। जिन तरीकों से इसका प्रयोग किया जाता है वे तरीके इसे अच्छा और बुरा बनाते हैं ।" अतएव यह कहा जा सकता है कि हिंसा संघर्ष का एक प्रकार और मानव जीवन का सत्य है। जिस तरह सभी संघर्ष बुरे नहीं होते, उसी तरह सभी प्रकार की हिंसा बुरी नहीं हो सकती। (स्पष्टतः यहां हिंसा को सामाजिक एवं विश्वशांति के परिप्रेक्ष्य में देखा गया है, आत्मशुद्धि के रूप में नहीं) । फिर भी हमें हिंसा पर नियंत्रण के मार्ग और साधन खोजने चाहिए। हिंसा में कमी और अहिंसा के विकास के लिए एक व्यवस्था का उद्भव आवश्यक है जिससे अनावश्यक हिंसा को न्यूनतम किया जा स तथा मनुष्य हिंसा का सहारा लिए बिना पर्यावरण के साथ अनुकूलन सीख सकें। चूंकि हिंसा मानव जीवन की सच्चाई है, इसलिए अहिंसा को प्रायः निषेधात्मक माना जाता है और अहिंसा के बहुत से विरोधी इसी आधार पर अहिंसा की आलोचना करते हैं। अहिंसा शाब्दिक रूप से निषेधात्मक लगती है किन्तु इसका एक भावात्मक उद्देश्य भी है जो मानव जीवन के अस्तित्व और उसकी समृद्धि के लिए आधार प्रदान करता है।
सामान्यतः किसी भी जीव को न मारना अहिंसा है। व्यापक अर्थ में मन, वचन और कर्म द्वारा प्राणी मात्र को किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचाना अहिंसा है। मन, वचन और काय- इनमें से किसी एक के द्वारा किसी प्रकार के जीवों की हिंसा न हो, ऐसा व्यवहार ही संयमी जीवन है । ऐसे जीवन का निरन्तर धारण ही अहिंसा है। 12 कुछ दार्शनिक संयमपूर्वक जीवन व्यवहार का तात्पर्य सभी प्रकार के जीवों के प्रति करुणा भाव से लेते हैं। गांधीजी ने भी अहिंसा का यही अर्थ किया है। इनके अनुसार सर्व जीवों के प्रति सद्भावना या समस्त जीवों के प्रति दुर्भावना का पूर्ण अभाव ही अहिंसा है। 13
अहिंसा का सैद्धान्तिक और नैतिक आधार जैनदर्शन में उपलब्ध है। अहिंसा को जितना संकुचित समझा जाता है, उसका क्षेत्र उतना सीमित नहीं है। अहिंसा का सम्बन्ध अन्तर और बाह्य दोनों जगत् से है | अहिंसा का बाह्य स्वरूप प्राणी मात्र को मन, वचन और शरीर से किसी प्रकार की हानि न पहुंचाना, पीड़ा न देना अथवा दिल नहीं दुखाना है। राग-द्वेष परिणामों से निवृत्त होकर साम्यभाव में स्थिर होना अन्तरंग अहिंसा है। इतनी व्यापक परिभाषा हमें पूर्व और पश्चिम में अन्यत्र देखने को नहीं मिलती। वह कोई भी क्रिया या कार्य जो राग-द्वेष भाव से किया जाता है, अहिंसा की कोटि में नहीं आता। राग-द्वेष रहित क्रिया ही अहिंसा है। वस्तुतः अन्तरंग में आंशिक साम्यता आए बिना अहिंसा सम्भव ही नहीं है। इस प्रकार उसके अति व्यापक स्वरूप में सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य आदि सभी सद्गुण समा जाते हैं। जैनदर्शन का मानना है कि जल, थल आदि में सर्वत्र ही क्षुद्र जीवों का सद्भाव होने के कारण यद्यपि बाह्य में पूर्ण अहिंसा का पालन असम्भव है किन्तु यदि अन्तरंग में साम्यता और बाहर में पूरा-पूरा यत्नाचार रखने में प्रमाद न किया जाये तो बाह्य जीवों के मरने से भी व्यक्ति अहिंसक ही रहता है। स्पष्टतः अन्तरंग में साम्यभाव और व्यवहार में अप्रमाद अहिंसा के लिए आवश्यक
है I
तुलसी प्रज्ञा अंक 115
18
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org