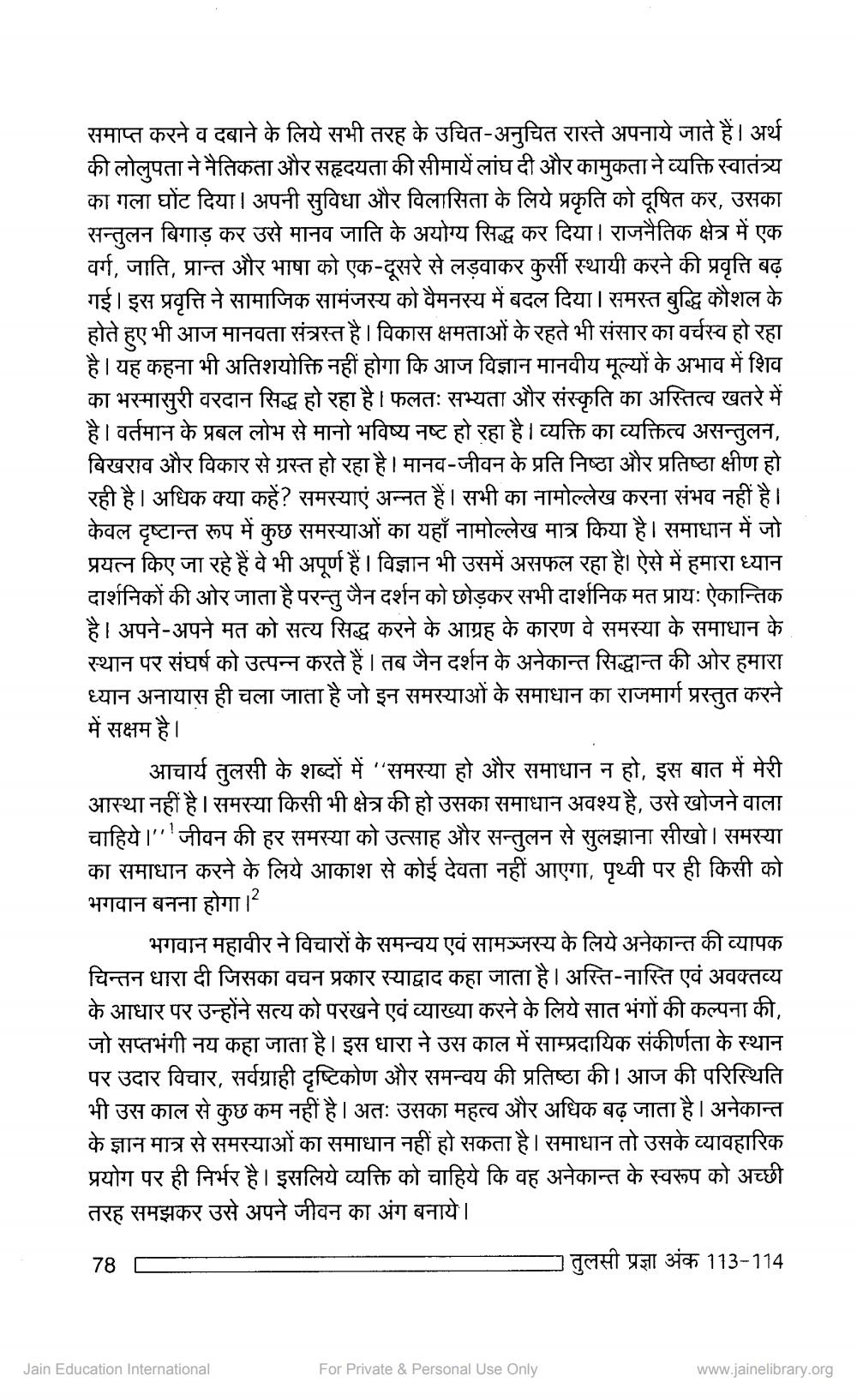________________
समाप्त करने व दबाने के लिये सभी तरह के उचित-अनुचित रास्ते अपनाये जाते हैं। अर्थ की लोलुपता ने नैतिकता और सहृदयता की सीमायें लांघ दी और कामुकता ने व्यक्ति स्वातंत्र्य का गला घोंट दिया। अपनी सुविधा और विलासिता के लिये प्रकृति को दूषित कर, उसका सन्तुलन बिगाड़ कर उसे मानव जाति के अयोग्य सिद्ध कर दिया। राजनैतिक क्षेत्र में एक वर्ग, जाति, प्रान्त और भाषा को एक-दूसरे से लड़वाकर कुर्सी स्थायी करने की प्रवृत्ति बढ़ गई। इस प्रवृत्ति ने सामाजिक सामंजस्य को वैमनस्य में बदल दिया । समस्त बुद्धि कौशल के होते हुए भी आज मानवता संत्रस्त है। विकास क्षमताओं के रहते भी संसार का वर्चस्व हो रहा है। यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आज विज्ञान मानवीय मूल्यों के अभाव में शिव का भस्मासुरी वरदान सिद्ध हो रहा है। फलतः सभ्यता और संस्कृति का अस्तित्व खतरे में है। वर्तमान के प्रबल लोभ से मानो भविष्य नष्ट हो रहा है। व्यक्ति का व्यक्तित्व असन्तुलन, बिखराव और विकार से ग्रस्त हो रहा है। मानव-जीवन के प्रति निष्ठा और प्रतिष्ठा क्षीण हो रही है। अधिक क्या कहें? समस्याएं अन्नत हैं। सभी का नामोल्लेख करना संभव नहीं है। केवल दृष्टान्त रूप में कुछ समस्याओं का यहाँ नामोल्लेख मात्र किया है। समाधान में जो प्रयत्न किए जा रहे हैं वे भी अपूर्ण हैं । विज्ञान भी उसमें असफल रहा है। ऐसे में हमारा ध्यान दार्शनिकों की ओर जाता है परन्तु जैन दर्शन को छोड़कर सभी दार्शनिक मत प्रायः ऐकान्तिक है। अपने-अपने मत को सत्य सिद्ध करने के आग्रह के कारण वे समस्या के समाधान के स्थान पर संघर्ष को उत्पन्न करते हैं । तब जैन दर्शन के अनेकान्त सिद्धान्त की ओर हमारा ध्यान अनायास ही चला जाता है जो इन समस्याओं के समाधान का राजमार्ग प्रस्तुत करने में सक्षम है।
आचार्य तुलसी के शब्दों में "समस्या हो और समाधान न हो, इस बात में मेरी आस्था नहीं है। समस्या किसी भी क्षेत्र की हो उसका समाधान अवश्य है, उसे खोजने वाला चाहिये।''जीवन की हर समस्या को उत्साह और सन्तुलन से सुलझाना सीखो। समस्या का समाधान करने के लिये आकाश से कोई देवता नहीं आएगा, पृथ्वी पर ही किसी को भगवान बनना होगा।
भगवान महावीर ने विचारों के समन्वय एवं सामञ्जस्य के लिये अनेकान्त की व्यापक चिन्तन धारा दी जिसका वचन प्रकार स्याद्वाद कहा जाता है। अस्ति-नास्ति एवं अवक्तव्य के आधार पर उन्होंने सत्य को परखने एवं व्याख्या करने के लिये सात भंगों की कल्पना की, जो सप्तभंगी नय कहा जाता है। इस धारा ने उस काल में साम्प्रदायिक संकीर्णता के स्थान पर उदार विचार, सर्वग्राही दृष्टिकोण और समन्वय की प्रतिष्ठा की। आज की परिस्थिति भी उस काल से कुछ कम नहीं है। अतः उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। अनेकान्त के ज्ञान मात्र से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। समाधान तो उसके व्यावहारिक प्रयोग पर ही निर्भर है। इसलिये व्यक्ति को चाहिये कि वह अनेकान्त के स्वरूप को अच्छी तरह समझकर उसे अपने जीवन का अंग बनाये । 78 ।
- तुलसी प्रज्ञा अंक 113-114
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org