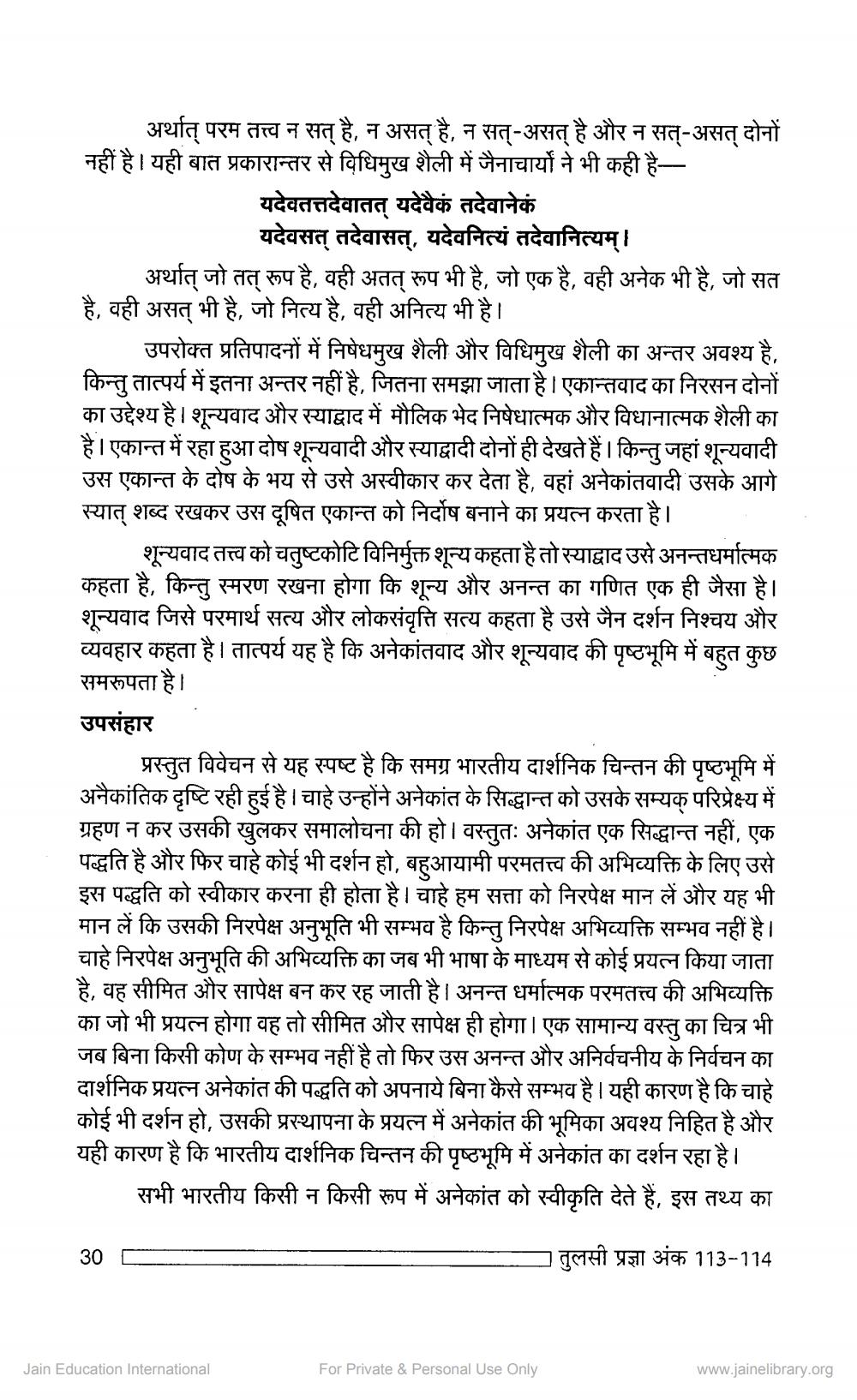________________
अर्थात् परम तत्त्व न सत् है, न असत् है, न सत्-असत् है और न सत्-असत् दोनों नहीं है। यही बात प्रकारान्तर से विधिमुख शैली में जैनाचार्यों ने भी कही है— यदेवतत्तदेवातत् यदेवैकं तदेवानेकं
यदेवसत् तदेवासत्, यदेवनित्यं तदेवानित्यम् ।
अर्थात् जो तत् रूप है, वही अतत् रूप भी है, जो एक है, वही अनेक भी है, जो सत है, वही असत् भी है, जो नित्य है, वही अनित्य भी है।
उपरोक्त प्रतिपादनों में निषेधमुख शैली और विधिमुख शैली का अन्तर अवश्य है, किन्तु तात्पर्य में इतना अन्तर नहीं है, जितना समझा जाता है। एकान्तवाद का निरसन दोनों का उद्देश्य है । शून्यवाद और स्याद्वाद में मौलिक भेद निषेधात्मक और विधानात्मक शैली का है । एकान्त में रहा हुआ दोष शून्यवादी और स्याद्वादी दोनों ही देखते हैं । किन्तु जहां शून्यवादी उस एकान्त के दोष के भय से उसे अस्वीकार कर देता है, वहां अनेकांतवादी उसके आगे स्यात् शब्द रखकर उस दूषित एकान्त को निर्दोष बनाने का प्रयत्न करता है ।
शून्यवाद तत्त्व को चतुष्टकोटि विनिर्मुक्त शून्य कहता है तो स्याद्वाद उसे अनन्तधर्मात्मक कहता है, किन्तु स्मरण रखना होगा कि शून्य और अनन्त का गणित एक ही जैसा है। शून्यवाद जिसे परमार्थ सत्य और लोकसंवृत्ति सत्य कहता है उसे जैन दर्शन निश्चय और व्यवहार कहता है। तात्पर्य यह है कि अनेकांतवाद और शून्यवाद की पृष्ठभूमि में बहुत कुछ समरूपता है।
उपसंहार
प्रस्तुत विवेचन से यह स्पष्ट है कि समग्र भारतीय दार्शनिक चिन्तन की पृष्ठभूमि में अनैकांतिक दृष्टि रही हुई है । चाहे उन्होंने अनेकांत के सिद्धान्त को उसके सम्यक् परिप्रेक्ष्य में ग्रहण न कर उसकी खुलकर समालोचना की हो । वस्तुतः अनेकांत एक सिद्धान्त नहीं, एक पद्धति है और फिर चाहे कोई भी दर्शन हो, बहुआयामी परमतत्त्व की अभिव्यक्ति के लिए उसे इस पद्धति को स्वीकार करना ही होता है। चाहे हम सत्ता को निरपेक्ष मान लें और यह भी मान लें कि उसकी निरपेक्ष अनुभूति भी सम्भव है किन्तु निरपेक्ष अभिव्यक्ति सम्भव नहीं है। चाहे निरपेक्ष अनुभूति की अभिव्यक्ति का जब भी भाषा के माध्यम से कोई प्रयत्न किया जाता है, वह सीमित और सापेक्ष बन कर रह जाती है। अनन्त धर्मात्मक परमतत्त्व की अभिव्यक्ति का जो भी प्रयत्न होगा वह तो सीमित और सापेक्ष ही होगा। एक सामान्य वस्तु का चित्र भी जब बिना किसी कोण के सम्भव नहीं है तो फिर उस अनन्त और अनिर्वचनीय के निर्वचन का दार्शनिक प्रयत्न अनेकांत की पद्धति को अपनाये बिना कैसे सम्भव है। यही कारण है कि चाहे कोई भी दर्शन हो, उसकी प्रस्थापना के प्रयत्न में अनेकांत की भूमिका अवश्य निहित है और यही कारण है कि भारतीय दार्शनिक चिन्तन की पृष्ठभूमि में अनेकांत का दर्शन रहा है।
सभी भारतीय किसी न किसी रूप में अनेकांत को स्वीकृति देते हैं, इस तथ्य का
तुलसी प्रज्ञा अंक 113-114
30
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org