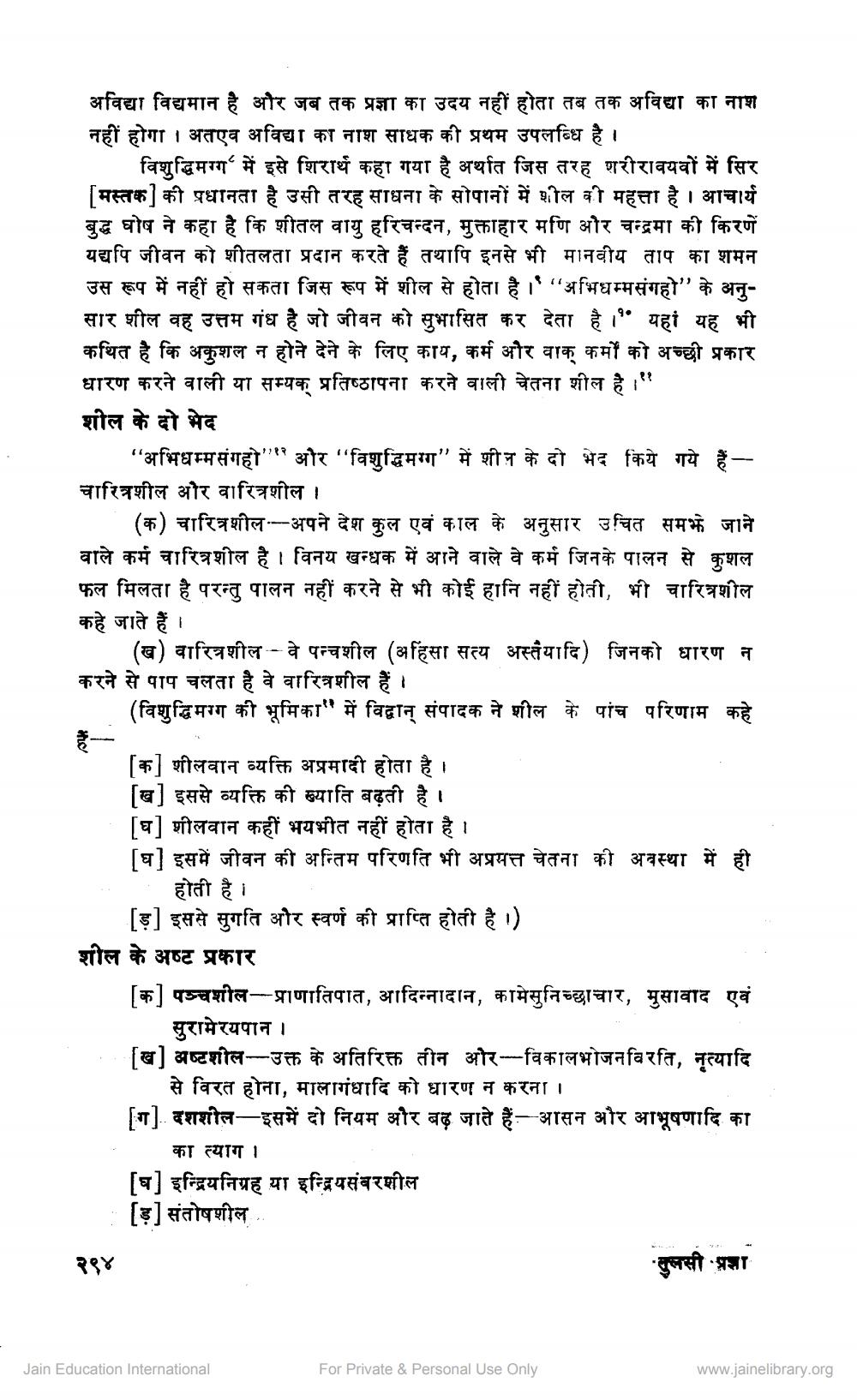________________
अविद्या विद्यमान है और जब तक प्रज्ञा का उदय नहीं होता तब तक अविद्या का नाश नहीं होगा । अतएव अविद्या का नाश साधक की प्रथम उपलब्धि है।
विशुद्धिमग्ग' में इसे शिरार्थ कहा गया है अर्थात जिस तरह शरीरावयवों में सिर [मस्तक] की प्रधानता है उसी तरह साधना के सोपानों में शील की महत्ता है । आचार्य बुद्ध घोष ने कहा है कि शीतल वायु हरिचन्दन, मुक्ताहार मणि और चन्द्रमा की किरणे यद्यपि जीवन को शीतलता प्रदान करते हैं तथापि इनसे भी मानवीय ताप का शमन उस रूप में नहीं हो सकता जिस रूप में शील से होता है । "अभिधम्मसंगहो' के अनुसार शील वह उत्तम गंध है जो जीवन को सुभासित कर देता है। यहां यह भी कथित है कि अकुशल न होने देने के लिए काय, कर्म और वाक् कर्मों को अच्छी प्रकार धारण करने वाली या सम्यक् प्रतिष्ठापना करने वाली चेतना शील है ।११ शील के दो भेद
"अभिधम्मसंगहो' और "विशुद्धिमग्ग" में शील के दो भेद किये गये हैंचारित्रशील और वारित्रशील ।
(क) चारित्रशील-अपने देश कुल एवं काल के अनुसार उचित समझे जाने वाले कर्म चारित्रशील है । विनय खन्धक में आने वाले वे कर्म जिनके पालन से कुशल फल मिलता है परन्तु पालन नहीं करने से भी कोई हानि नहीं होती, भी चारित्रशील कहे जाते हैं।
(ख) वारित्रशील - वे पन्चशील (अहिंसा सत्य अस्तैयादि) जिनको धारण न करने से पाप चलता है वे वारित्रशील हैं।
(विशुद्धिमग्ग की भूमिका में विद्वान् संपादक ने शील के पांच परिणाम कहे
[क] शीलवान व्यक्ति अप्रमादी होता है । [ख] इससे व्यक्ति की ख्याति बढ़ती है। [घ] शीलवान कहीं भयभीत नहीं होता है । [घ] इसमें जीवन की अन्तिम परिणति भी अप्रमत्त चेतना की अवस्था में ही
होती है। [3] इससे सुगति और स्वर्ण की प्राप्ति होती है।) शील के अष्ट प्रकार [क] पञ्चशील-प्राणातिपात, आदिन्नादान, कामेसुनिच्छाचार, मुसावाद एवं
सुरामेरयपान । [ख] अष्टशील-उक्त के अतिरिक्त तीन और-विकालभोजनविरति, नृत्यादि
से विरत होना, मालागंधादि को धारण न करना। [ग] दशशील—इसमें दो नियम और बढ़ जाते हैं-आसन और आभूषणादि का
का त्याग । [५] इन्द्रियनिग्रह या इन्द्रियसंवरशील
[] संतोषशील २९४
तुलसी प्रज्ञा
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org