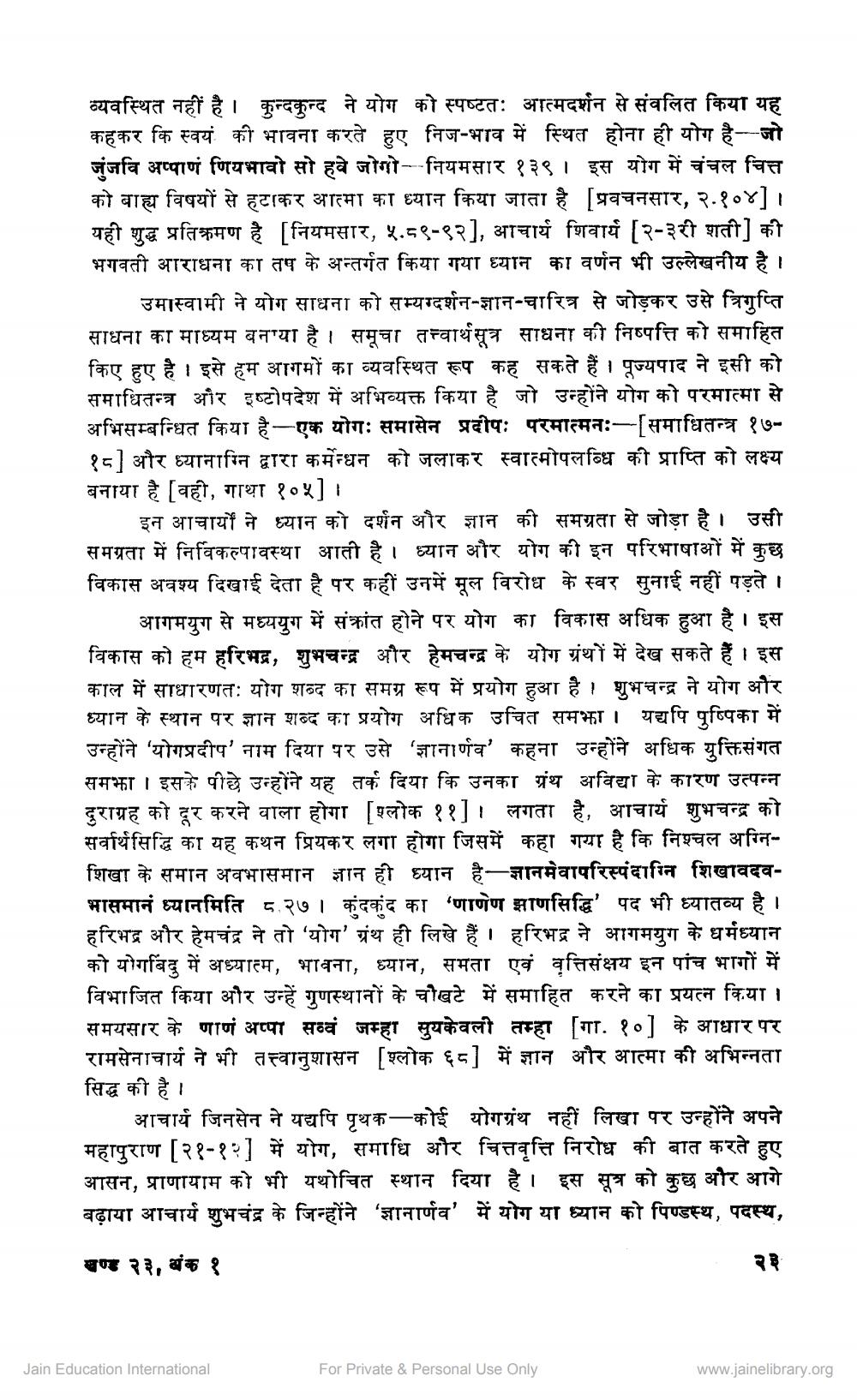________________
व्यवस्थित नहीं है। कुन्दकुन्द ने योग को स्पष्टतः आत्मदर्शन से संवलित किया यह कहकर कि स्वयं की भावना करते हुए निज-भाव में स्थित होना ही योग है--जो जुंजवि अप्पाणं णियभावो सो हवे जोगो--नियमसार १३९ । इस योग में चंचल चित्त को बाह्य विषयों से हटाकर आत्मा का ध्यान किया जाता है [प्रवचनसार, २.१०४] । यही शुद्ध प्रतिक्रमण है [नियमसार, ५.८९-९२], आचार्य शिवार्य [२-३री शती] की भगवती आराधना का तप के अन्तर्गत किया गया ध्यान का वर्णन भी उल्लेखनीय है ।
उमास्वामी ने योग साधना को सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र से जोड़कर उसे त्रिगुप्ति साधना का माध्यम बनाया है। समूचा तत्त्वार्थसूत्र साधना की निष्पत्ति को समाहित किए हुए है । इसे हम आगमों का व्यवस्थित रूप कह सकते हैं। पूज्यपाद ने इसी को समाधितन्त्र और इष्टोपदेश में अभिव्यक्त किया है जो उन्होंने योग को परमात्मा से अभिसम्बन्धित किया है-एक योगः समासेन प्रदीपः परमात्मनः-[समाधितन्त्र १७१८] और ध्यानाग्नि द्वारा कर्मेन्धन को जलाकर स्वात्मोपलब्धि की प्राप्ति को लक्ष्य बनाया है [वही, गाथा १०५] ।
इन आचार्यों ने ध्यान को दर्शन और ज्ञान की समग्रता से जोड़ा है। उसी समग्रता में निर्विकल्पावस्था आती है। ध्यान और योग की इन परिभाषाओं में कुछ विकास अवश्य दिखाई देता है पर कहीं उनमें मूल विरोध के स्वर सुनाई नहीं पड़ते ।
आगमयुग से मध्ययुग में संक्रांत होने पर योग का विकास अधिक हुआ है । इस विकास को हम हरिभद्र, शुभचन्द्र और हेमचन्द्र के योग ग्रंथों में देख सकते हैं । इस काल में साधारणत: योग शब्द का समग्र रूप में प्रयोग हुआ है। शुभचन्द्र ने योग और ध्यान के स्थान पर ज्ञान शब्द का प्रयोग अधिक उचित समझा। यद्यपि पुष्पिका में उन्होंने 'योगप्रदीप' नाम दिया पर उसे 'ज्ञानार्णव' कहना उन्होंने अधिक युक्तिसंगत समझा । इसके पीछे उन्होंने यह तर्क दिया कि उनका ग्रंथ अविद्या के कारण उत्पन्न दुराग्रह को दूर करने वाला होगा [श्लोक ११] । लगता है, आचार्य शुभचन्द्र को सर्वार्थसिद्धि का यह कथन प्रियकर लगा होगा जिसमें कहा गया है कि निश्चल अग्निशिखा के समान अवभासमान ज्ञान ही ध्यान है-ज्ञानमेवापरिस्पंदाग्नि शिखावदवभासमानं ध्यानमिति ८.२७ । कुंदकुंद का 'णाणण झाणसिद्धि' पद भी ध्यातव्य है । हरिभद्र और हेमचंद्र ने तो 'योग' ग्रंथ ही लिखे हैं। हरिभद्र ने आगमयुग के धर्मध्यान को योगबिंदु में अध्यात्म, भावना, ध्यान, समता एवं वत्तिसंक्षय इन पांच भागों में विभाजित किया और उन्हें गुणस्थानों के चौखटे में समाहित करने का प्रयत्न किया। समयसार के णाणं अप्पा सव्वं जम्हा सुयकेवली तम्हा [गा. १०] के आधार पर रामसेनाचार्य ने भी तत्त्वानुशासन [श्लोक ६८] में ज्ञान और आत्मा की अभिन्नता सिद्ध की है।
आचार्य जिनसेन ने यद्यपि पृथक-कोई योगग्रंथ नहीं लिखा पर उन्होंने अपने महापुराण [२१-१२] में योग, समाधि और चित्तवृत्ति निरोध की बात करते हुए आसन, प्राणायाम को भी यथोचित स्थान दिया है। इस सूत्र को कुछ और आगे बढ़ाया आचार्य शुभचंद्र के जिन्होंने 'ज्ञानार्णव' में योग या ध्यान को पिण्डस्थ, पदस्थ,
खण्ड २३, बंक १
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org