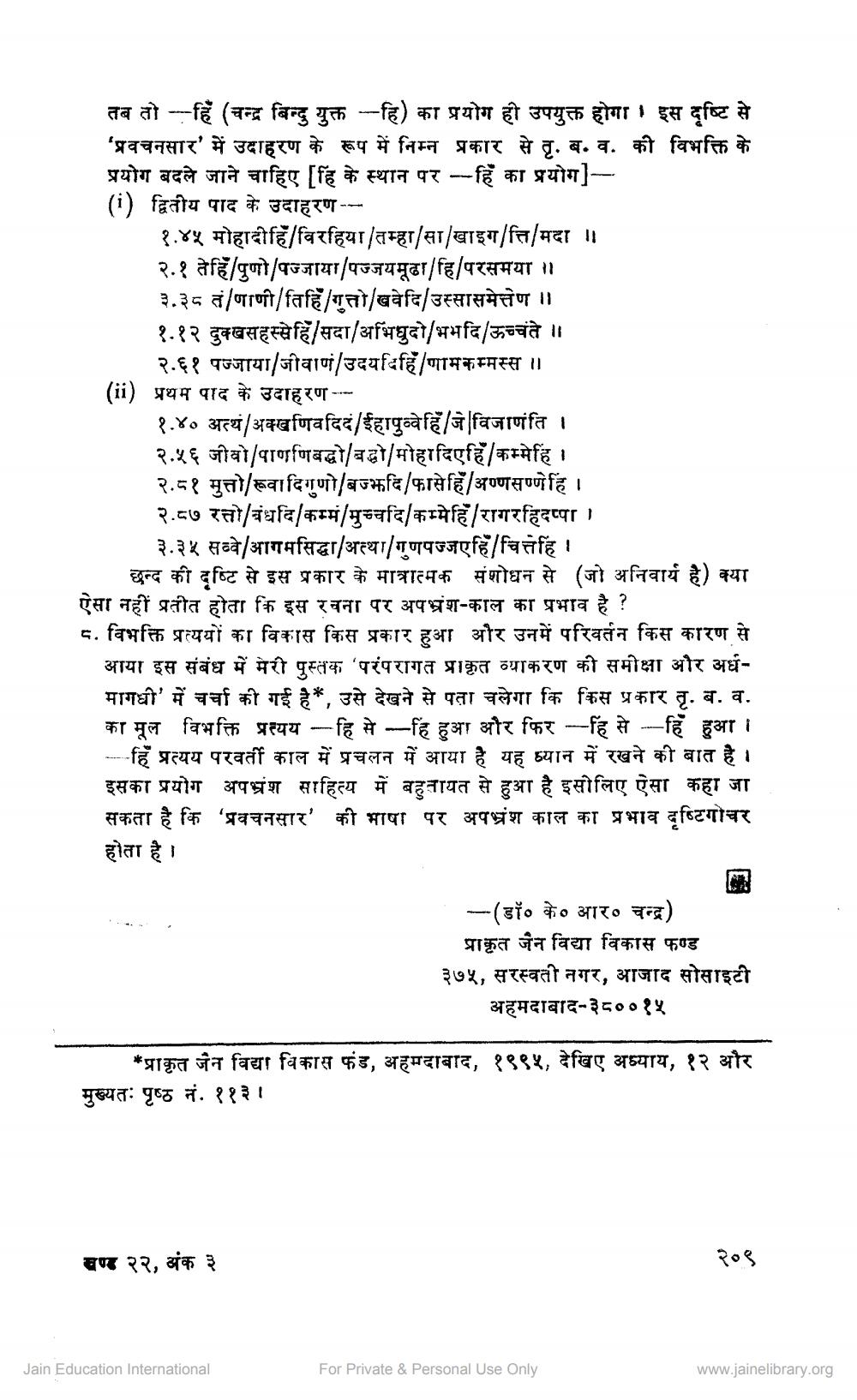________________
तब तो --हिं (चन्द्र बिन्दु युक्त -हि) का प्रयोग ही उपयुक्त होगा। इस दृष्टि से 'प्रवचनसार' में उदाहरण के रूप में निम्न प्रकार से तृ. ब. व. की विभक्ति के प्रयोग बदले जाने चाहिए [हिं के स्थान पर ---हिं का प्रयोग](i) द्वितीय पाद के उदाहरण---
१.४५ मोहादीहिं/विरहिया तम्हा/सा/खाइग/त्ति/मदा । २.१ तेहि/पुणो/पज्जाया/पज्जयमूढा/हि/परसमया ॥ ३.३८ तं/गाणी/तिहि/गुत्तो/खवेदि/उस्सासमेत्तेण ।। १.१२ दुक्खसहस्सेहि/सदा/अभिधुदो/भभदि/ऊच्चंते ॥
२.६१ पज्जाया/जीवाणं/उदयदिहिं /णामकम्मस्स ॥ (ii) प्रथम पाद के उदाहरण -----
१.४० अत्थं अक्खणिवदिदं/ईहापुव्वेहिँ/जे विजाणंति । २.५६ जीवो/पाणणिबद्धो/बद्धो/मोहादिएहिँ कम्मेहिं । २.८१ मुत्तो/रूवादिगुणो/बज्झदि/फासे हिँ/अण्णसणेहिं । २.८७ रत्तो/बंधदि कम्म/मुच्चदि/कम्मेहि / रागरहिदप्पा ।
३.३५ सव्वे/आगमसिद्धा/अत्था/गुणपज्जएहि/चित्तेहिं ।
छन्द की दृष्टि से इस प्रकार के मात्रात्मक संशोधन से (जो अनिवार्य है) क्या ऐसा नहीं प्रतीत होता कि इस रचना पर अपभ्रंश-काल का प्रभाव है ? ८. विभक्ति प्रत्ययों का विकास किस प्रकार हुआ और उनमें परिवर्तन किस कारण से
आया इस संबंध में मेरी पुस्तक 'परंपरागत प्राकृत व्याकरण की समीक्षा और अर्धमागधी' में चर्चा की गई है*, उसे देखने से पता चलेगा कि किस प्रकार तृ. ब. व. का मूल विभक्ति प्रत्यय -हि से -हिं हुआ और फिर -हिं से ---हिं हुआ। -----हिं प्रत्यय परवर्ती काल में प्रचलन में आया है यह ध्यान में रखने की बात है। इसका प्रयोग अपभ्रंश साहित्य में बहुतायत से हुआ है इसीलिए ऐसा कहा जा सकता है कि 'प्रवचनसार' की भाषा पर अपभ्रंश काल का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है।
---(डॉ० के० आर० चन्द्र) प्राकृत जैन विद्या विकास फण्ड ३७५, सरस्वती नगर, आजाद सोसाइटी
अहमदाबाद-३८००१५
-
*प्राकृत जैन विद्या विकास फंड, अहमदाबाद, १९९५, देखिए अध्याय, १२ और मुख्यतः पृष्ठ नं. ११३ ।
खण्ड २२, अंक ३
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org